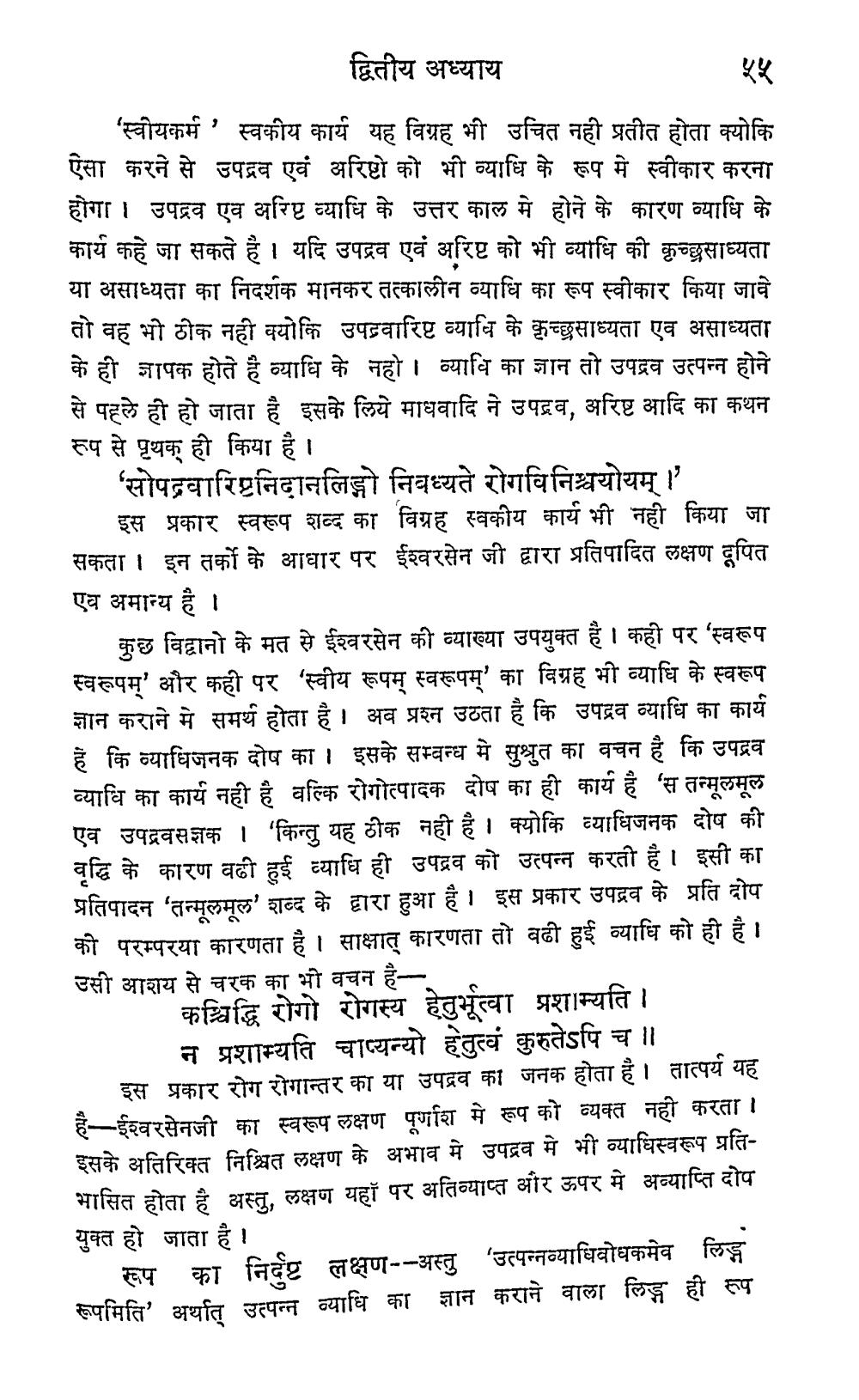________________
द्वितीय अध्याय 'स्त्रीयकर्म' स्वकीय कार्य यह विग्रह भी उचित नही प्रतीत होता क्योकि ऐसा करने से उपद्रव एवं अरिष्टो को भी व्याधि के रूप मे स्वीकार करना होगा। उपद्रव एव अरिष्ट व्याधि के उत्तर काल मे होने के कारण व्याधि के कार्य कहे जा सकते है । यदि उपद्रव एवं अरिट को भी व्याधि की कृच्छ्रसाध्यता या असाध्यता का निदर्शक मानकर तत्कालीन व्याधि का रूप स्वीकार किया जावे तो वह भी ठीक नही क्योकि उपद्रवारिष्ट व्याधि के कृच्छ्रसाध्यता एव असाध्यता के ही ज्ञापक होते है व्याधि के नहो । व्यावि का ज्ञान तो उपद्रव उत्पन्न होने से पहले ही हो जाता है इसके लिये माधवादि ने उपद्रव, अरिष्ट आदि का कथन रूप से पृथक् ही किया है।
'सोपवारिष्टनिदानलिङ्गो निबध्यते रोगविनिश्चयोयम् ।'
इस प्रकार स्वरूप शब्द का विग्रह स्वकीय कार्य भी नही किया जा सकता। इन तर्कों के आधार पर ईश्वरसेन जी द्वारा प्रतिपादित लक्षण दूपित एव अमान्य है ।
कुछ विद्वानो के मत से ईश्वरसेन की व्याख्या उपयुक्त है । कही पर 'स्वरूप स्वरूपम्' और कही पर 'स्वीय रूपम् स्वरूपम्' का विग्रह भी व्याधि के स्वरूप ज्ञान कराने में समर्थ होता है। अब प्रश्न उठता है कि उपद्रव व्याधि का कार्य है कि व्याधिजनक दोष का। इसके सम्बन्ध मे सुश्रुत का वचन है कि उपद्रव व्याधि का कार्य नहीं है बल्कि रोगोत्पादक दोष का ही कार्य है 'स तन्मूलमूल एव उपद्रवसज्ञक । 'किन्तु यह ठीक नही है। क्योकि व्याधिजनक दोष की वृद्धि के कारण वढी हुई व्याधि ही उपद्रव को उत्पन्न करती है। इसी का प्रतिपादन 'तन्मूलमूल' शब्द के द्वारा हुआ है। इस प्रकार उपद्रव के प्रति दोप को परम्परया कारणता है । साक्षात् कारणता तो बढी हुई व्याधि को ही है। उसी आशय से चरक का भी वचन है
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूत्वा प्रशाम्यति ।
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ॥ __ इस प्रकार रोग रोगान्तर का या उपद्रव का जनक होता है। तात्पर्य यह है-ईश्वरसेनजी का स्वरूप लक्षण पूर्गाश मे रूप को व्यक्त नही करता। इसके अतिरिक्त निश्चित लक्षण के अभाव मे उपद्रव मे भी व्याधिस्वरूप प्रतिभासित होता है अस्तु, लक्षण यहाँ पर अतिव्याप्त और ऊपर मे अव्याप्ति दोप युक्त हो जाता है।
रूप का निर्दष्ट लक्षण--अस्तु 'उत्पन्नव्याधिवोधकमेव लिङ्ग रूपमिति' अर्थात उत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराने वाला लिन ही रूप