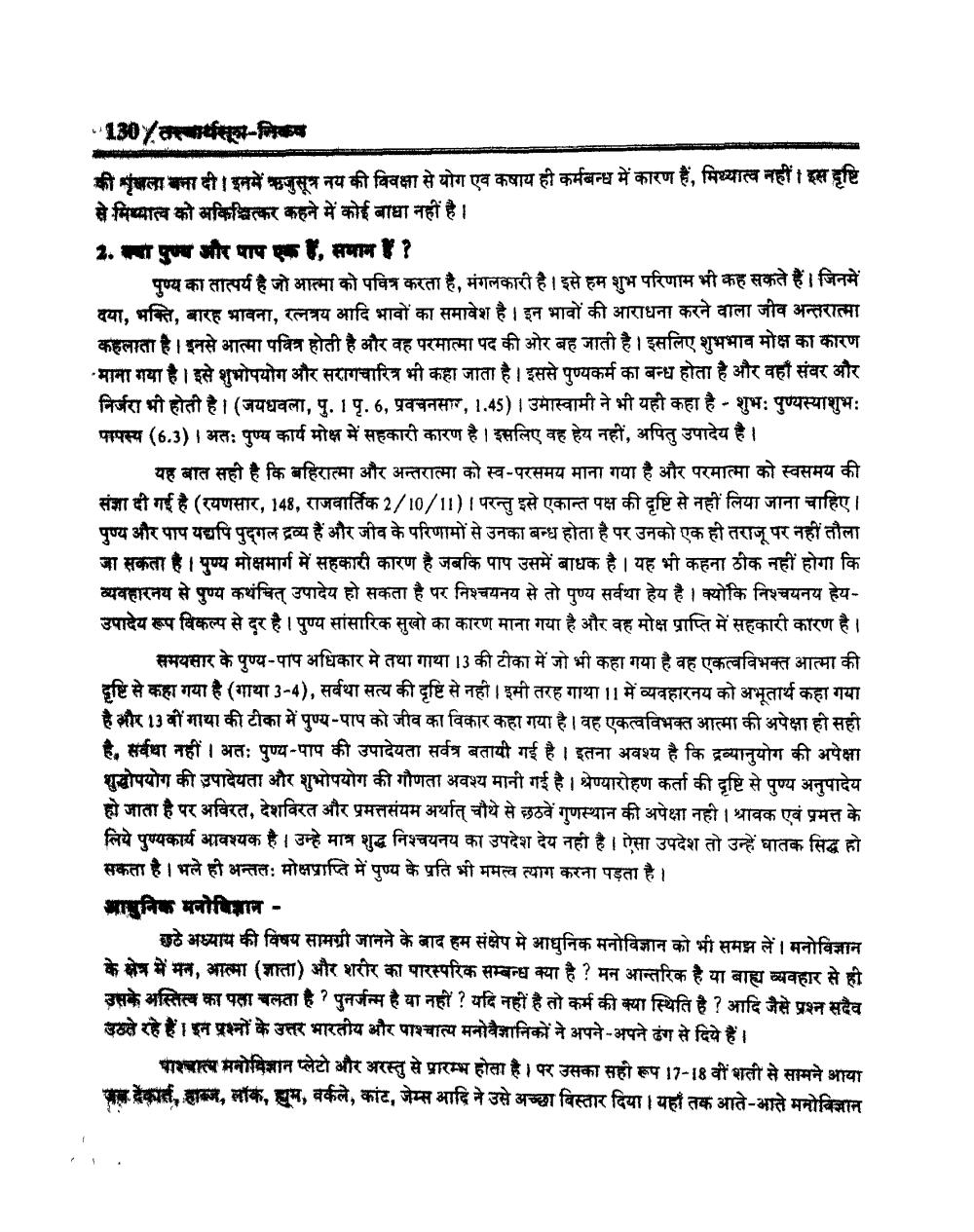________________
130/ तत्वार्थसूत्र - निकव
की श्रृंखला बना दी। इनमें ऋजुसूत्र नय की विवक्षा से योग एव कषाय ही कर्मबन्ध में कारण हैं, मिथ्यात्व नहीं। इस दृष्टि सेमियात्व को चित्कर कहने में कोई बाधा नहीं है।
2. क्या पुण्य और पाप एक हैं, समान हैं ?
पुण्य का तात्पर्य है जो आत्मा को पवित्र करता है, मंगलकारी है। इसे हम शुभ परिणाम भी कह सकते हैं। जिनमें दया, भक्ति, बारह भावना, रत्नत्रय आदि भावों का समावेश है। इन भावों की आराधना करने वाला जीव अन्तरात्मा कहलाता है। इनसे आत्मा पवित्र होती है और वह परमात्मा पद की ओर बह जाती है। इसलिए शुभभाव मोक्ष का कारण - माना गया है। इसे शुभोपयोग और सरागचारित्र भी कहा जाता है। इससे पुण्यकर्म का बन्ध होता है और वहाँ संवर और निर्जरा भी होती है। (जयधवला, पु. 1 पृ.6, प्रवचनसार, 1.45 ) । उमास्वामी ने भी यही कहा है - शुभः पुण्यस्याशुभ: पापस्य (6.3) 1 अत: पुण्य कार्य मोक्ष में सहकारी कारण है। इसलिए वह हेय नहीं, अपितु उपादेय है।
यह बात सही है कि बहिरात्मा और अन्तरात्मा को स्व-परसमय माना गया है और परमात्मा को स्वसमय की संज्ञा दी गई है ( रयणसार, 148, राजवार्तिक 2/10/11 ) । परन्तु इसे एकान्त पक्ष की दृष्टि से नहीं लिया जाना चाहिए। पुण्य और पाप यद्यपि पुद्गल द्रव्य हैं और जीव के परिणामों से उनका बन्ध होता है पर उनको एक ही तराजू पर नहीं तौला जा सकता है। पुण्य मोक्षमार्ग में सहकारी कारण है जबकि पाप उसमें बाधक है। यह भी कहना ठीक नहीं होगा कि व्यवहारनय से पुण्य कथंचित् उपादेय हो सकता है पर निश्चयनय से तो पुण्य सर्वथा हेय है। क्योंकि निश्चयनय हेय - उपादेय रूप विकल्प से दूर है। पुण्य सांसारिक सुखो का कारण माना गया है और वह मोक्ष प्राप्ति में सहकारी कारण है।
समयसार के पुण्य-पाप अधिकार मे तथा गाथा 13 की टीका में जो भी कहा गया है वह एकत्वविभक्त आत्मा की दृष्टि से कहा गया है (गाथा 3-4 ), सर्वथा सत्य की दृष्टि से नही। इसी तरह गाथा 11 में व्यवहारनय को अभूतार्थ कहा गया है और 13 वीं गाथा की टीका में पुण्य-पाप को जीव का विकार कहा गया है। वह एकत्वविभक्त आत्मा की अपेक्षा ही सही है, सर्वथा नहीं । अतः पुण्य-पाप की उपादेयता सर्वत्र बतायी गई है । इतना अवश्य है कि द्रव्यानुयोग की अपेक्षा शुद्धोपयोग की उपादेयता और शुभोपयोग की गौणता अवश्य मानी गई है। श्रेण्यारोहण कर्ता की दृष्टि से पुण्य अनुपादेय हो जाता है पर अविरत, देशविरत और प्रमत्तसंयम अर्थात् चौथे से छठवें गुणस्थान की अपेक्षा नही । श्रावक एवं प्रमत्त के लिये पुण्यकार्य आवश्यक है। उन्हे मात्र शुद्ध निश्चयनय का उपदेश देय नही है। ऐसा उपदेश तो उन्हें घातक सिद्ध हो सकता है। भले ही अन्ततः मोक्षप्राप्ति में पुण्य के प्रति भी ममत्व त्याग करना पड़ता है।
आधुनिक मनोविज्ञान
छठे अध्याय की विषय सामग्री जानने के बाद हम संक्षेप मे आधुनिक मनोविज्ञान को भी समझ लें । मनोविज्ञान के क्षेत्र में मन, आत्मा (ज्ञाता) और शरीर का पारस्परिक सम्बन्ध क्या है ? मन आन्तरिक है या बाह्य व्यवहार से ही उसके अस्तित्व का पता चलता है ? पुनर्जन्म है या नहीं ? यदि नहीं है तो कर्म की क्या स्थिति है ? आदि जैसे प्रश्न सदैव उठते रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भारतीय और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने ढंग से दिये हैं।
-
पाश्चात्य मनोविज्ञान प्लेटो और अरस्तु से प्रारम्भ होता है। पर उसका सही रूप 17-18 वीं शती से सामने आया जब देकार्त हाब्ज, लॉक, ह्यूम, बर्कले, कांट, जेम्स आदि ने उसे अच्छा विस्तार दिया। यहाँ तक आते-आते मनोविज्ञान