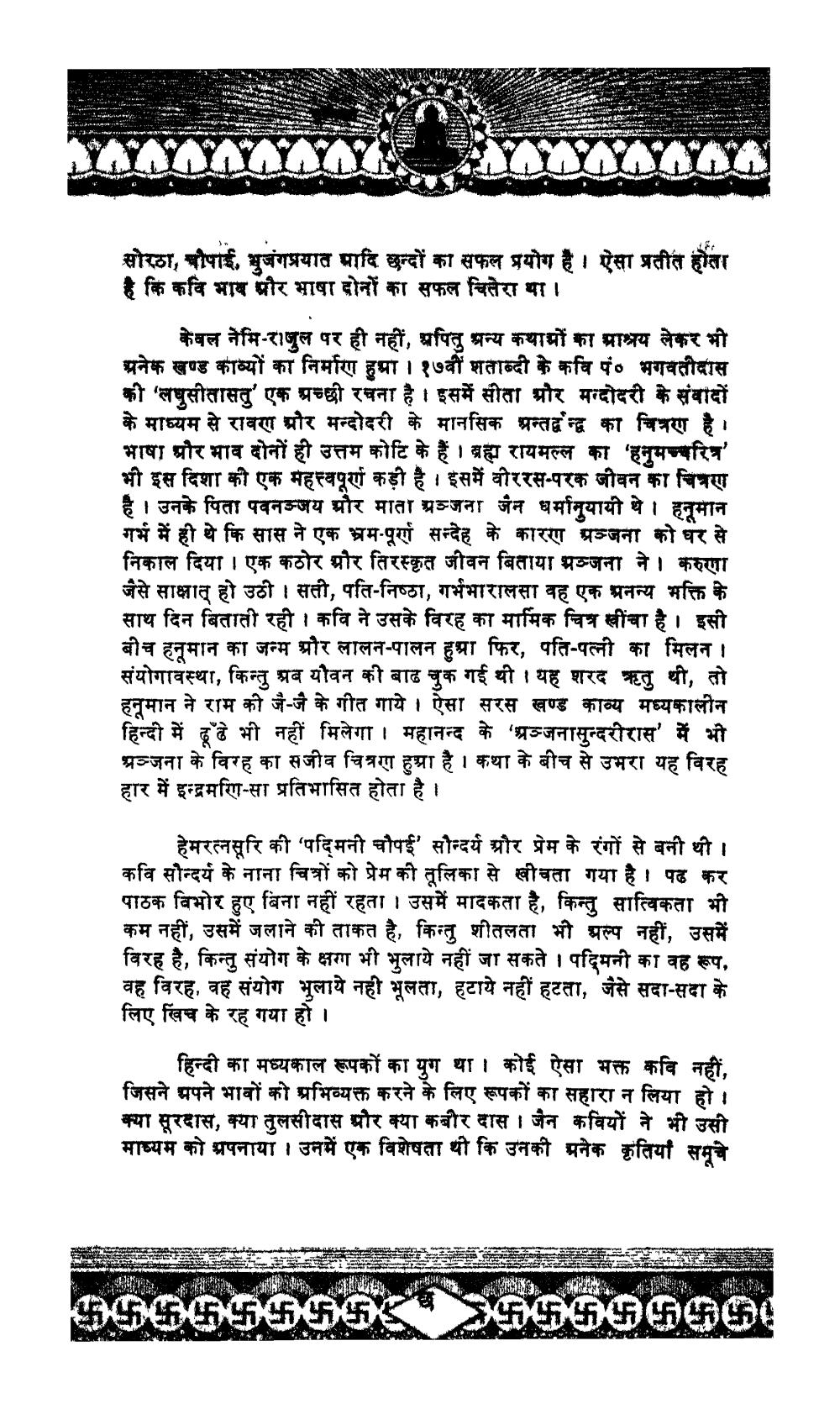________________
सोरठा, चौपाई, भुजंगप्रयात मादि छन्दों का सफल प्रयोग है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि भाव और भाषा दोनों का सफल चितेरा था ।
केवल म राजुल पर ही नहीं, अपितु अन्य कथाओं का प्राश्रय लेकर भी अनेक खण्ड काव्यों का निर्माण हुआ । १७वीं शताब्दी के कवि पं० भगवतीदास की 'लघुसीतास्तु' एक अच्छी रचना है। इसमें सीता भोर मन्दोदरी के संवादों के माध्यम से रावण और मन्दोदरी के मानसिक प्रन्तर्द्वन्द्व का चित्रण है भाषा और भाव दोनों ही उत्तम कोटि के हैं। ब्रह्म रायमल्ल का 'हनुमच्चरित्र' भी इस दिशा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें वीररस-परक जीवन का चित्रण है । उनके पिता पवनञ्जय और माता अञ्जना जैन धर्मानुयायी थे । हनूमान गर्भ में ही थे कि सास ने एक भ्रम पूर्ण सन्देह के कारण प्रञ्जना को घर से निकाल दिया । एक कठोर और तिरस्कृत जीवन बिताया भञ्जना ने । करुणा जैसे साक्षात् हो उठी । सती, पति-निष्ठा, गर्भभारालसा वह एक अनन्य भक्ति के साथ दिन बिताती रही । कवि ने उसके विरह का मार्मिक चित्र खींचा है। इसी बीच हनुमान का जन्म और लालन-पालन हुम्रा फिर, पति-पत्नी का मिलन | संयोगावस्था, किन्तु अब यौवन की बाढ चुक गई थी। यह शरद ऋतु थी, तो हनुमान ने राम की जै जै के गीत गाये । ऐसा सरस खण्ड काव्य मध्यकालीन हिन्दी में ढूढे भी नहीं मिलेगा । महानन्द के 'अञ्जना सुन्दरीरास' में भी अञ्जना के विरह का सजीव चित्रण हुआ है । कथा के बीच से उभरा यह विरह हार में इन्द्रमणि-सा प्रतिभासित होता है ।
हेमरत्नसूर की 'पद्मिनी चौपई' सौन्दर्य और प्रेम के रंगों से बनी थी । कवि सौन्दर्य के नाना चित्रों को प्रेम की तूलिका से खीचता गया है । पढ कर पाठक विभोर हुए बिना नहीं रहता । उसमें मादकता है, किन्तु सात्विकता भी कम नहीं, उसमें जलाने की ताकत है, किन्तु शीतलता भी अल्प नहीं, उसमें विरह है, किन्तु संयोग के क्षरण भी भुलाये नहीं जा सकते । पद्मिनी का वह रूप, वह विरह, वह संयोग भुलाये नही भूलता, हटाये नहीं हटता, जैसे सदा-सदा के लिए खिंच के रह गया हो ।
हिन्दी का मध्यकाल रूपकों का युग था । कोई ऐसा भक्त कवि नहीं, जिसने अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए रूपकों का सहारा न लिया हो । क्या सूरदास, क्या तुलसीदास और क्या कबीर दास । जैन कवियों ने भी उसी माध्यम को अपनाया । उनमें एक विशेषता थी कि उनकी अनेक कृतियां समूचे
$$$$5555
39666666