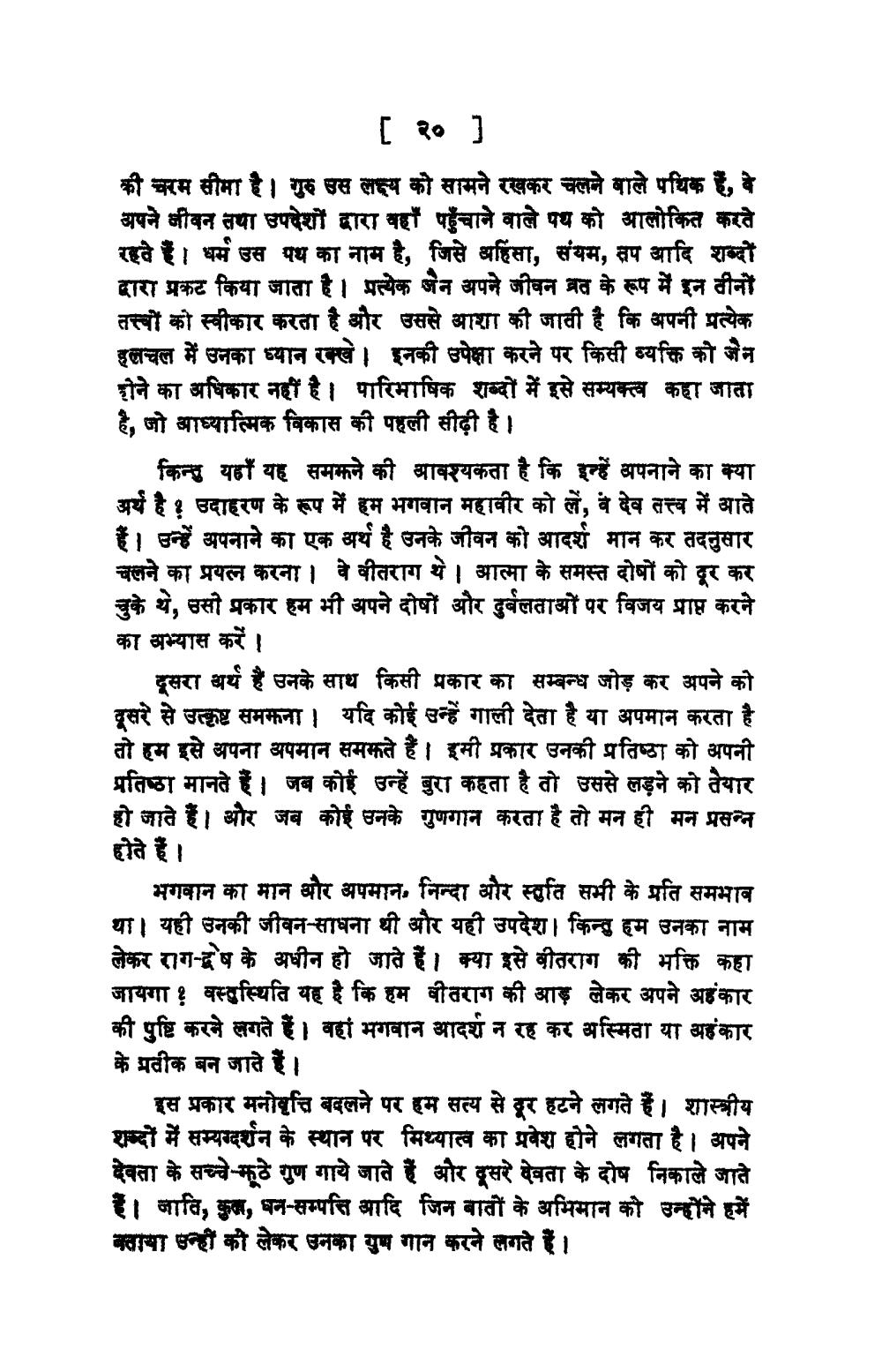________________
[ २० ] की चरम सीमा है। गुरु उस लक्ष्य को सामने रखकर चलने वाले पथिक है, वे अपने जीवन तथा उपदेशों द्वारा वहाँ पहुँचाने वाले पथ को आलोकित करते रहते हैं। धर्म उस पथ का नाम है, जिसे अहिंसा, संयम, तप आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रत्येक जैन अपने जीवन व्रत के रूप में इन तीनों तत्त्वों को स्वीकार करता है और उससे आशा की जाती है कि अपनी प्रत्येक इलचल में उनका ध्यान रक्खे। इनकी उपेक्षा करने पर किसी व्यक्ति को जैन होने का अधिकार नहीं है। पारिभाषिक शब्दों में इसे सम्यक्त्व कहा जाता है, जो आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी है।
किन्तु यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि इन्हें अपनाने का क्या अर्थ है ? उदाहरण के रूप में हम भगवान महावीर को लें, वे देव तत्त्व में आते हैं। उन्हें अपनाने का एक अर्थ है उनके जीवन को आदर्श मान कर तदनुसार चलने का प्रयल करना। वे वीतराग थे। आत्मा के समस्त दोषों को दूर कर चुके थे, उसी प्रकार हम भी अपने दोषों और दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करें।
दूसरा अर्थ है उनके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध जोड़ कर अपने को दूसरे से उत्कृष्ट समझना। यदि कोई उन्हें गाली देता है या अपमान करता है तो हम इसे अपना अपमान समझते हैं। इसी प्रकार उनकी प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। जब कोई उन्हें बुरा कहता है तो उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और जब कोई उनके गुणगान करता है तो मन ही मन प्रसन्न होते हैं।
भगवान का मान और अपमान. निन्दा और स्तुति सभी के प्रति समभाव था। यही उनकी जीवन-साधना थी और यही उपदेश। किन्तु हम उनका नाम लेकर राग-द्वेष के अधीन हो जाते हैं। क्या इसे वीतराग की भक्ति कहा जायगा ? वस्तुस्थिति यह है कि हम वीतराग की आड़ लेकर अपने अहंकार की पुष्टि करने लगते हैं। वहां भगवान आदर्श न रह कर अस्मिता या अहंकार के प्रतीक बन जाते हैं।
इस प्रकार मनोवृत्ति बदलने पर हम सत्य से दूर हटने लगते हैं। शास्त्रीय शब्दों में सम्यग्दर्शन के स्थान पर मिथ्यात्व का प्रवेश होने लगता है। अपने देवता के सच्चे-कुठे गुण गाये जाते हैं और दूसरे देवता के दोष निकाले जाते है। जाति, कुन, धन-सम्पत्ति आदि जिन बातों के अभिमान को उन्होंने हमें बताया उन्हीं को लेकर उनका गुण गान करने लगते हैं।