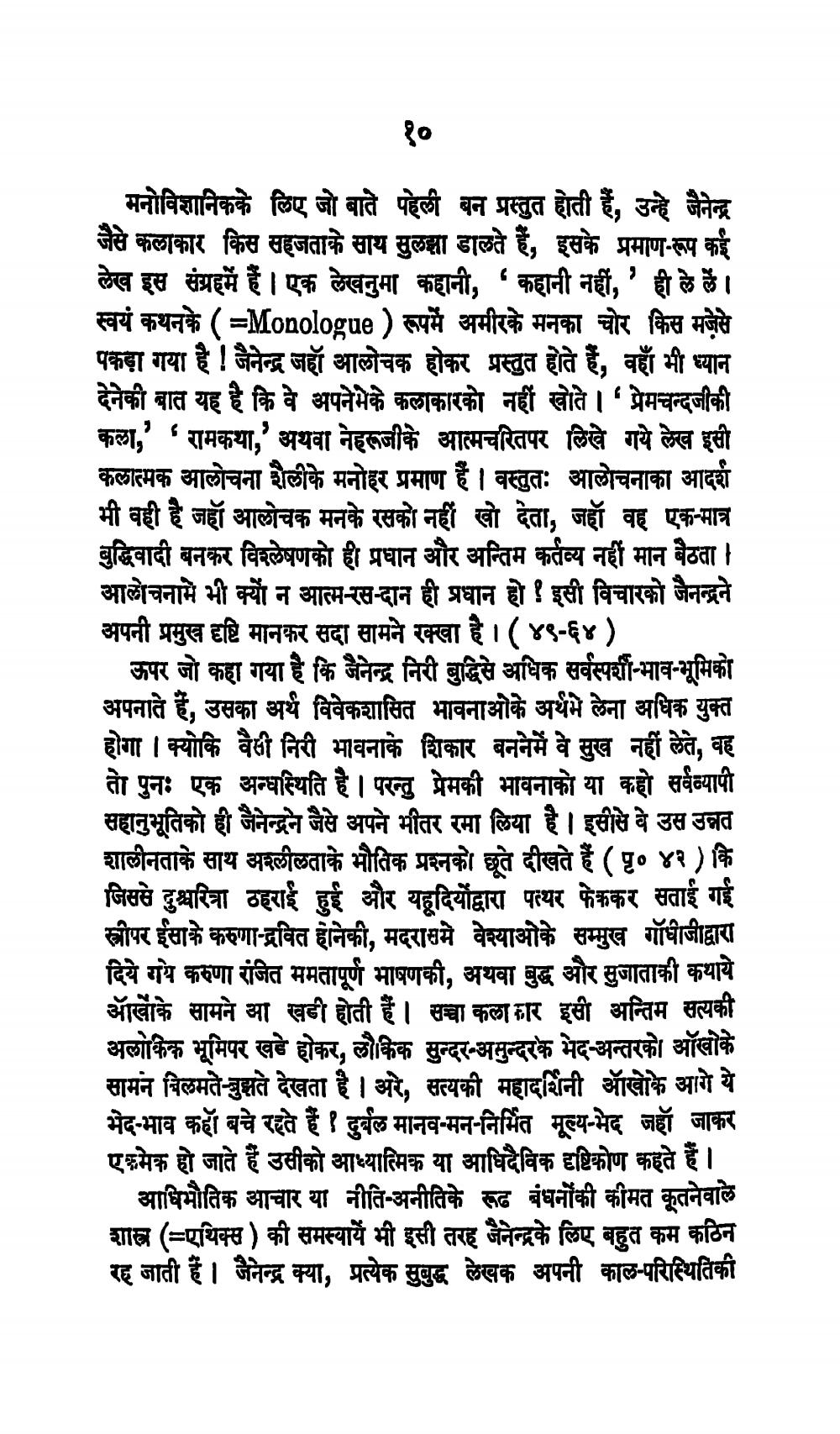________________
१०
मनोविज्ञानिकके लिए जो बाते पहेली बन प्रस्तुत होती हैं, उन्हे जैनेन्द्र जैसे कलाकार किस सहजता के साथ सुलझा डालते हैं, इसके प्रमाण रूप कई लेख इस संग्रहमें हैं । एक लेखनुमा कहानी, ' कहानी नहीं, ' ही ले लें। | स्वयं कथनके ( =Monologue) रूपमें अमीरके मनका चोर किस मज़ेसे पकड़ा गया है ! जैनेन्द्र जहाँ आलोचक होकर प्रस्तुत होते हैं, वहाँ भी ध्यान देनेकी बात यह है कि वे अपनेभेके कलाकारको नहीं खोते। ' प्रेमचन्दजीकी कला, ' ' रामकथा, ' अथवा नेहरूजीके आत्मचरितपर लिखे गये लेख इसी कलात्मक आलोचना शैलीके मनोहर प्रमाण हैं । वस्तुतः आलोचनाका आदर्श भी वही है जहाँ आलोचक मनके रसको नहीं खो देता, जहाँ वह एक मात्र बुद्धिवादी बनकर विश्लेषणको ही प्रधान और अन्तिम कर्तव्य नहीं मान बैठता । आलोचना भी क्यों न आत्म-रस-दान ही प्रधान हो ! इसी विचारको जैनन्द्रने अपनी प्रमुख दृष्टि मानकर सदा सामने रक्खा है । ( ४९-६४ )
ऊपर जो कहा गया है कि जैनेन्द्र निरी बुद्धिसे अधिक सर्वस्पर्शी भाव-भूमिको अपनाते हैं, उसका अर्थ विवेकशासित भावनाओके अर्थभे लेना अधिक युक्त होगा । क्योकि वैसी निरी भावनाके शिकार बननेमें वे सुख नहीं लेते, वह तो पुनः एक अन्धस्थिति है । परन्तु प्रेमकी भावनाको या कहो सर्वव्यापी सहानुभूतिको ही जैनेन्द्रने जैसे अपने भीतर रमा लिया है । इसीसे वे उस उन्नत 1 शालीनताके साथ अश्लीलताके भौतिक प्रश्नको छूते दीखते हैं ( पृ० ४२ ) कि जिससे दुश्चरित्रा ठहराई हुई और यहूदियोंद्वारा पत्थर फेककर सताई गई स्त्रीपर ईसा के करुणा-द्रवित होनेकी, मदरासमे वेश्याओके सम्मुख गॉधीजीद्वारा दिये गये करुणा रंजित ममतापूर्ण भाषणकी, अथवा बुद्ध और सुजाताकी कथाये आँखाके सामने आ खड़ी होती हैं । सच्चा कलाकार इसी अन्तिम सत्यकी अलोकिक भूमिपर खडे होकर, लौकिक सुन्दर - अमुन्दरके भेद अन्तरको आँखो के सामन चिलमते- बुझते देखता है । अरे, सत्यकी महादर्शिनी आँखो के आगे ये भेद-भाव कहाँ बचे रहते हैं ? दुर्बल मानव-मन-निर्मित मूल्य-भेद जहाँ जाकर एकमेक हो जाते हैं उसीको आध्यात्मिक या आधिदैविक दृष्टिकोण कहते हैं ।
आधिभौतिक आचार या नीति- अनीतिके रूढ बंधनों की कीमत कूतनेवाले शास्त्र (= एथिक्स ) की समस्यायें भी इसी तरह जैनेन्द्रके लिए बहुत कम कठिन रह जाती हैं । जैनेन्द्र क्या, प्रत्येक सुबुद्ध लेखक अपनी काल-परिस्थितिकी