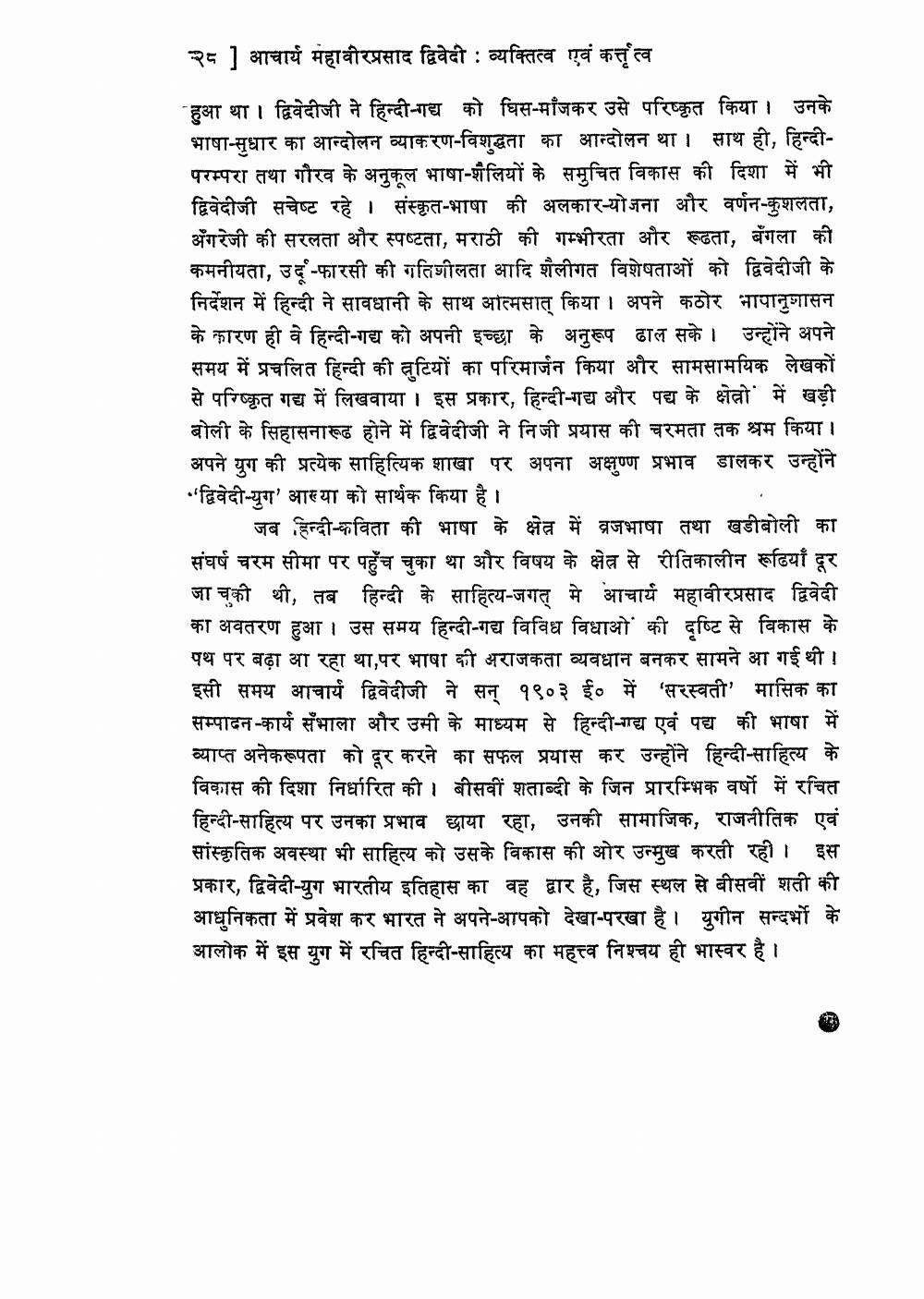________________
२८ ] आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व
दिशा में भी वर्णन - कुशलता,
हुआ था । द्विवेदीजी ने हिन्दी गद्य को घिस माँजकर उसे परिष्कृत किया। उनके भाषा-सुधार का आन्दोलन व्याकरण-विशुद्धता का आन्दोलन था । साथ ही, हिन्दीपरम्परा तथा गौरव के अनुकूल भाषा - शैलियों के समुचित विकास की द्विवेदीजी सचेष्ट रहे । संस्कृत भाषा की अलकार-योजना और अंगरेजी की सरलता और स्पष्टता, मराठी की गम्भीरता और रूढता, बँगला की कमनीयता, उर्दू-फारसी की गतिशीलता आदि शैलीगत विशेषताओं को द्विवेदीजी के निर्देशन में हिन्दी ने सावधानी के साथ आत्मसात् किया । अपने कठोर नापानुशासन के कारण ही वे हिन्दी गद्य को अपनी इच्छा के अनुरूप ढाल सके। उन्होंने अपने समय में प्रचलित हिन्दी की त्रुटियों का परिमार्जन किया और सामसामयिक लेखकों से परिष्कृत गद्य में लिखवाया । इस प्रकार, हिन्दी गद्य और पद्य के क्षेत्रों में खड़ी बोली के सिहासनारूढ होने में द्विवेदीजी ने निजी प्रयास की चरमता तक श्रम किया । अपने युग की प्रत्येक साहित्यिक शाखा पर अपना अक्षुण्ण प्रभाव डालकर उन्होंने " द्विवेदी युग' आख्या को सार्थक किया है ।
जब हिन्दी - कविता की भाषा के क्षेत्र में व्रजभाषा तथा खडीबोली का संघर्ष चरम सीमा पर पहुँच चुका था और विषय के क्षेत्र से रीतिकालीन रूढियाँ दूर जा चुकी थी, तब हिन्दी के साहित्य जगत् में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का अवतरण हुआ । उस समय हिन्दी गद्य विविध विधाओं की दृष्टि से विकास के पथ पर बढ़ा आ रहा था, पर भाषा की अराजकता व्यवधान बनकर सामने आ गई थी । इसी समय आचार्य द्विवेदीजी ने सन् १९०३ ई० में 'सरस्वती' मासिक का सम्पादन कार्य सँभाला और उसी के माध्यम से हिन्दी गद्य एवं पद्य की भाषा में व्याप्त अनेकरूपता को दूर करने का सफल प्रयास कर उन्होंने हिन्दी - साहित्य के विकास की दिशा निर्धारित की । बीसवीं शताब्दी के जिन प्रारम्भिक वर्षो में रचित हिन्दी साहित्य पर उनका प्रभाव छाया रहा, उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अवस्था भी साहित्य को उसके विकास की ओर उन्मुख करती रही । इस प्रकार, द्विवेदी युग भारतीय इतिहास का वह द्वार है, जिस स्थल से बीसवीं शती की आधुनिकता में प्रवेश कर भारत ने अपने-आपको देखा-परखा है । युगीन सन्दर्भों के आलोक में इस युग में रचित हिन्दी - साहित्य का महत्त्व निश्चय ही भास्वर है ।