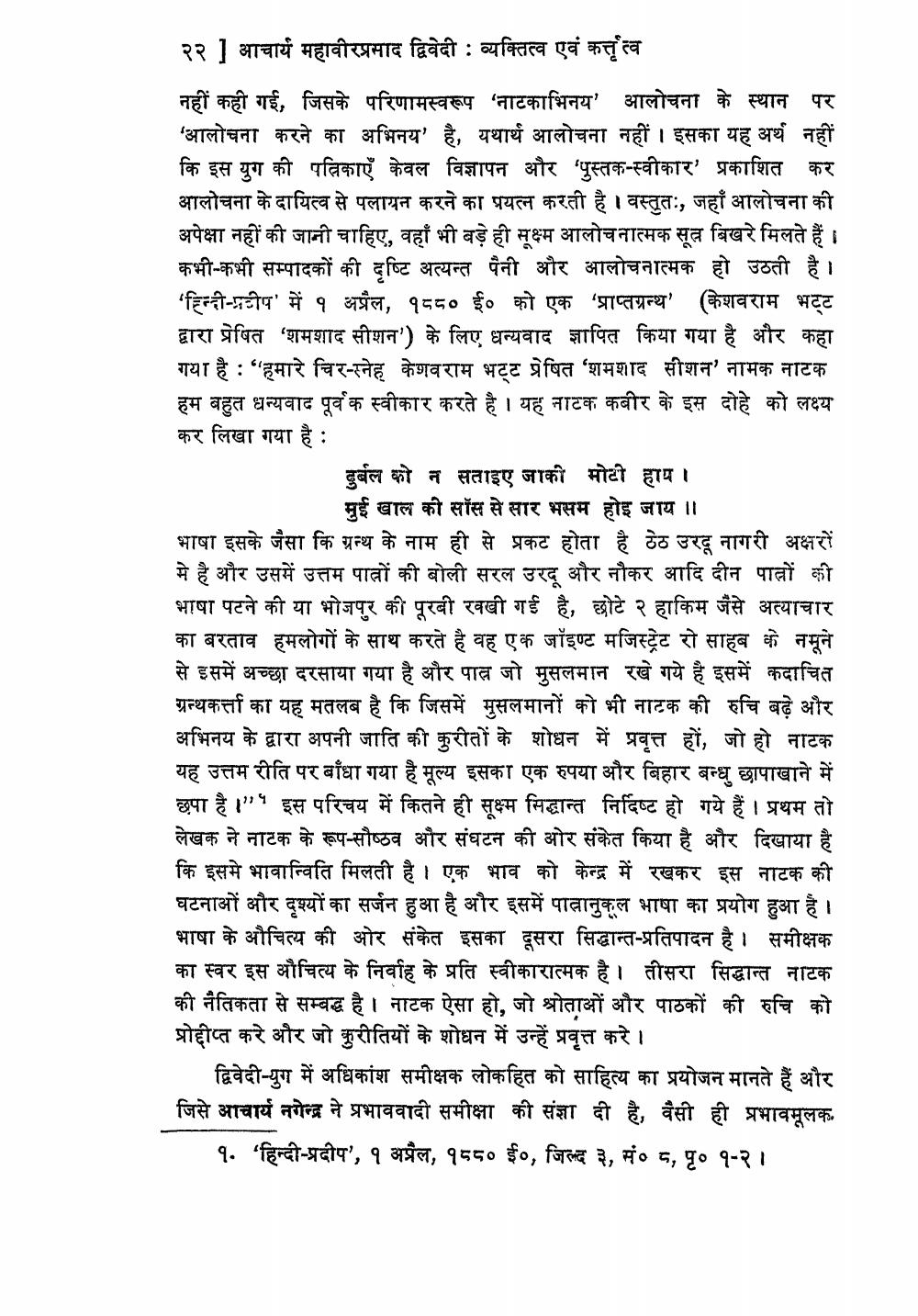________________
२२ ] आचार्य महावीरप्रमाद द्विवेदी : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व नहीं कही गई, जिसके परिणामस्वरूप 'नाटकाभिनय' आलोचना के स्थान पर 'आलोचना करने का अभिनय' है, यथार्थ आलोचना नहीं । इसका यह अर्थ नहीं कि इस युग की पत्रिकाएँ केवल विज्ञापन और 'पुस्तक-स्वीकार' प्रकाशित कर आलोचना के दायित्व से पलायन करने का प्रयत्न करती है । वस्तुतः, जहाँ आलोचना की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वहाँ भी बड़े ही सूक्ष्म आलोचनात्मक सूत्र बिखरे मिलते हैं । कभी-कभी सम्पादकों की दृष्टि अत्यन्त पैनी और आलोचनात्मक हो उठती है। 'हिन्दी-प्रटीप' में १ अप्रैल, १८८० ई० को एक 'प्राप्तग्रन्थ' (केशवराम भट्ट द्वारा प्रेषित 'शमशाद सीशन') के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया है और कहा गया है : "हमारे चिर-स्नेह केशवराम भट्ट प्रेषित 'शमशाद सीशन' नामक नाटक हम बहुत धन्यवाद पूर्वक स्वीकार करते है। यह नाटक कबीर के इस दोहे को लक्ष्य कर लिखा गया है :
दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय ।
मुई खाल की सॉस से सार भसम होइ जाय ।। भाषा इसके जैसा कि ग्रन्थ के नाम ही से प्रकट होता है ठेठ उरदू नागरी अक्षरों मे है और उसमें उत्तम पात्रों की बोली सरल उरदू और नौकर आदि दीन पात्रों की भाषा पटने की या भोजपुर की पूरबी रवखी गई है, छोटे २ हाकिम जैसे अत्याचार का बरताव हमलोगों के साथ करते है वह एक जॉइण्ट मजिस्ट्रेट रो साहब के नमूने से इसमें अच्छा दरसाया गया है और पात्र जो मुसलमान रखे गये है इसमें कदाचित ग्रन्थकर्ता का यह मतलब है कि जिसमें मुसलमानों को भी नाटक की रुचि बढ़े और अभिनय के द्वारा अपनी जाति की कुरीतों के शोधन में प्रवृत्त हों, जो हो नाटक यह उत्तम रीति पर बाँधा गया है मूल्य इसका एक रुपया और बिहार बन्धु छापाखाने में छपा है।'' इस परिचय में कितने ही सूक्ष्म सिद्धान्त निर्दिष्ट हो गये हैं । प्रथम तो लेखक ने नाटक के रूप-सौष्ठव और संघटन की ओर संकेत किया है और दिखाया है कि इसमे भावान्विति मिलती है। एक भाव को केन्द्र में रखकर इस नाटक की घटनाओं और दृश्यों का सर्जन हुआ है और इसमें पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा के औचित्य की ओर संकेत इसका दूसरा सिद्धान्त-प्रतिपादन है। समीक्षक का स्वर इस औचित्य के निर्वाह के प्रति स्वीकारात्मक है। तीसरा सिद्धान्त नाटक की नैतिकता से सम्बद्ध है। नाटक ऐसा हो, जो श्रोताओं और पाठकों की रुचि को प्रोद्दीप्त करे और जो कुरीतियों के शोधन में उन्हें प्रवृत्त करे।
द्विवेदी-युग में अधिकांश समीक्षक लोकहित को साहित्य का प्रयोजन मानते हैं और जिसे आचार्य नगेन्द्र ने प्रभाववादी समीक्षा की संज्ञा दी है, वैसी ही प्रभावमूलक
१. "हिन्दी-प्रदीप', १ अप्रैल, १८८० ई०, जिल्द ३, मं० ८, पृ० १-२।