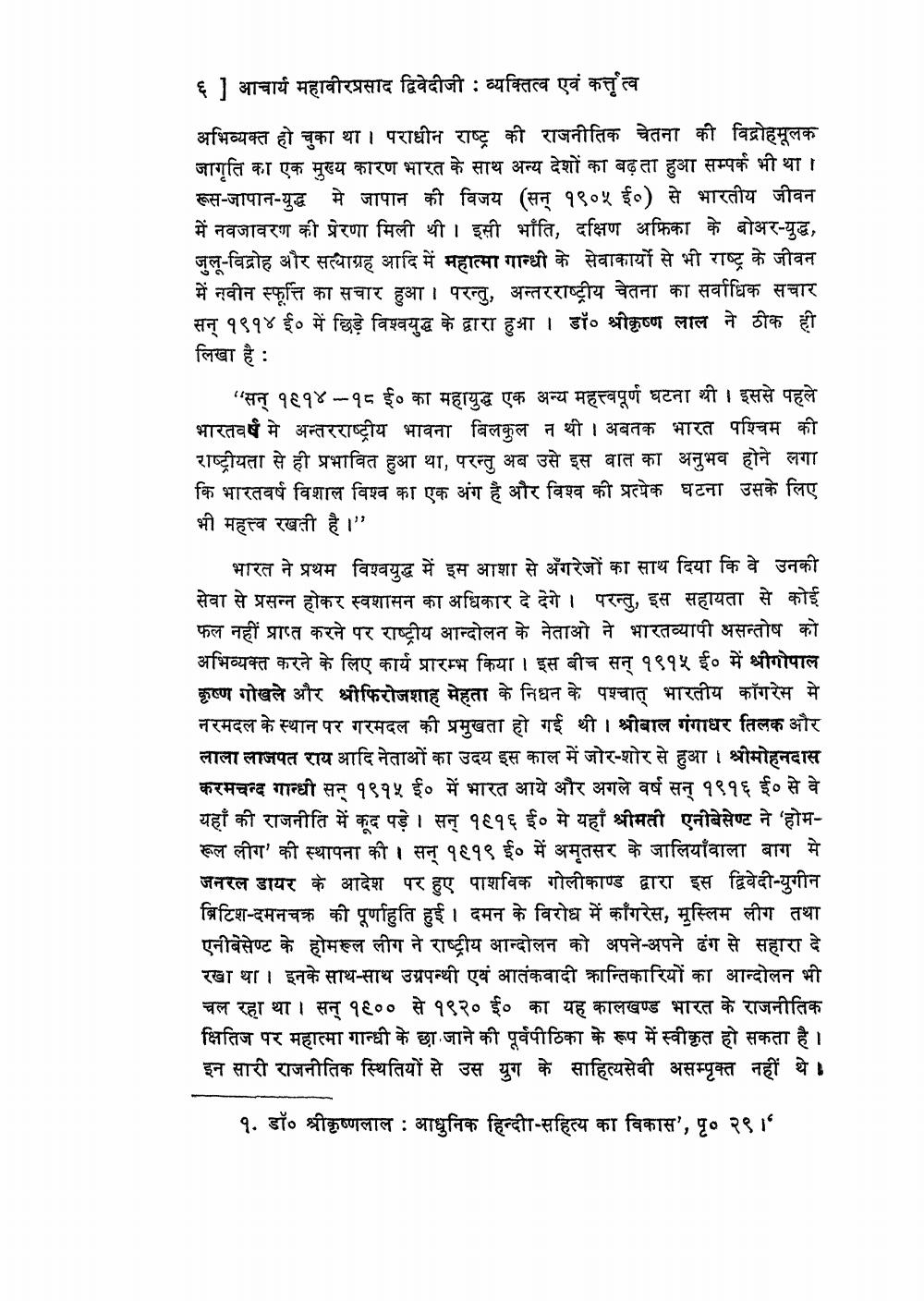________________
६] आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीजी : व्यक्तित्व एवं कर्त्तृत्व
अभिव्यक्त हो चुका था । पराधीन राष्ट्र की राजनीतिक चेतना की विद्रोहमूलक जागृति का एक मुख्य कारण भारत के साथ अन्य देशों का बढ़ता हुआ सम्पर्क भी था । रूस-जापान युद्ध मे जापान की विजय (सन् १९०५ ई० ) से भारतीय जीवन में नवजावरण की प्रेरणा मिली थी। इसी भाँति, दक्षिण अफ्रिका के बोअर युद्ध, जुलू - विद्रोह और सत्याग्रह आदि में महात्मा गान्धी के सेवाकार्यों से भी राष्ट्र के जीवन में नवीन स्फूर्ति का संचार हुआ । परन्तु अन्तरराष्ट्रीय चेतना का सर्वाधिक सचार सन् १९१४ ई० में छिड़े विश्वयुद्ध के द्वारा हुआ । डॉ० श्रीकृष्ण लाल ने ठीक ही लिखा है :
“सन् १९१४ - १८ ई० का महायुद्ध एक अन्य महत्त्वपूर्ण घटना थी । इससे पहले भारतवर्ष मे अन्तरराष्ट्रीय भावना बिलकुल न थी । अबतक भारत पश्चिम की राष्ट्रीयता से ही प्रभावित हुआ था, परन्तु अब उसे इस बात का अनुभव होने लगा कि भारतवर्ष विशाल विश्व का एक अंग है और विश्व की प्रत्येक घटना उसके लिए भी महत्त्व रखती है ।"
भारत ने प्रथम विश्वयुद्ध में इस आशा से अँगरेजों का साथ दिया कि वे उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वशासन का अधिकार दे देगे । परन्तु इस सहायता से कोई फल नहीं प्राप्त करने पर राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओ ने भारतव्यापी असन्तोष को अभिव्यक्त करने के लिए कार्य प्रारम्भ किया । इस बीच सन् १९१५ ई० में श्रीगोपाल कृष्ण गोखले और श्रीफिरोजशाह मेहता के निधन के पश्चात् भारतीय कॉगरेस मे नरमदल के स्थान पर गरमदल की प्रमुखता हो गई थी । श्रीबाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय आदि नेताओं का उदय इस काल में जोर-शोर से हुआ । श्रीमोहनदास करमचन्द गान्धी सन् १९१५ ई० में भारत आये और अगले वर्ष सन् १९१६ ई० से वे यहाँ की राजनीति में कूद पड़े । सन् १९१६ ई० मे यहाँ श्रीमती एनीबेसेण्ट ने 'होमरूल लीग' की स्थापना की । सन् १९१९ ई० में अमृतसर के जालियाँवाला बाग मे जनरल डायर के आदेश पर हुए पाशविक गोलीकाण्ड द्वारा इस द्विवेदी-युगीन ब्रिटिश- दमनचक्र की पूर्णाहुति हुई । दमन के विरोध में कॉंगरेस, मुस्लिम लीग तथा एनीबेसेण्ट के होमरूल लीग ने राष्ट्रीय आन्दोलन को अपने-अपने ढंग से सहारा दे रखा था। इनके साथ-साथ उग्रपन्थी एवं आतंकवादी क्रान्तिकारियों का आन्दोलन भी चल रहा था । सन् १९०० से १९२० ई० का यह कालखण्ड भारत के राजनीतिक क्षितिज पर महात्मा गान्धी के छा जाने की पूर्वपीठिका के रूप में स्वीकृत हो सकता है । इन सारी राजनीतिक स्थितियों से उस युग के साहित्यसेवी असम्पृक्त नहीं थे ।
१. डॉ० श्रीकृष्णलाल : आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास', पृ० २९ ।