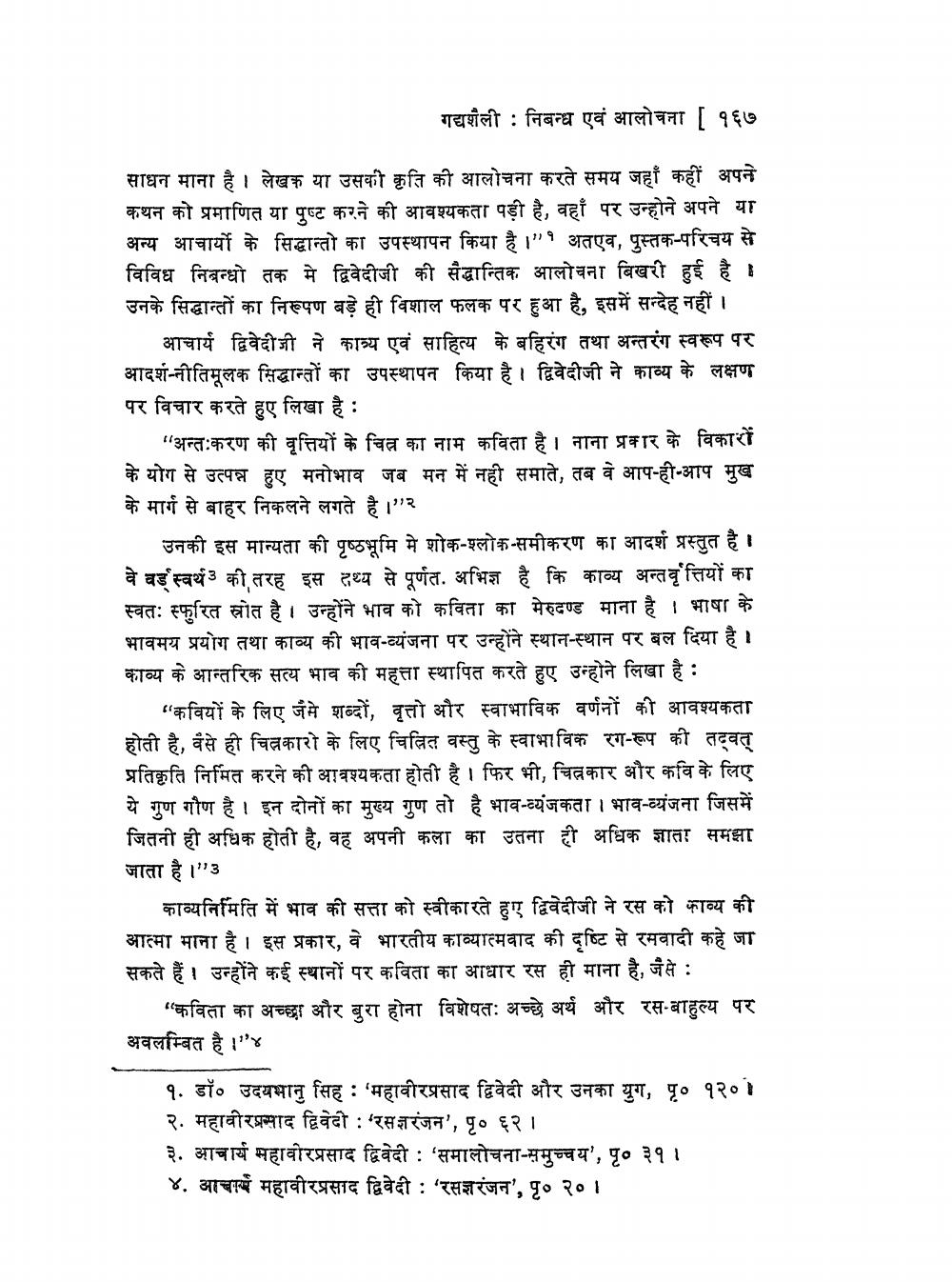________________
गद्यशैली : निबन्ध एवं आलोचना [ १६७
साधन माना है । लेखक या उसकी कृति की आलोचना करते समय जहाँ कहीं अपने कथन को प्रमाणित या पुष्ट करने की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ पर उन्होने अपने या अन्य आचार्यो के सिद्धान्तो का उपस्थापन किया है ।" १ अतएव, पुस्तक परिचय से विविध निबन्धो तक मे द्विवेदीजी की सैद्धान्तिक आलोचना बिखरी हुई है । उनके सिद्धान्तों का निरूपण बड़े ही विशाल फलक पर हुआ है, इसमें सन्देह नहीं ।
आचार्य द्विवेदीजी ने कात्र्य एवं साहित्य के बहिरंग तथा अन्तरंग स्वरूप पर आदर्श - नीतिमूलक सिद्धान्तों का उपस्थापन किया है । द्विवेदीजी ने काव्य के लक्षण पर विचार करते हुए लिखा है :
"अन्तःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है । नाना प्रकार के विकारों के योग से उत्पन्न हुए मनोभाव जब मन में नही समाते, तब वे आप ही आप मुख के मार्ग से बाहर निकलने लगते है । २
उनकी इस मान्यता की पृष्ठभूमि मे शोक - श्लोक - समीकरण का आदर्श प्रस्तुत है । वे व स्वर्थ की तरह इस तथ्य से पूर्णत अभिज्ञ है कि काव्य अन्तर्वृत्तियों का स्वतः स्फुरित स्रोत है। उन्होंने भाव को कविता का मेरुदण्ड माना है । भाषा के भावमय प्रयोग तथा काव्य की भाव-व्यंजना पर उन्होंने स्थान-स्थान पर बल दिया है । काव्य के आन्तरिक सत्य भाव की महत्ता स्थापित करते हुए उन्होने लिखा है :
" कवियों के लिए जैसे शब्दों, वृत्तो और स्वाभाविक वर्णनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही चित्रकारो के लिए चित्रित वस्तु के स्वाभाविक रंग-रूप की तद्वत् प्रतिकृति निर्मित करने की आवश्यकता होती है। फिर भी, चित्रकार और कवि के लिए ये गुण गौण है। इन दोनों का मुख्य गुण तो है भाव व्यंजकता । भाव-व्यंजना जिसमें जितनी ही अधिक होती है, वह अपनी कला का उतना ही अधिक ज्ञाता समझा जाता है। 3
काव्यनिर्मिति में भाव की सत्ता को स्वीकारते हुए द्विवेदीजी ने रस को काव्य की आत्मा माना है । इस प्रकार, वे भारतीय काव्यात्मवाद की दृष्टि से रमवादी कहे जा सकते हैं । उन्होंने कई स्थानों पर कविता का आधार रस ही माना है, जैसे :
" कविता का अच्छा और बुरा होना विशेषतः अच्छे अर्थ और रस- बाहुल्य पर अवलम्बित है । ४
१. डॉ० उदयभानु सिंह : 'महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग, पृ० १२० ॥ २. महावीरप्रसाद द्विवेदी : 'रसज्ञरंजन', पृ० ६२ ।
३. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : 'समालोचना-समुच्चय', पृ० ३१ ।
४. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : 'रसज्ञरंजन', पृ० २० ।