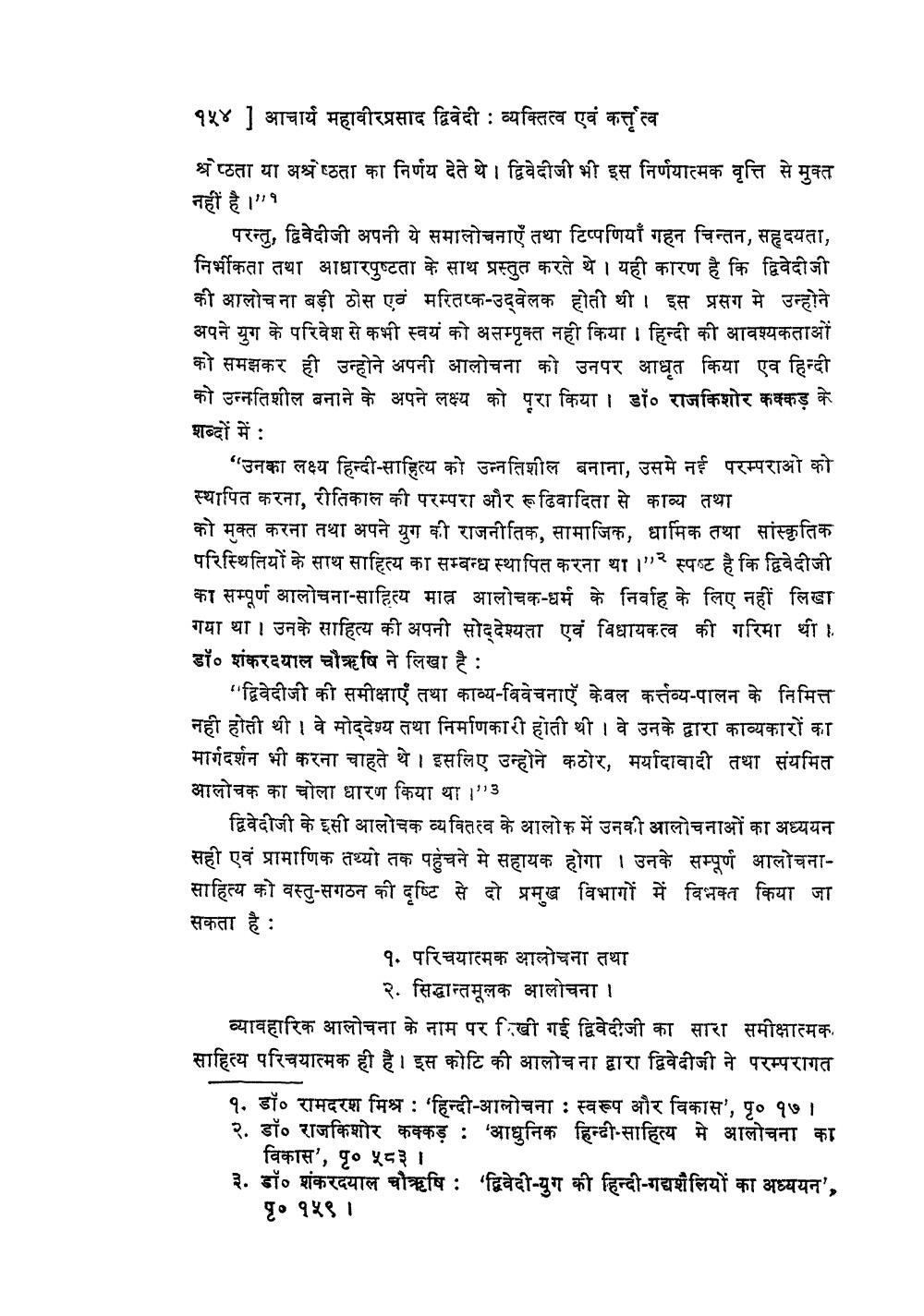________________
१५४ ] आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता का निर्णय देते थे। द्विवेदीजी भी इस निर्णयात्मक वृत्ति से मुक्त नहीं है।"
परन्तु, द्विवेदीजी अपनी ये समालोचनाएँ तथा टिप्पणियाँ गहन चिन्तन, सहृदयता, निर्भीकता तथा आधारपुष्टता के साथ प्रस्तुत करते थे। यही कारण है कि द्विवेदीजी की आलोचना बड़ी ठोस एवं मरितप्क-उद्वेलक होती थी। इस प्रसग मे उन्होने अपने युग के परिवेश से कभी स्वयं को असम्पृक्त नहीं किया । हिन्दी की आवश्यकताओं को समझकर ही उन्होने अपनी आलोचना को उनपर आधृत किया एव हिन्दी को उन्नतिशील बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा किया। डॉ० राजकिशोर कक्कड़ के शब्दों में: ___ "उनका लक्ष्य हिन्दी-साहित्य को उन्नतिशील बनाना, उसमे नई परम्पराओ को स्थापित करना, रीतिकाल की परम्परा और रूढिवादिता से काव्य तथा को मुक्त करना तथा अपने युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ साहित्य का सम्बन्ध स्थापित करना था।"२ स्पष्ट है कि द्विवेदीजी का सम्पूर्ण आलोचना-साहित्य मात्र आलोचक-धर्म के निर्वाह के लिए नहीं लिखा गया था। उनके साहित्य की अपनी सोद्देश्यता एवं विधायकत्व की गरिमा थी। डॉ० शंकरदयाल चौऋषि ने लिखा है :
"द्विवेदीजी की समीक्षाएं तथा काव्य-विवेचनाएँ केवल कर्त्तव्य-पालन के निमित्त नहीं होती थी। वे मोद्देश्य तथा निर्माणकारी होती थी। वे उनके द्वारा काव्यकारों का मार्गदर्शन भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होने कठोर, मर्यादावादी तथा संयमित आलोचक का चोला धारण किया था।"3
द्विवेदीजी के इसी आलोचक व्यक्तित्व के आलोक में उनकी आलोचनाओं का अध्ययन सही एवं प्रामाणिक तथ्यो तक पहुंचने मे सहायक होगा । उनके सम्पूर्ण आलोचनासाहित्य को वस्तु-सगठन की दृष्टि से दो प्रमुख विभागों में विभक्त किया जा सकता है :
१. परिचयात्मक आलोचना तथा
२. सिद्धान्तमूलक आलोचना । व्यावहारिक आलोचना के नाम पर लिखी गई द्विवेदीजी का सारा समीक्षात्मक, साहित्य परिचयात्मक ही है। इस कोटि की आलोचना द्वारा द्विवेदीजी ने परम्परागत
१. डॉ० रामदरश मिश्र : 'हिन्दी-आलोचना : स्वरूप और विकास', पृ० १७ । २. डॉ० राजकिशोर कक्कड़ : 'आधुनिक हिन्दी-साहित्य मे आलोचना का
विकास', पृ० ५८३ । ३. डॉ० शंकरदयाल चौऋषि : 'द्विवेदी-युग की हिन्दी-गद्यशैलियों का अध्ययन',
पृ० १५९ ।