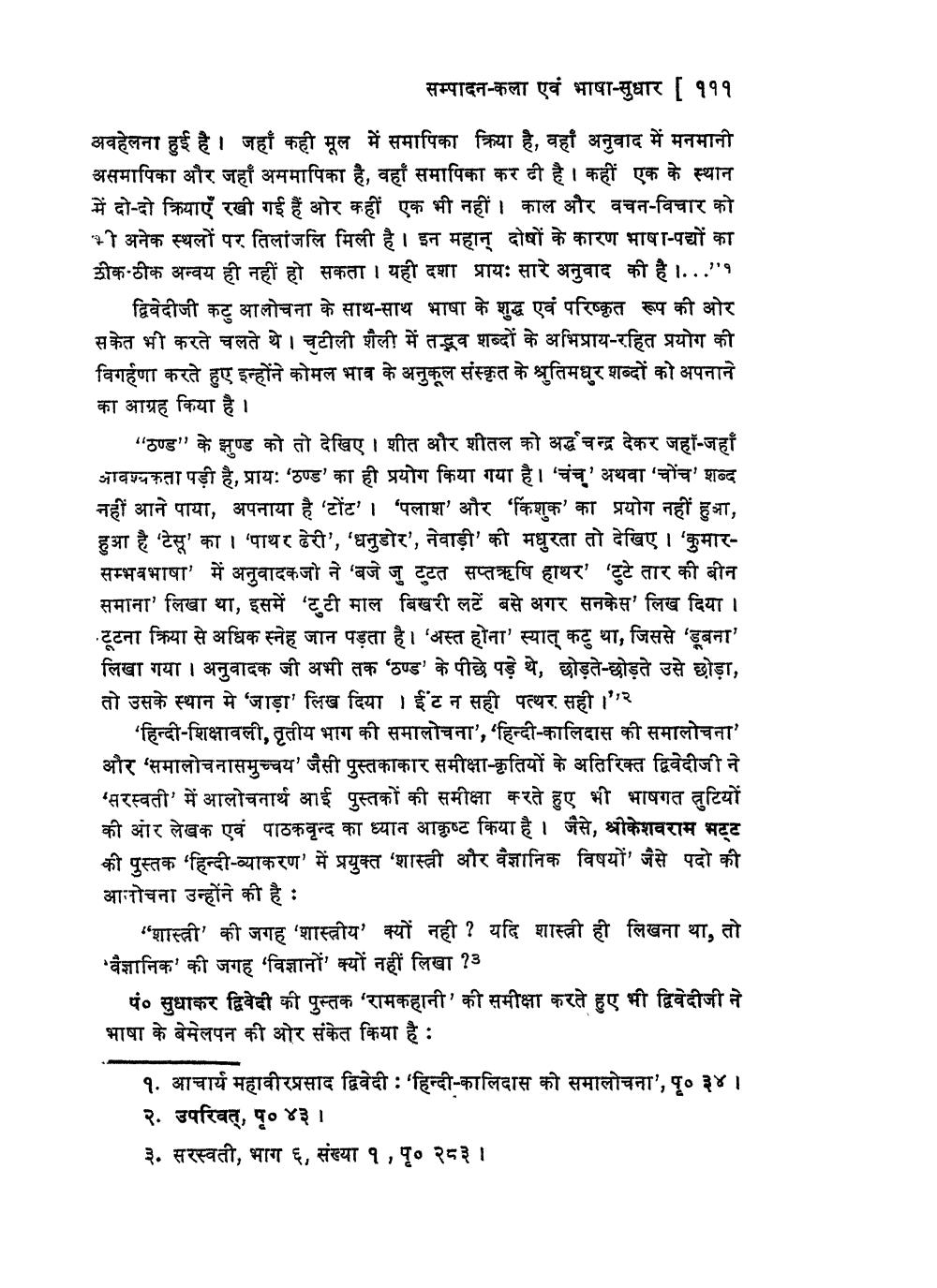________________
सम्पादन-कला एवं भाषा-सुधार [ १११ अवहेलना हुई है। जहाँ कही मूल में समापिका क्रिया है, वहाँ अनुवाद में मनमानी असमापिका और जहाँ अममापिका है, वहाँ समापिका कर दी है। कहीं एक के स्थान में दो-दो क्रियाएँ रखी गई हैं ओर कहीं एक भी नहीं। काल और वचन-विचार को की अनेक स्थलों पर तिलांजलि मिली है। इन महान् दोषों के कारण भाषा-पद्यों का ठीक-ठीक अन्वय ही नहीं हो सकता । यही दशा प्रायः सारे अनुवाद की है।..."१
द्विवेदीजी कटु आलोचना के साथ-साथ भाषा के शुद्ध एवं परिष्कृत रूप की ओर सकेत भी करते चलते थे। चुटीली शैली में तद्भव शब्दों के अभिप्राय-रहित प्रयोग की विगर्हणा करते हुए इन्होंने कोमल भाव के अनुकूल संस्कृत के श्रुतिमधुर शब्दों को अपनाने का आग्रह किया है।
"ठण्ड" के झुण्ड को तो देखिए । शीत और शीतल को अर्द्ध चन्द्र देकर जहाँ-जहाँ आवश्यकता पड़ी है, प्रायः 'ठण्ड' का ही प्रयोग किया गया है। 'चंच' अथवा 'चोंच' शब्द नहीं आने पाया, अपनाया है 'टोंट'। "पलाश' और 'किंशुक' का प्रयोग नहीं हुआ, हुआ है 'टेसू' का । 'पाथर ढेरी', 'धनुडोर', नेवाड़ी' की मधुरता तो देखिए । 'कुमारसम्भवभाषा' में अनुवादकजो ने 'बजे जु टुटत सप्तऋषि हाथर' 'टुटे तार की बीन समाना' लिखा था, इसमें 'टुटी माल बिखरी लटें बसे अगर सनकेस' लिख दिया । टूटना क्रिया से अधिक स्नेह जान पड़ता है। 'अस्त होना' स्यात् कटु था, जिससे 'डूबना' लिखा गया। अनुवादक जी अभी तक 'ठण्ड' के पीछे पड़े थे, छोड़ते-छोड़ते उसे छोड़ा, तो उसके स्थान मे 'जाड़ा' लिख दिया । ईंट न सही पत्थर सही।।२ _ 'हिन्दी-शिक्षावली, तृतीय भाग की समालोचना','हिन्दी-कालिदास की समालोचना' और 'समालोचनासमुच्चय' जैसी पुस्तकाकार समीक्षा-कृतियों के अतिरिक्त द्विवेदीजी ने 'सरस्वती' में आलोचनार्थ आई पुस्तकों की समीक्षा करते हुए भी भाषगत त्रुटियों की ओर लेखक एवं पाठकवृन्द का ध्यान आकृष्ट किया है । जैसे, श्रीकेशवराम भट्ट की पुस्तक 'हिन्दी-व्याकरण' में प्रयुक्त 'शास्त्री और वैज्ञानिक विषयों' जैसे पदो की आलोचना उन्होंने की है : __ "शास्त्री' की जगह 'शास्त्रीय' क्यों नही ? यदि शास्त्री ही लिखना था, तो 'वैज्ञानिक' की जगह 'विज्ञानों' क्यों नहीं लिखा ?3
पं० सुधाकर द्विवेदी की पुस्तक 'रामकहानी' की समीक्षा करते हुए भी द्विवेदीजी ने भाषा के बेमेलपन की ओर संकेत किया है :
१. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : 'हिन्दी-कालिदास को समालोचना', पृ० ३४ । २. उपरिवत्, पृ० ४३ । ३. सरस्वती, भाग ६, संख्या १, पृ० २८३ ।