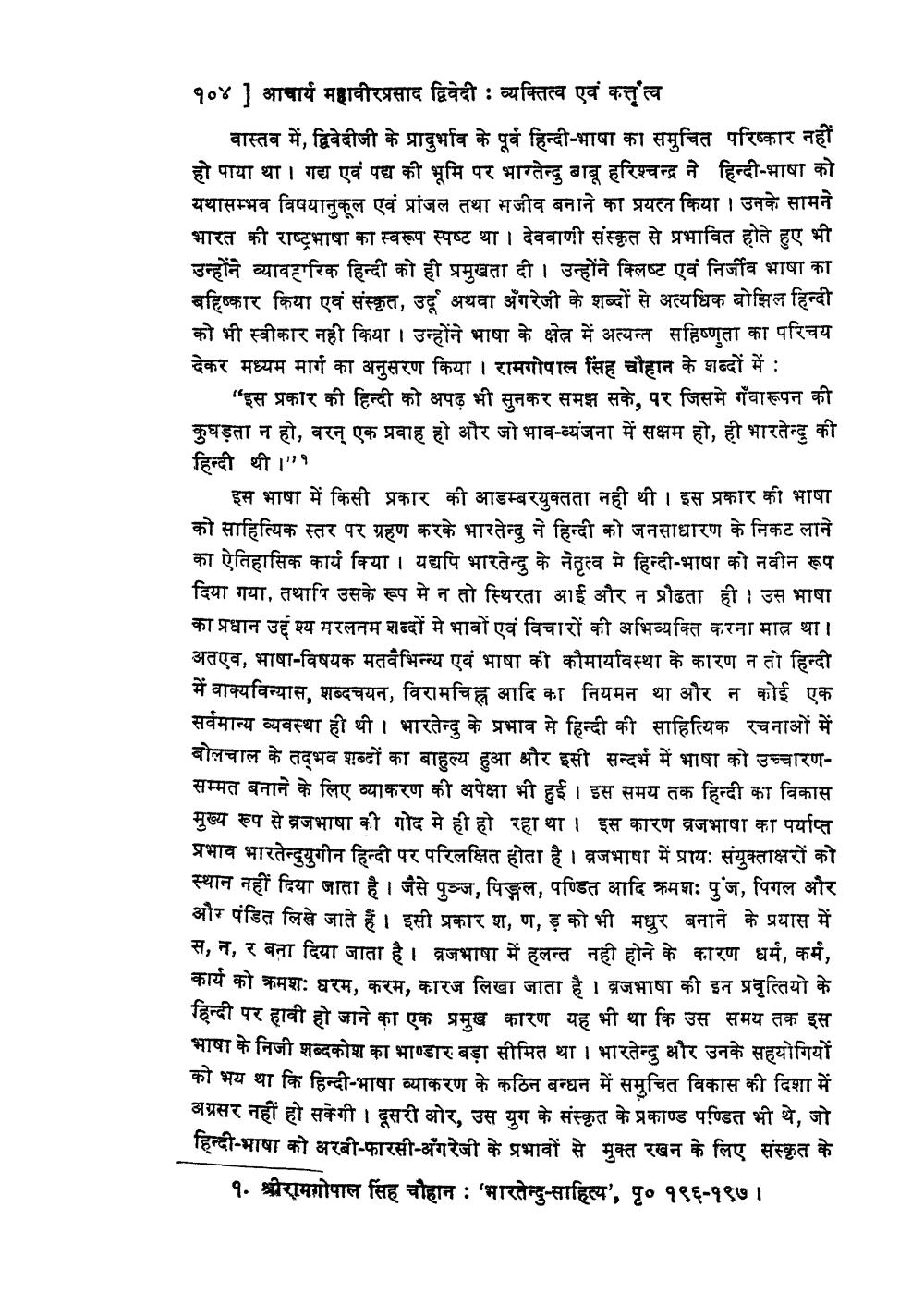________________
१०४ ] आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व
वास्तव में, द्विवेदीजी के प्रादुर्भाव के पूर्व हिन्दी-भाषा का समुचित परिष्कार नहीं हो पाया था। गद्य एवं पद्य की भूमि पर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने हिन्दी-भाषा को यथासम्भव विषयानुकूल एवं प्रांजल तथा मजीव बनाने का प्रयत्न किया। उनके सामने भारत की राष्ट्रभाषा का स्वरूप स्पष्ट था। देववाणी संस्कृत से प्रभावित होते हुए भी उन्होंने व्यावहारिक हिन्दी को ही प्रमुखता दी। उन्होंने क्लिष्ट एवं निर्जीव भाषा का बहिष्कार किया एवं संस्कृत, उर्दू अथवा अँगरेजी के शब्दों से अत्यधिक बोझिल हिन्दी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भाषा के क्षेत्र में अत्यन्त सहिष्णुता का परिचय देकर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। रामगोपाल सिंह चौहान के शब्दों में :
___ "इस प्रकार की हिन्दी को अपढ़ भी सुनकर समझ सके, पर जिसमे गँवारूपन की कुघड़ता न हो, वरन् एक प्रवाह हो और जो भाव-व्यंजना में सक्षम हो, ही भारतेन्दु की हिन्दी थी।"१
इस भाषा में किसी प्रकार की आडम्बरयुक्तता नही थी । इस प्रकार की भाषा को साहित्यिक स्तर पर ग्रहण करके भारतेन्दु ने हिन्दी को जनसाधारण के निकट लाने का ऐतिहासिक कार्य क्यिा । यद्यपि भारतेन्दु के नेतृत्व मे हिन्दी-भाषा को नवीन रूप दिया गया, तथापि उसके रूप मे न तो स्थिरता आई और न प्रौढता ही। उस भाषा का प्रधान उद्देश्य मरलतम शब्दों मे भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति करना मात्र था। अतएव, भाषा-विषयक मतभिन्न्य एवं भाषा की कौमार्यावस्था के कारण न तो हिन्दी में वाक्यविन्यास, शब्दचयन, विरामचिह्न आदि का नियमन था और न कोई एक सर्वमान्य व्यवस्था ही थी। भारतेन्दु के प्रभाव मे हिन्दी की साहित्यिक रचनाओं में बोलचाल के तद्भव शब्दों का बाहुल्य हुआ और इसी सन्दर्भ में भाषा को उच्चारणसम्मत बनाने के लिए व्याकरण की अपेक्षा भी हुई। इस समय तक हिन्दी का विकास मुख्य रूप से व्रजभाषा की गोद मे ही हो रहा था। इस कारण व्रजभाषा का पर्याप्त प्रभाव भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पर परिलक्षित होता है । व्रजभाषा में प्रायः संयुक्ताक्षरों को स्थान नहीं दिया जाता है । जैसे पुञ्ज, पिङ्गल, पण्डित आदि क्रमशः पुज, पिगल और
और पंडित लिखे जाते हैं। इसी प्रकार श, ण, ड़ को भी मधुर बनाने के प्रयास में स, न, र बना दिया जाता है। व्रजभाषा में हलन्त नही होने के कारण धर्म, कर्म, कार्य को क्रमश: धरम, करम, कारज लिखा जाता है । ब्रजभाषा की इन प्रवृत्तियो के रहन्दी पर हावी हो जाने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उस समय तक इस भाषा के निजी शब्दकोश का भाण्डार बड़ा सीमित था । भारतेन्दु और उनके सहयोगियों को भय था कि हिन्दी-भाषा व्याकरण के कठिन बन्धन में समुचित विकास की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकेगी। दूसरी ओर, उस युग के संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित भी थे, जो हिन्दी-भाषा को अरबी-फारसी-अंगरेजी के प्रभावों से मुक्त रखन के लिए संस्कृत के
१. श्रीरामगोपाल सिंह चौहान : 'भारतेन्दु-साहित्य', पृ० १९६-१९७ ।