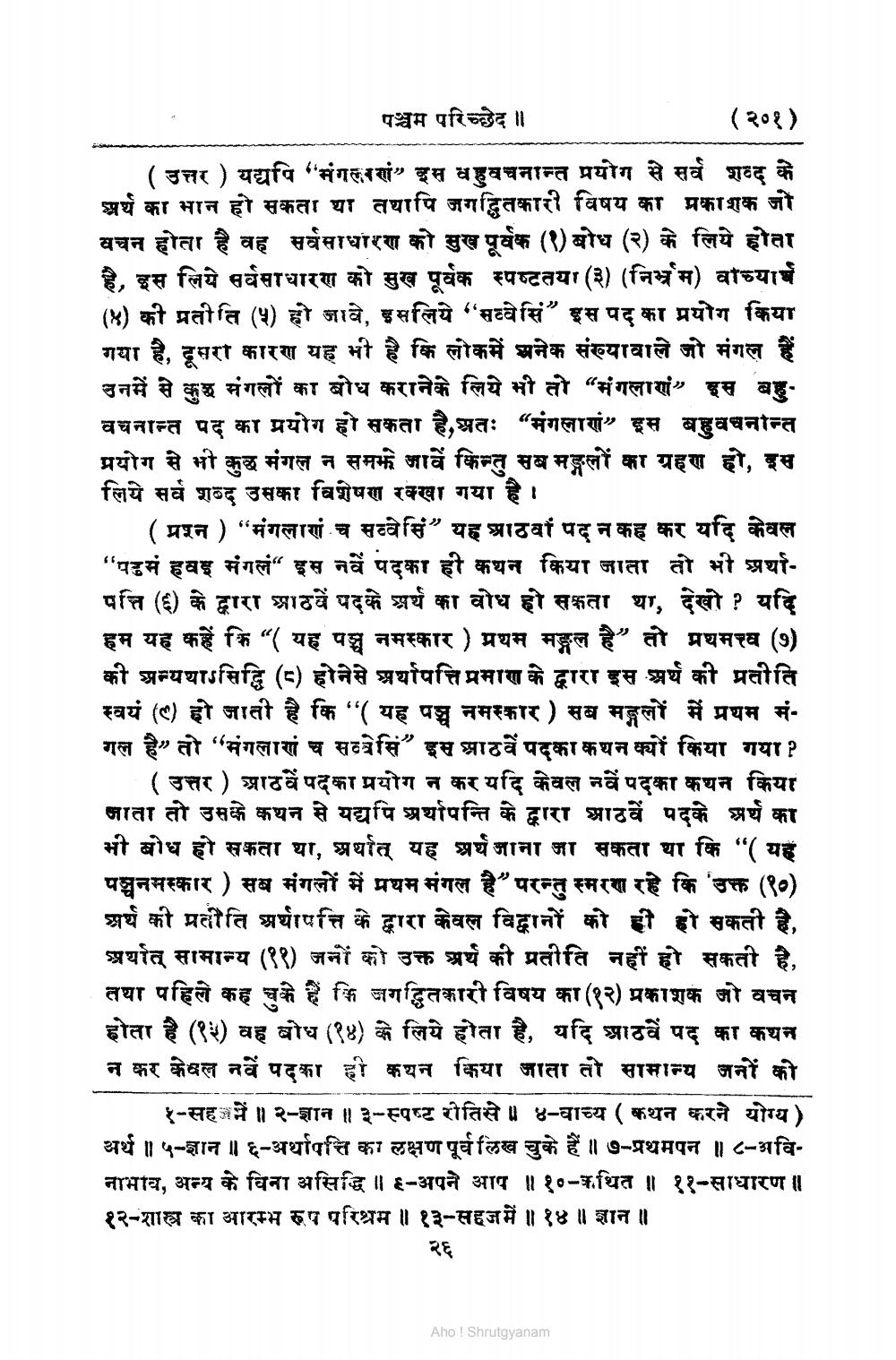________________
पञ्चम परिच्छेद ॥
(२०१) ( उत्तर ) यद्यपि “मंगलम” इस बहुवचनान्त प्रयोग से सर्व शब्द के अर्थ का भान हो सकता था तथापि जगद्वितकारी विषय का प्रकाशक जो वचन होता है वह सर्वसाधारण को सुख पूर्वक (१) बोध (२) के लिये होता है, इस लिये सर्वसाधारण को सुख पूर्वक स्पष्टतया (३) (निर्भम) वाच्या (४) की प्रतीति (५) हो जावे, इसलिये "सध्वेसिं” इस पद का प्रयोग किया गया है, दूसरा कारण यह भी है कि लोकमें अनेक संख्यावाले जो मंगल हैं उनमें से कुछ मंगलों का बोध करानेके लिये भी तो “मंगलाणं" इस बहु. वचनान्त पद का प्रयोग हो सकता है,अतः “मंगलाणं” इस बहुवचनान्त प्रयोग से भी कुछ मंगल न समझे जावें किन्तु सब मङ्गलों का ग्रहण हो, इस लिये सर्व शब्द उसका विशेषण रक्खा गया है।
(प्रश्न ) “मंगलाणं च सव्वेसिं" यह पाठवां पद न कह कर यदि केवल "पडम हवाइ मंगलं" इस नवें पदका ही कथन किया जाता तो भी अर्थापत्ति (६) के द्वारा पाठवें पदके अर्थ का वोध हो सकता था, देखो ? यदि हम यह कहें कि “( यह पञ्च नमस्कार ) प्रथम मङ्गल है" तो प्रथमत्त्व (9) की अन्यथासिद्धि (क) होनेसे अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा इस अर्थ की प्रतीति स्वयं (ए) हो जाती है कि "( यह पञ्च नमस्कार ) सब मङ्गलों में प्रथम मं. गल है" तो "मंगलाणं च सब्वेसिं” इस पाठवें पदका कथन क्यों किया गया?
( उत्तर ) आठवें पदका प्रयोग न कर यदि केवल नवें पदका कथन किया जाता तो उसके कथन से यद्यपि अर्थापन्ति के द्वारा आठवें पदके अर्थ का भी बोध हो सकता था, अर्थात् यह अर्थ जाना जा सकता था कि "( यह पञ्चनमस्कार ) सब मंगलों में प्रथम मंगल है" परन्तु स्मरण रहे कि 'उक्त (१०) अर्थ की प्रतीति अर्यापत्ति के द्वारा केवल विद्वानों को ही हो सकती है, अर्थात् सामान्य (११) जनों को उक्त अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है, तथा पहिले कह चुके हैं कि जगद्वितकारी विषय का (१२) प्रकाशक जो वचन होता है (१३) वह बोध (१४) के लिये होता है, यदि आठवें पद का कथन न कर केवल नवें पदका ही कथन किया जाता तो सामान्य जनों को
-सहज ॥२-ज्ञान ॥३-स्पष्ट रोतिसे ॥ ४-वाच्य (कथन करने योग्य) अर्थ ॥ ५-ज्ञान ॥ ६-अर्थापत्ति का लक्षण पूर्व लिख चुके हैं ॥ ७-प्रथमपन ॥ ८-अविनाभाव, अन्य के विना असिद्धि ॥ 8-अपने आप ॥१०-कथित ॥ ११-साधारण ।। १२-शास्त्र का आरम्भ रूप परिश्रम ॥ १३-सहज में ॥ १४ ॥ ज्ञान ॥
Aho! Shrutgyanam