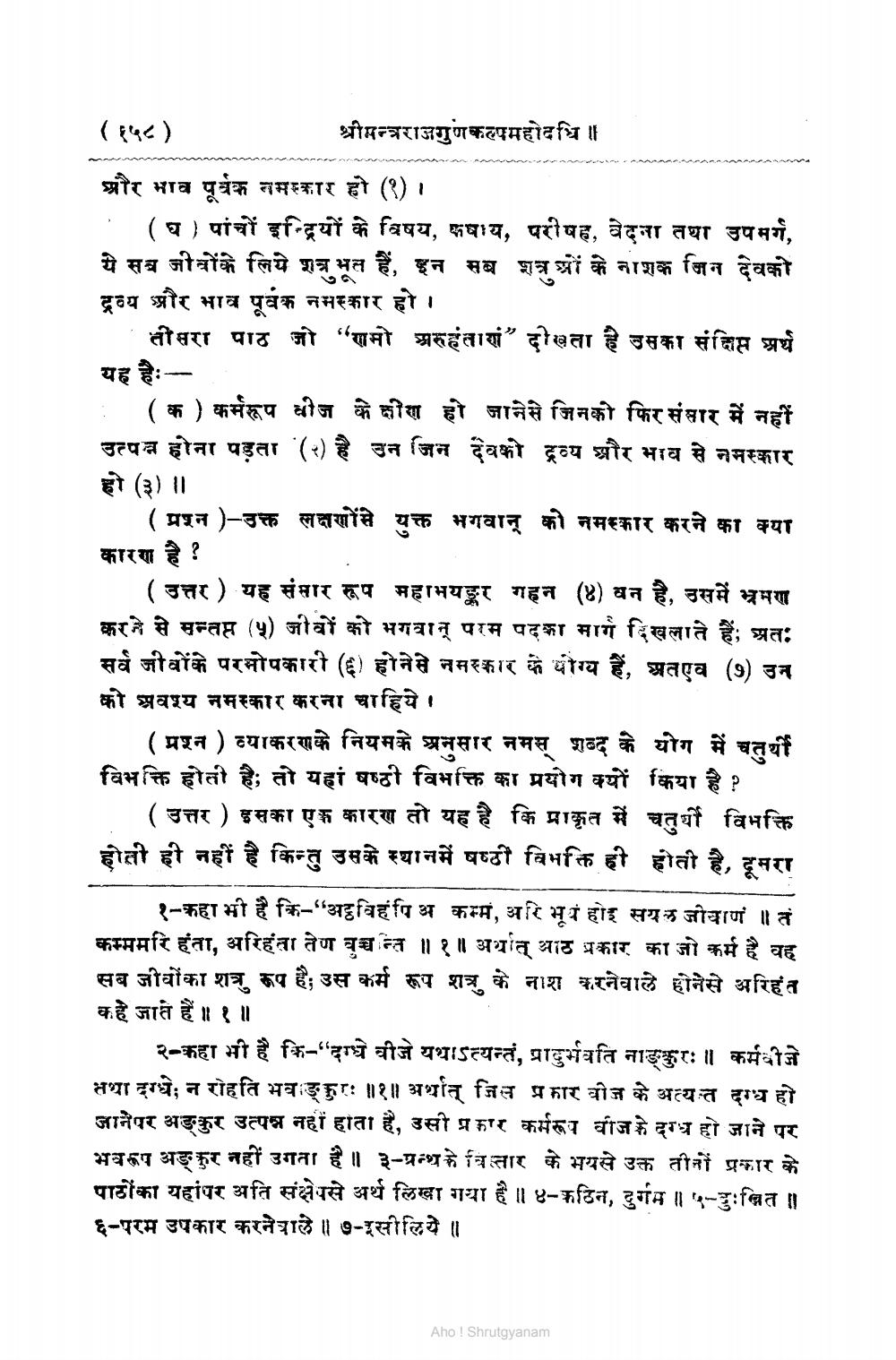________________
( १५८ )
और भाव पूर्वक नमस्कार हो (१) ।
(घ) पांचों इन्द्रियों के विषय, कषाय, परोषह, वेदना तथा उपमर्ग, शत्रुओं के नाशक जिन देवको
ये सब जीवोंके लिये शत्रु भूत हैं, इन सब द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार हो ।
तीसरा पाठ जो " णमो अरुहंताणं" दीखता है उसका संक्षिप्त अर्थ यह है :
( क ) कर्मरूप वीज के क्षीण हो जाने से जिनको फिर संसार में नहीं उत्पन्न होना पड़ता (२) है उन जिन देवको द्रव्य और भाव से नमस्कार हो (३) ।
( प्रश्न ) - उक्त लक्षणोंसे युक्त भगवान् को नमस्कार करने का क्या कारण है ?
श्रीमन्त्रराजगुण कल्पमहोदधि ॥
--
( उत्तर ) यह संसार रूप महाभयङ्कर गहन ( ४ ) वन है, उसमें भ्रमण करने से सन्तप्त (५) जीवों को भगवान् परम पदका मार्ग दिखलाते हैं; अतः सर्व जीवोंके परोपकारी (६) होनेसे नमस्कार के योग्य हैं, अतएव (9) उन को अवश्य नमस्कार करना चाहिये ।
( प्रश्न ) व्याकरण के नियमके अनुसार नमस् शब्द के विभक्ति होती है; तो यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्यों ( उत्तर ) इसका एक कारण तो यह है कि प्राकृत में होती ही नहीं है किन्तु उसके स्थान में षष्ठी विभक्ति ही
योग में चतुर्थी किया है ?
चतुर्थी विभक्ति होती है, दूसरा
१- कहा भी है कि - " अट्ठविहंपि अ कम्म, अरि भूयं होइ सयल जीवाणं ॥ तं कम्ममरिहंता, अरिहंता तेण वुञ्चन्ति ॥ १ ॥ अर्थात् आठ प्रकार का जो कर्म है वह सब जीवों का शत्रु रूप है; उस कर्म रूप शत्रु के नाश करनेवाले होनेसे अरिहंत कहे जाते हैं ॥ १ ॥
२- कहा भी है कि- "दग्धे वीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ॥ कर्मवीजे तथा दग्धे; न रोहति भवःङ्कुरः ॥ १ ॥ अर्थात् जिस प्रकार वीज के अत्यन्त दग्ध हो जानेपर अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार कर्मरूप वीज के दग्ध हो जाने पर भवरूप अङ्कुर नहीं उगता है ॥ ३-प्रन्थ के विस्तार के भयले उक्त तीनों प्रकार के पाठोंका यहां पर अति संक्षेपसे अर्थ लिखा गया है ॥ ४-कठिन, दुर्गम ॥ ५- दुःखित || ६- परम उपकार करनेवाले ॥ ७- इसीलिये ॥
Aho! Shrutgyanam