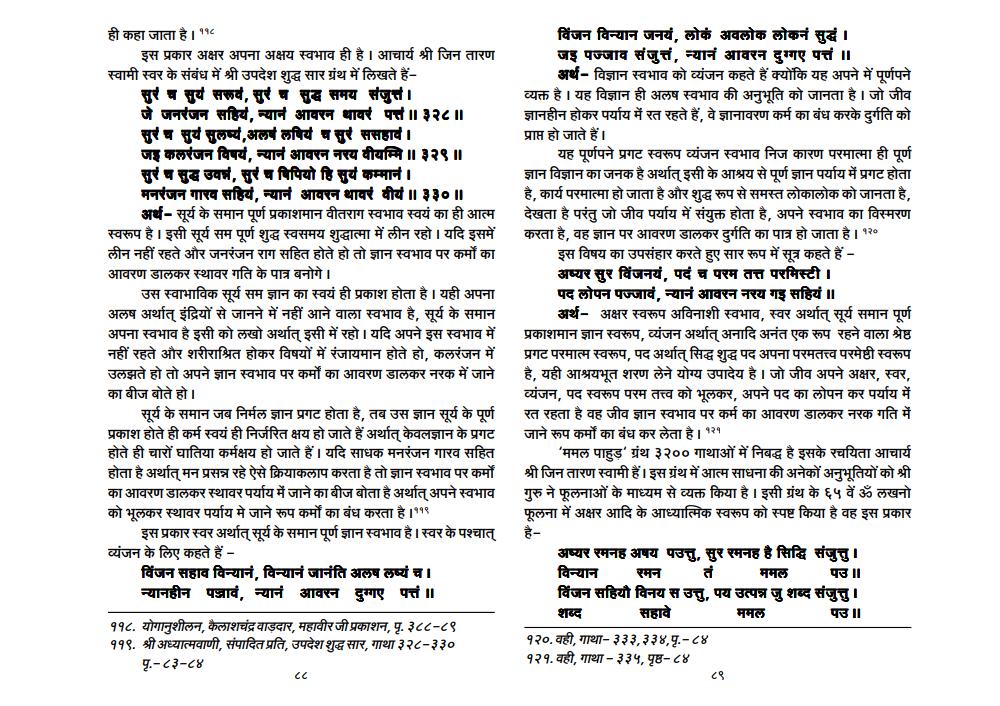________________
ही कहा जाता है। ११८
इस प्रकार अक्षर अपना अक्षय स्वभाव ही है। आचार्य श्री जिन तारण स्वामी स्वर के संबंध में श्री उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में लिखते हैं
सुरंब सुर्य सलव, सुरं च सुख समय संजुत्त। जे जनरंजन सहिय, न्यानं आवरन थावर पत्तं ॥ ३२८॥ सुरंच सुर्य सुलय,अलब लषियं च सुरं ससहावं । जइ कलरंजन विषयं, न्यानं आवरन नस्य वीयम्मि ॥ ३२९॥ सुरंच सुख उवान, सुरंप पिपियो हि सुर्य कम्मान । मनरंजन गारव सहियं, न्यानं आवरन थावरं वीयं ॥३३०॥
अर्थ- सूर्य के समान पूर्ण प्रकाशमान वीतराग स्वभाव स्वयं का ही आत्म स्वरूप है। इसी सूर्य सम पूर्ण शुद्ध स्वसमय शुद्धात्मा में लीन रहो । यदि इसमें लीन नहीं रहते और जनरंजन राग सहित होते हो तो ज्ञान स्वभाव पर कर्मों का आवरण डालकर स्थावर गति के पात्र बनोगे।
उस स्वाभाविक सूर्य सम ज्ञान का स्वयं ही प्रकाश होता है। यही अपना अलष अर्थात् इंद्रियों से जानने में नहीं आने वाला स्वभाव है, सूर्य के समान अपना स्वभाव है इसी को लखो अर्थात् इसी में रहो। यदि अपने इस स्वभाव में नहीं रहते और शरीराश्रित होकर विषयों में रंजायमान होते हो, कलरंजन में उलझते हो तो अपने ज्ञान स्वभाव पर कर्मों का आवरण डालकर नरक में जाने का बीज बोते हो।
सूर्य के समान जब निर्मल ज्ञान प्रगट होता है, तब उस ज्ञान सूर्य के पूर्ण प्रकाश होते ही कर्म स्वयं ही निर्जरित क्षय हो जाते हैं अर्थात् केवलज्ञान के प्रगट होते ही चारों घातिया कर्मक्षय हो जाते हैं। यदि साधक मनरंजन गारव सहित होता है अर्थात् मन प्रसन्न रहे ऐसे क्रियाकलाप करता है तो ज्ञान स्वभाव पर कर्मों का आवरण डालकर स्थावर पर्याय में जाने का बीज बोता है अर्थात् अपने स्वभाव को भूलकर स्थावर पर्याय मे जाने रूप कर्मों का बंध करता है ।११९
इस प्रकार स्वर अर्थात् सूर्य के समान पूर्ण ज्ञान स्वभाव है। स्वर के पश्चात् । व्यंजन के लिए कहते हैं
विजन सहाव विन्यानं, विन्यानं जानंति अलष लष्यं च । न्यानहीन पजावं, न्यानं आवरन दुग्गए पत्तं ॥
विजन विन्यान जनयं,लोकं अवलोक लोकनं सुद्धं । जइ पज्जाव संजुत्तं, न्यानं आवरन दुग्गए पत्तं ॥
अर्थ-विज्ञान स्वभाव को व्यंजन कहते हैं क्योंकि यह अपने में पूर्णपने व्यक्त है। यह विज्ञान ही अलष स्वभाव की अनुभूति को जानता है। जो जीव ज्ञानहीन होकर पर्याय में रत रहते हैं, वे ज्ञानावरण कर्म का बंध करके दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं।
यह पूर्णपने प्रगट स्वरूप व्यंजन स्वभाव निज कारण परमात्मा ही पूर्ण ज्ञान विज्ञान का जनक है अर्थात् इसी के आश्रय से पूर्ण ज्ञान पर्याय में प्रगट होता है, कार्य परमात्मा हो जाता है और शुद्ध रूप से समस्त लोकालोक को जानता है, देखता है परंतु जो जीव पर्याय में संयुक्त होता है, अपने स्वभाव का विस्मरण करता है, वह ज्ञान पर आवरण डालकर दुर्गति का पात्र हो जाता है । १२०
इस विषय का उपसंहार करते हुए सार रूप में सूत्र कहते हैंअभ्यर सुर विंजनयं, पदं च परम तत्त परमिस्टी। पद लोपन पज्जावं,न्यानं आवरन नरय गइ सहियं ॥
अर्थ- अक्षर स्वरूप अविनाशी स्वभाव, स्वर अर्थात् सूर्य समान पूर्ण प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप, व्यंजन अर्थात् अनादि अनंत एक रूप रहने वाला श्रेष्ठ प्रगट परमात्म स्वरूप, पद अर्थात् सिद्ध शुद्ध पद अपना परमतत्त्व परमेष्ठी स्वरूप है, यही आश्रयभूत शरण लेने योग्य उपादेय है। जो जीव अपने अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद स्वरूप परम तत्त्व को भूलकर, अपने पद का लोपन कर पर्याय में रत रहता है वह जीव ज्ञान स्वभाव पर कर्म का आवरण डालकर नरक गति में जाने रूप कर्मों का बंध कर लेता है। १२१
'ममल पाहुड' ग्रंथ ३२०० गाथाओं में निबद्ध है इसके रचयिता आचार्य श्री जिन तारण स्वामी हैं। इस ग्रंथ में आत्म साधना की अनेकों अनुभूतियों को श्री गुरु ने फूलनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। इसी ग्रंथ के ६५ वें ॐ लखनो फूलना में अक्षर आदि के आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट किया है वह इस प्रकार
अव्यर रमनह अषय पउत्तु, सुर रमनह है सिद्धि संजुत्तु । विन्यान रमन तं ममल पउ॥ विजन सहियौ विनय स उत्तु, पय उत्पन्न जु शब्द संजुत्तु।
शब्द सहावे ममल पउ॥ १२०. वही, गाथा-३३३,३३४,पृ.-८४ १२१.वही,गाथा-३३५, पृष्ठ-८४
११८. योगानुशीलन, कैलाशचंद्र वाडदार, महावीरजी प्रकाशन, पृ.३८८-८९ ११९. श्री अध्यात्मवाणी, संपादित प्रति, उपदेश शुद्ध सार, गाथा ३२८-३३०
पृ.-८३-८४
८८