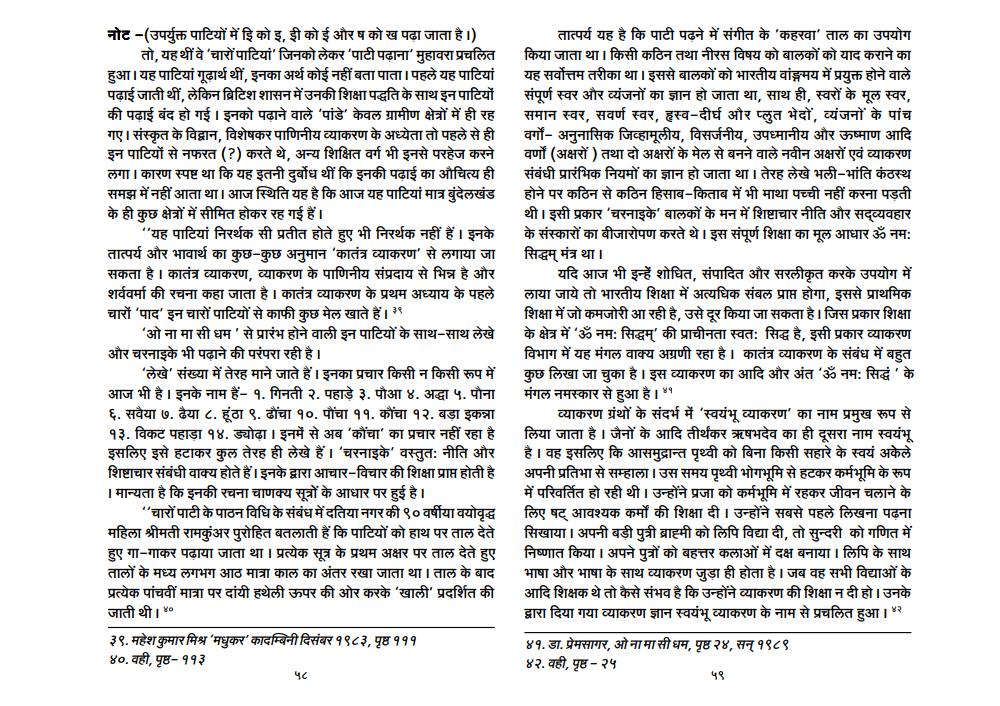________________
नोट - (उपर्युक्त पाटियों में इि को इ, ईी को ई और ष को ख पढ़ा जाता है ।)
तो, यह थीं वे 'चारों पाटियां' जिनको लेकर 'पाटी पढ़ाना' मुहावरा प्रचलित हुआ। यह पाटियां गूढार्थ थीं, इनका अर्थ कोई नहीं बता पाता। पहले यह पाटियां पढ़ाई जाती थीं, लेकिन ब्रिटिश शासन में उनकी शिक्षा पद्धति के साथ इन पाटियों की पढ़ाई बंद हो गई। इनको पढ़ाने वाले 'पांडे' केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रह गए। संस्कृत के विद्वान, विशेषकर पाणिनीय व्याकरण के अध्येता तो पहले से ही इन पाटियों से नफरत (?) करते थे, अन्य शिक्षित वर्ग भी इनसे परहेज करने लगा। कारण स्पष्ट था कि यह इतनी दुर्बोध थीं कि इनकी पढ़ाई का औचित्य ही समझ में नहीं आता था। आज स्थिति यह है कि आज यह पाटियां मात्र बुंदेलखंड के ही कुछ क्षेत्रों में सीमित होकर रह गई हैं।
"यह पाटियां निरर्थक सी प्रतीत होते हुए भी निरर्थक नहीं हैं। इनके तात्पर्य और भावार्थ का कुछ-कुछ अनुमान 'कातंत्र व्याकरण' से लगाया जा सकता है। कातंत्र व्याकरण, व्याकरण के पाणिनीय संप्रदाय से भिन्न है और शर्ववर्मा की रचना कहा जाता है। कातंत्र व्याकरण के प्रथम अध्याय के पहले चारों 'पाद' इन चारों पाटियों से काफी कुछ मेल खाते हैं।
३९
'ओ ना मा सी धम' से प्रारंभ होने वाली इन पाटियों के साथ-साथ लेखे और चरनाइके भी पढ़ाने की परंपरा रही है।
'लेखे' संख्या में तेरह माने जाते हैं। इनका प्रचार किसी न किसी रूप में आज भी है। इनके नाम हैं- १. गिनती २. पहाड़े ३. पौआ ४. अद्धा ५ पौना ६. सवैया ७. ढैया ८. हूंठा ९. ढौंचा १०. पौंचा ११. कौंचा १२. बड़ा इकन्ना १३. विकट पहाड़ा १४. ड्योढ़ा । इनमें से अब 'कौंचा' का प्रचार नहीं रहा है इसलिए इसे हटाकर कुल तेरह ही लेखे हैं। 'चरनाइके' वस्तुतः नीति और शिष्टाचार संबंधी वाक्य होते हैं। इनके द्वारा आचार-विचार की शिक्षा प्राप्त होती है । मान्यता है कि इनकी रचना चाणक्य सूत्रों के आधार पर हुई है।
"चारों पाटी के पाठन विधि के संबंध में दतिया नगर की ९० वर्षीया वयोवृद्ध महिला श्रीमती रामकुंअर पुरोहित बतलाती हैं कि पाटियों को हाथ पर ताल देते हुए गा-गाकर पढ़ाया जाता था। प्रत्येक सूत्र के प्रथम अक्षर पर ताल देते हुए तालों के मध्य लगभग आठ मात्रा काल का अंतर रखा जाता था। ताल के बाद प्रत्येक पांचवीं मात्रा पर दांयी हथेली ऊपर की ओर करके 'खाली' प्रदर्शित की जाती थी। ४०
३९. महेश कुमार मिश्र 'मधुकर' कादम्बिनी दिसंबर १९८३, पृष्ठ १११ ४०. वही, पृष्ठ- ११३
५८
तात्पर्य यह है कि पाटी पढ़ने में संगीत के 'कहरवा' ताल का उपयोग किया जाता था। किसी कठिन तथा नीरस विषय को बालकों को याद कराने का यह सर्वोत्तम तरीका था। इससे बालकों को भारतीय वांङ्गमय में प्रयुक्त होने वाले संपूर्ण स्वर और व्यंजनों का ज्ञान हो जाता था, साथ ही, स्वरों के मूल स्वर, समान स्वर, सवर्ण स्वर, हस्व-दीर्घ और प्लुत भेदों, व्यंजनों के पांच वर्गों - अनुनासिक जिव्हामूलीय, विसर्जनीय, उपध्मानीय और ऊष्माण आदि वर्णों (अक्षरों) तथा दो अक्षरों के मेल से बनने वाले नवीन अक्षरों एवं व्याकरण संबंधी प्रारंभिक नियमों का ज्ञान हो जाता था। तेरह लेखे भली-भांति कंठस्थ होने पर कठिन से कठिन हिसाब-किताब में भी माथा पच्ची नहीं करना पड़ती थी। इसी प्रकार 'चरनाइके' बालकों के मन में शिष्टाचार नीति और सद्व्यवहार के संस्कारों का बीजारोपण करते थे। इस संपूर्ण शिक्षा का मूल आधार ॐ नमः सिद्धम् मंत्र था।
यदि आज भी इन्हें शोधित, संपादित और सरलीकृत करके उपयोग में लाया जाये तो भारतीय शिक्षा में अत्यधिक संबल प्राप्त होगा, इससे प्राथमिक • शिक्षा में जो कमजोरी आ रही है, उसे दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में 'ॐ नमः सिद्धम्' की प्राचीनता स्वतः सिद्ध है, इसी प्रकार व्याकरण विभाग में यह मंगल वाक्य अग्रणी रहा है। कातंत्र व्याकरण के संबंध में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस व्याकरण का आदि और अंत 'ॐ नमः सिद्धं ' के मंगल नमस्कार से हुआ है। ४१
व्याकरण ग्रंथों के संदर्भ में 'स्वयंभू व्याकरण' का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जैनों के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का ही दूसरा नाम स्वयंभू है। वह इसलिए कि आसमुद्रान्त पृथ्वी को बिना किसी सहारे के स्वयं अकेले अपनी प्रतिभा से सम्हाला। उस समय पृथ्वी भोगभूमि से हटकर कर्मभूमि के रूप में परिवर्तित हो रही थी। उन्होंने प्रजा को कर्मभूमि में रहकर जीवन चलाने के लिए षट् आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। उन्होंने सबसे पहले लिखना पढ़ना सिखाया। अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी को लिपि विद्या दी, तो सुन्दरी को गणित में निष्णात किया । अपने पुत्रों को बहत्तर कलाओं में दक्ष बनाया। लिपि के साथ भाषा और भाषा के साथ व्याकरण जुड़ा ही होता है। जब वह सभी विद्याओं के आदि शिक्षक थे तो कैसे संभव है कि उन्होंने व्याकरण की शिक्षा न दी हो। उनके द्वारा दिया गया व्याकरण ज्ञान स्वयंभू व्याकरण के नाम से प्रचलित हुआ ।
४२
४१. डा. प्रेमसागर, ओ ना मा सी धम, पृष्ठ २४, सन् १९८९ ४२. वही, पृष्ठ २५
-
५९