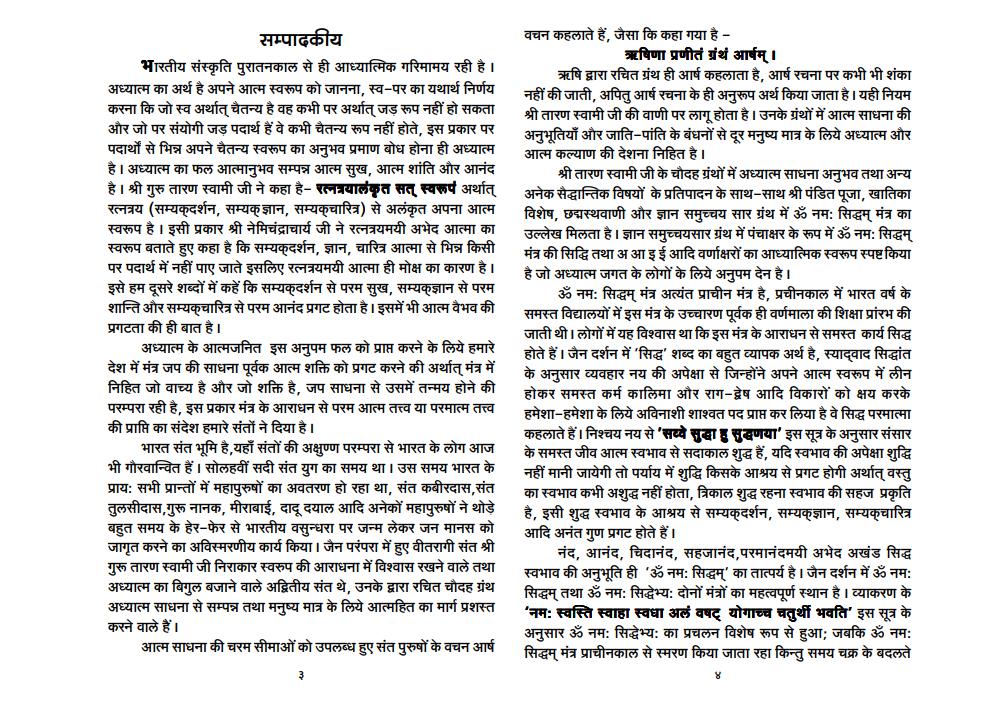________________
सम्पादकीय भारतीय संस्कृति पुरातनकाल से ही आध्यात्मिक गरिमामय रही है। अध्यात्म का अर्थ है अपने आत्म स्वरूप को जानना, स्व-पर का यथार्थ निर्णय करना कि जो स्व अर्थात् चैतन्य है वह कभी पर अर्थात् जड़ रूप नहीं हो सकता और जो पर संयोगी जड़ पदार्थ हैं वे कभी चैतन्य रूप नहीं होते, इस प्रकार पर पदार्थों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव प्रमाण बोध होना ही अध्यात्म है। अध्यात्म का फल आत्मानुभव सम्पन्न आत्म सुख, आत्म शांति और आनंद है। श्री गुरु तारण स्वामी जी ने कहा है- रत्नत्रयालंकृत सत् स्वरूप अर्थात् रत्नत्रय (सम्यक्दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक्चारित्र) से अलंकृत अपना आत्म स्वरूप है। इसी प्रकार श्री नेमिचंद्राचार्य जी ने रत्नत्रयमयी अभेद आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा है कि सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा से भिन्न किसी पर पदार्थ में नहीं पाए जाते इसलिए रत्नत्रयमयी आत्मा ही मोक्ष का कारण है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें कि सम्यक्दर्शन से परम सुख, सम्यकज्ञान से परम शान्ति और सम्यक्चारित्र से परम आनंद प्रगट होता है। इसमें भी आत्म वैभव की प्रगटता की ही बात है।
अध्यात्म के आत्मजनित इस अनुपम फल को प्राप्त करने के लिये हमारे देश में मंत्र जप की साधना पूर्वक आत्म शक्ति को प्रगट करने की अर्थात् मंत्र में निहित जो वाच्य है और जो शक्ति है, जप साधना से उसमें तन्मय होने की परम्परा रही है, इस प्रकार मंत्र के आराधन से परम आत्म तत्त्व या परमात्म तत्त्व की प्राप्ति का संदेश हमारे संतों ने दिया है।
भारत संत भूमि है,यहाँ संतों की अक्षुण्ण परम्परा से भारत के लोग आज भी गौरवान्वित हैं। सोलहवीं सदी संत युग का समय था। उस समय भारत के प्राय: सभी प्रान्तों में महापुरुषों का अवतरण हो रहा था, संत कबीरदास,संत तुलसीदास,गुरू नानक, मीराबाई, दादू दयाल आदि अनेकों महापुरुषों ने थोड़े बहुत समय के हेर-फेर से भारतीय वसुन्धरा पर जन्म लेकर जन मानस को जागृत करने का अविस्मरणीय कार्य किया। जैन परंपरा में हुए वीतरागी संत श्री गुरू तारण स्वामी जी निराकार स्वरुप की आराधना में विश्वास रखने वाले तथा अध्यात्म का बिगुल बजाने वाले अद्वितीय संत थे, उनके द्वारा रचित चौदह ग्रंथ अध्यात्म साधना से सम्पन्न तथा मनुष्य मात्र के लिये आत्महित का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं।
आत्म साधना का चरम सामाआ का उपलब्ध हुए सत पुरुषा कवचन आष
वचन कहलाते हैं, जैसा कि कहा गया है
ऋषिणा प्रणीतं ग्रंथं आर्षम् । ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ ही आर्ष कहलाता है, आर्ष रचना पर कभी भी शंका नहीं की जाती, अपितु आर्ष रचना के ही अनुरूप अर्थ किया जाता है। यही नियम श्री तारण स्वामी जी की वाणी पर लागू होता है। उनके ग्रंथों में आत्म साधना की अनुभूतियाँ और जाति-पांति के बंधनों से दूर मनुष्य मात्र के लिये अध्यात्म और आत्म कल्याण की देशना निहित है।
श्री तारण स्वामीजी के चौदह ग्रंथों में अध्यात्म साधना अनुभव तथा अन्य अनेक सैद्धान्तिक विषयों के प्रतिपादन के साथ-साथ श्री पंडित पूजा, खातिका विशेष, छदास्थवाणी और ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में ॐ नम: सिद्धम् मंत्र का उल्लेख मिलता है। ज्ञान समुच्चयसार ग्रंथ में पंचाक्षर के रूप में ॐ नम: सिद्धम् मंत्र की सिद्धि तथा अ आ इ ई आदि वर्णाक्षरों का आध्यात्मिक स्वरूप स्पष्ट किया है जो अध्यात्म जगत के लोगों के लिये अनुपम देन है।
ॐ नमः सिद्धम् मंत्र अत्यंत प्राचीन मंत्र है, प्रचीनकाल में भारत वर्ष के समस्त विद्यालयों में इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक ही वर्णमाला की शिक्षा प्रांरभ की जाती थी। लोगों में यह विश्वास था कि इस मंत्र के आराधन से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जैन दर्शन में 'सिद्ध' शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है, स्याद्वाद सिद्धांत के अनुसार व्यवहार नय की अपेक्षा से जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर समस्त कर्म कालिमा और राग-द्वेष आदि विकारों को क्षय करके हमेशा-हमेशा के लिये अविनाशी शाश्वत पद प्राप्त कर लिया है वे सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। निश्चय नय से 'सय्ये सुद्धा सुबणया' इस सूत्र के अनुसार संसार के समस्त जीव आत्म स्वभाव से सदाकाल शुद्ध हैं, यदि स्वभाव की अपेक्षा शुद्धि नहीं मानी जायेगी तो पर्याय में शुद्धि किसके आश्रय से प्रगट होगी अर्थात् वस्तु का स्वभाव कभी अशुद्ध नहीं होता, त्रिकाल शुद्ध रहना स्वभाव की सहज प्रकृति है, इसी शुद्ध स्वभाव के आश्रय से सम्यक्दर्शन, सम्यज्ञान, सम्यक्चारित्र आदि अनंत गुण प्रगट होते हैं।
नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद,परमानंदमयी अभेद अखंड सिद्ध स्वभाव की अनुभूति ही 'ॐ नमः सिद्धम्' का तात्पर्य है। जैन दर्शन में ॐ नमः सिद्धम् तथा ॐ नमः सिद्धेभ्य: दोनों मंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण के 'नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषट् योगाच्च चतुर्थी भवति' इस सूत्र के अनुसार ॐ नमः सिद्धेभ्य: का प्रचलन विशेष रूप से हुआ; जबकि ॐ नमः सिद्धम् मंत्र प्राचीनकाल से स्मरण किया जाता रहा किन्तु समय चक्र के बदलते