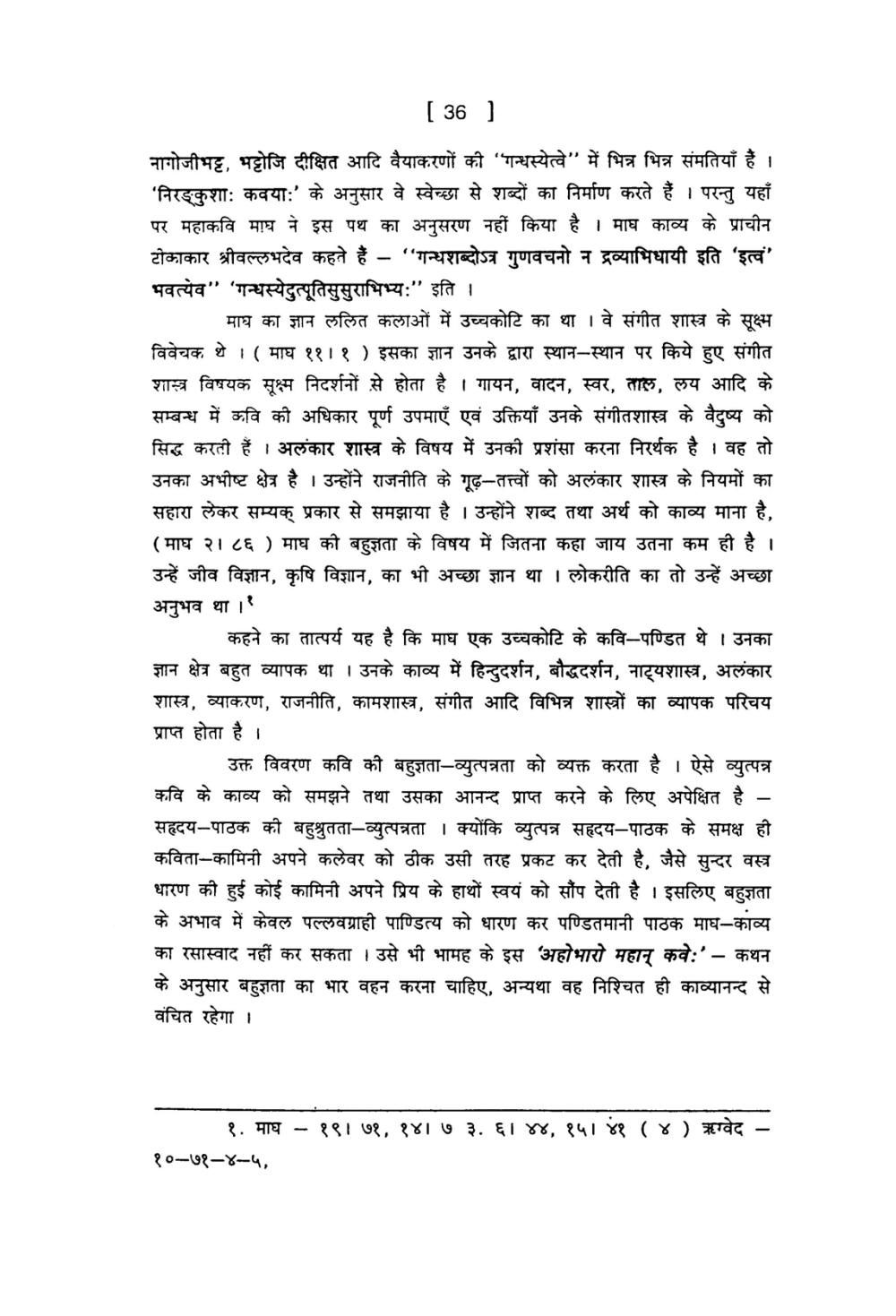________________
[ 36 ] नागोजीभट्ट, भट्टोजि दीक्षित आदि वैयाकरणों की “गन्धस्यत्वे' में भित्र भिन्न संमतियाँ है । 'निरङ्कुशाः कवयाः' के अनुसार वे स्वेच्छा से शब्दों का निर्माण करते हैं । परन्तु यहाँ पर महाकवि माघ ने इस पथ का अनुसरण नहीं किया है । माघ काव्य के प्राचीन टोकाकार श्रीवल्लभदेव कहते हैं - "गन्धशब्दोऽत्र गुणवचनो न द्रव्याभिधायी इति 'इत्वं' भवत्येव" 'गन्धस्येदुत्पूतिसुसुराभिभ्यः' इति ।
___ माघ का ज्ञान ललित कलाओं में उच्चकोटि का था । वे संगीत शास्त्र के सूक्ष्म विवेचक थे । ( माघ ११ । १ ) इसका ज्ञान उनके द्वारा स्थान-स्थान पर किये हुए संगीत शास्त्र विषयक सूक्ष्म निदर्शनों से होता है । गायन, वादन, स्वर, ताल, लय आदि के सम्बन्ध में ऊवि की अधिकार पूर्ण उपमाएँ एवं उक्तियाँ उनके संगीतशास्त्र के वैदुष्य को सिद्ध करती हैं । अलंकार शास्त्र के विषय में उनकी प्रशंसा करना निरर्थक है । वह तो उनका अभीष्ट क्षेत्र है । उन्होंने राजनीति के गढ-तत्त्वों को अलंकार शास्त्र के नियमों का सहारा लेकर सम्यक् प्रकार से समझाया है । उन्होंने शब्द तथा अर्थ को काव्य माना है, ( माघ २। ८६ ) माघ की बहुज्ञता के विषय में जितना कहा जाय उतना कम ही है । उन्हें जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, का भी अच्छा ज्ञान था । लोकरीति का तो उन्हें अच्छा अनुभव था ।'
कहने का तात्पर्य यह है कि माघ एक उच्चकोटि के कवि-पण्डित थे । उनका ज्ञान क्षेत्र बहुत व्यापक था । उनके काव्य में हिन्दुदर्शन, बौद्धदर्शन, नाट्यशास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण, राजनीति, कामशास्त्र, संगीत आदि विभिन्न शास्त्रों का व्यापक परिचय प्राप्त होता है ।
उक्त विवरण कवि की बहुज्ञता व्युत्पत्रता को व्यक्त करता है । ऐसे व्युत्पन्न कवि के काव्य को समझने तथा उसका आनन्द प्राप्त करने के लिए अपेक्षित है - सहृदय-पाठक की बहुश्रुतता-व्युत्पन्नता । क्योंकि व्युत्पन्न सहदय-पाठक के समक्ष ही कविता-कामिनी अपने कलेवर को ठीक उसी तरह प्रकट कर देती है, जैसे सुन्दर वस्त्र धारण की हुई कोई कामिनी अपने प्रिय के हाथों स्वयं को सौंप देती है । इसलिए बहुज्ञता के अभाव में केवल पल्लवग्राही पाण्डित्य को धारण कर पण्डितमानी पाठक माघ-काव्य का रसास्वाद नहीं कर सकता । उसे भी भामह के इस 'अहोभारो महान् कवेः' - कथन के अनुसार बहुज्ञता का भार वहन करना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित ही काव्यानन्द से वंचित रहेगा।
१. माघ - १९। ७१, १४। ७ ३.६। ४४, १५। ४१ ( ४ ) ऋग्वेद - १०-७१-४-५,