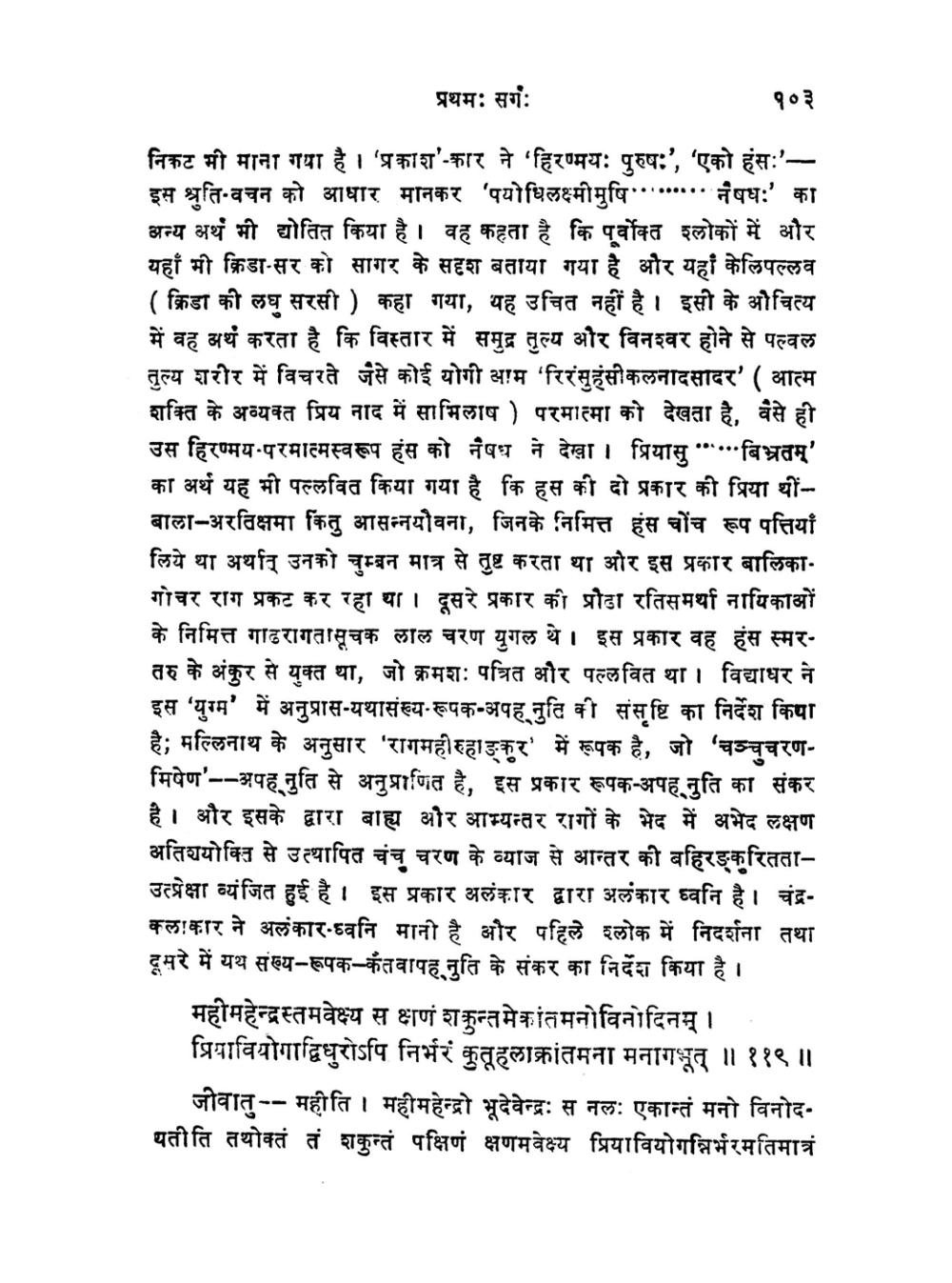________________
प्रथमः सर्गः
१०३
निकट भी माना गया है । 'प्रकाश' कार ने 'हिरण्मयः पुरुषः', 'एको हंसः 'इस श्रुति वचन को आधार मानकर 'पयोधिलक्ष्मीमुषि..... नैषधः' का अन्य अर्थ भी द्योतित किया है। वह कहता है कि पूर्वोक्त श्लोकों में और यहाँ भी क्रिडा सर को सागर के सदृश बताया गया है और यहाँ केलिपल्लव ( क्रिडा की लघु सरसी ) कहा गया, यह उचित नहीं है । इसी के औचित्य में वह अर्थ करता है कि विस्तार में समुद्र तुल्य और विनश्वर होने से पल्वल तुल्य शरीर में विचरते जैसे कोई योगी आम 'रिरंसुहंसी कलनादसादर' ( आत्म शक्ति के अव्यक्त प्रिय नाद में साभिलाष ) परमात्मा को देखता है, वैसे ही उस हिरण्मय परमात्मस्वरूप हंस को नैषध ने देखा । प्रियासु ..... बिभ्रतम्' का अर्थ यह भी पल्लवित किया गया है कि हस की दो प्रकार की प्रिया थींबाला- अरतिक्षमा किंतु आसन्नयोवना, जिनके निमित्त हंस चोंच रूप पत्तियाँ लिये था अर्थात् उनको चुम्बन मात्र से तुष्ट करता था और इस प्रकार बालिकागोचर राग प्रकट कर रहा था। दूसरे प्रकार की प्रौढा रतिसमर्था नायिकाओं के निमित्त गाढरागत सूचक लाल चरण युगल थे । इस प्रकार वह हंस स्मरतरु के अंकुर से युक्त था, जो क्रमशः पत्रित और पल्लवित था । विद्याधर ने इस ‘युग्म' में अनुप्रास-यथासंख्य - रूपक - अपहनुति की संसृष्टि का निर्देश किया है; मल्लिनाथ के अनुसार 'रागमहीरुहाङ्कुर' में रूपक है, जो 'चञ्चुचरणमिषेण' - - अपहनुति से अनुप्राणित है, इस प्रकार रूपक-अपहनुति का संकर है । और इसके द्वारा बाह्य और आभ्यन्तर रागों के भेद में अभेद लक्षण अतिशयोक्ति से उत्थापित चंचु चरण के व्याज से अन्तर की बहिरङ्कुरितताउत्प्रेक्षा व्यंजित हुई है । इस प्रकार अलंकार द्वारा अलंकार ध्वनि है। चंद्रकलाकार ने अलंकार-ध्वनि मानी है और पहिले श्लोक में निदर्शना तथा दूसरे में यथ संख्य- रूपक - कँतवापह, नुति के संकर का निर्देश किया है ।
महीमहेन्द्रस्तमवेक्ष्य स क्षणं शकुन्तमेकांत मनोविनोदिनम् । प्रियावियोगाद्विधुरोऽपि निर्भरं कुतूहलाक्रांतमना मनागभूत् ॥ ११९ ॥
जीवातु -- महीति । महीमहेन्द्रो भूदेवेन्द्रः स नलः एकान्तं मनो विनोदयतीति तथोक्तं तं शकुन्तं पक्षिणं क्षणमवेक्ष्य प्रियावियोगन्निर्भर मतिमात्रं