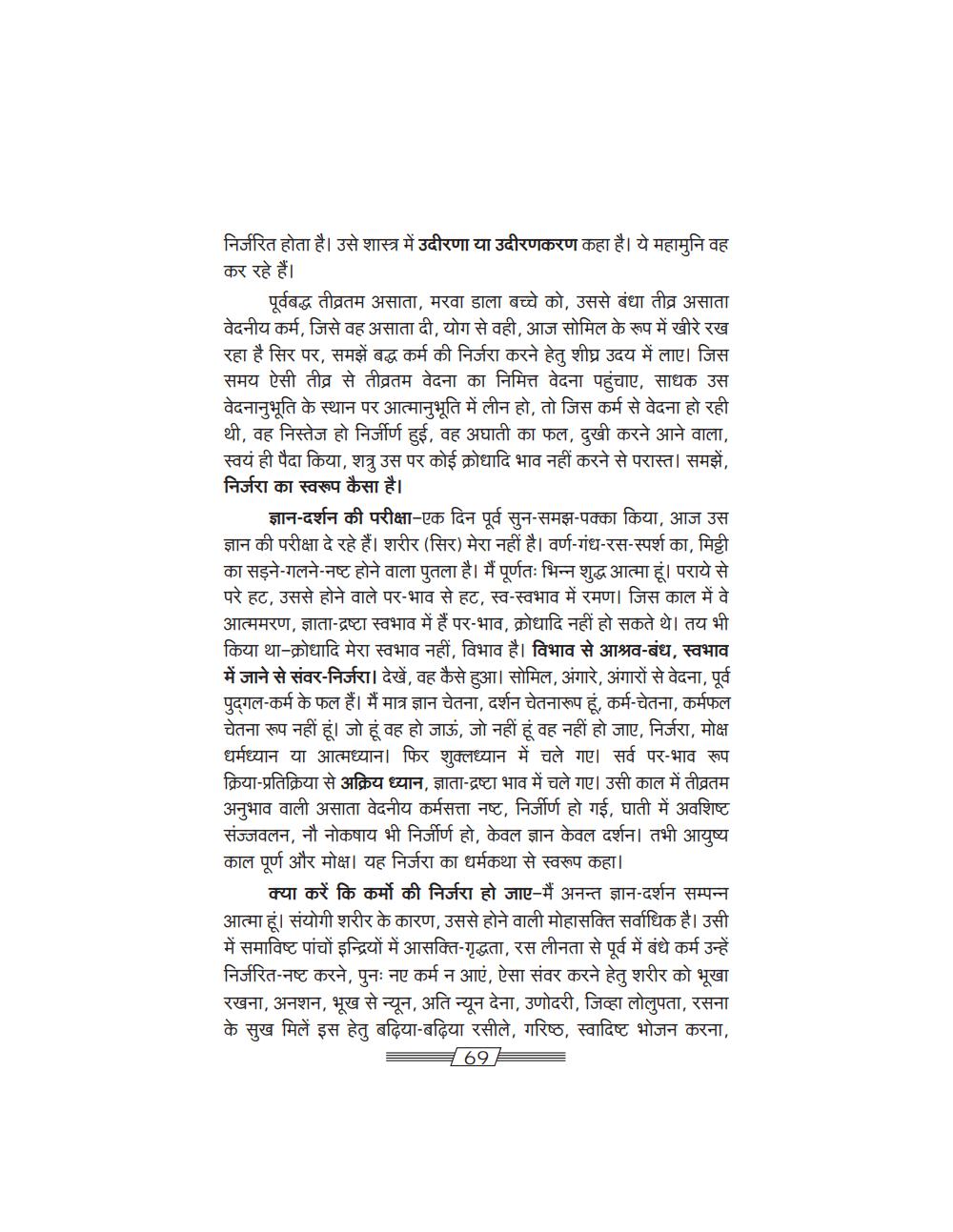________________
निर्जरित होता है। उसे शास्त्र में उदीरणा या उदीरणकरण कहा है। ये महामुनि वह कर रहे हैं।
पूर्वबद्ध तीव्रतम असाता, मरवा डाला बच्चे को, उससे बंधा तीव्र असाता वेदनीय कर्म, जिसे वह असाता दी,योग से वही, आज सोमिल के रूप में खीरे रख रहा है सिर पर, समझें बद्ध कर्म की निर्जरा करने हेतु शीघ्र उदय में लाए। जिस समय ऐसी तीव्र से तीव्रतम वेदना का निमित्त वेदना पहुंचाए, साधक उस वेदनानुभूति के स्थान पर आत्मानुभूति में लीन हो, तो जिस कर्म से वेदना हो रही थी, वह निस्तेज हो निर्जीर्ण हुई, वह अघाती का फल, दुखी करने आने वाला, स्वयं ही पैदा किया, शत्रु उस पर कोई क्रोधादि भाव नहीं करने से परास्त। समझें, निर्जरा का स्वरूप कैसा है।
ज्ञान-दर्शन की परीक्षा-एक दिन पूर्व सुन-समझ-पक्का किया, आज उस ज्ञान की परीक्षा दे रहे हैं। शरीर (सिर) मेरा नहीं है। वर्ण-गंध-रस-स्पर्श का, मिट्टी का सड़ने-गलने-नष्ट होने वाला पुतला है। मैं पूर्णतः भिन्न शुद्ध आत्मा हूं। पराये से परे हट, उससे होने वाले पर-भाव से हट, स्व-स्वभाव में रमण। जिस काल में वे आत्ममरण, ज्ञाता-द्रष्टा स्वभाव में हैं पर-भाव, क्रोधादि नहीं हो सकते थे। तय भी किया था-क्रोधादि मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। विभाव से आश्रव-बंध, स्वभाव में जाने से संवर-निर्जरा। देखें, वह कैसे हुआ। सोमिल, अंगारे, अंगारों से वेदना, पूर्व पुद्गल-कर्म के फल हैं। मैं मात्र ज्ञान चेतना, दर्शन चेतनारूप हूं, कर्म-चेतना, कर्मफल चेतना रूप नहीं हूं। जो हूं वह हो जाऊं, जो नहीं हूं वह नहीं हो जाए, निर्जरा, मोक्ष धर्मध्यान या आत्मध्यान। फिर शुक्लध्यान में चले गए। सर्व पर-भाव रूप क्रिया-प्रतिक्रिया से अक्रिय ध्यान, ज्ञाता-द्रष्टा भाव में चले गए। उसी काल में तीव्रतम अनुभाव वाली असाता वेदनीय कर्मसत्ता नष्ट, निर्जीर्ण हो गई, घाती में अवशिष्ट संज्जवलन, नौ नोकषाय भी निर्जीर्ण हो, केवल ज्ञान केवल दर्शन। तभी आयुष्य काल पूर्ण और मोक्ष। यह निर्जरा का धर्मकथा से स्वरूप कहा।
क्या करें कि कर्मो की निर्जरा हो जाए-मैं अनन्त ज्ञान-दर्शन सम्पन्न आत्मा हूं। संयोगी शरीर के कारण, उससे होने वाली मोहासक्ति सर्वाधिक है। उसी में समाविष्ट पांचों इन्द्रियों में आसक्ति-गृद्धता, रस लीनता से पूर्व में बंधे कर्म उन्हें निर्जरित-नष्ट करने, पुनः नए कर्म न आएं, ऐसा संवर करने हेतु शरीर को भूखा रखना, अनशन, भूख से न्यून, अति न्यून देना, उणोदरी, जिव्हा लोलुपता, रसना के सुख मिलें इस हेतु बढ़िया-बढ़िया रसीले, गरिष्ठ, स्वादिष्ट भोजन करना,
1694