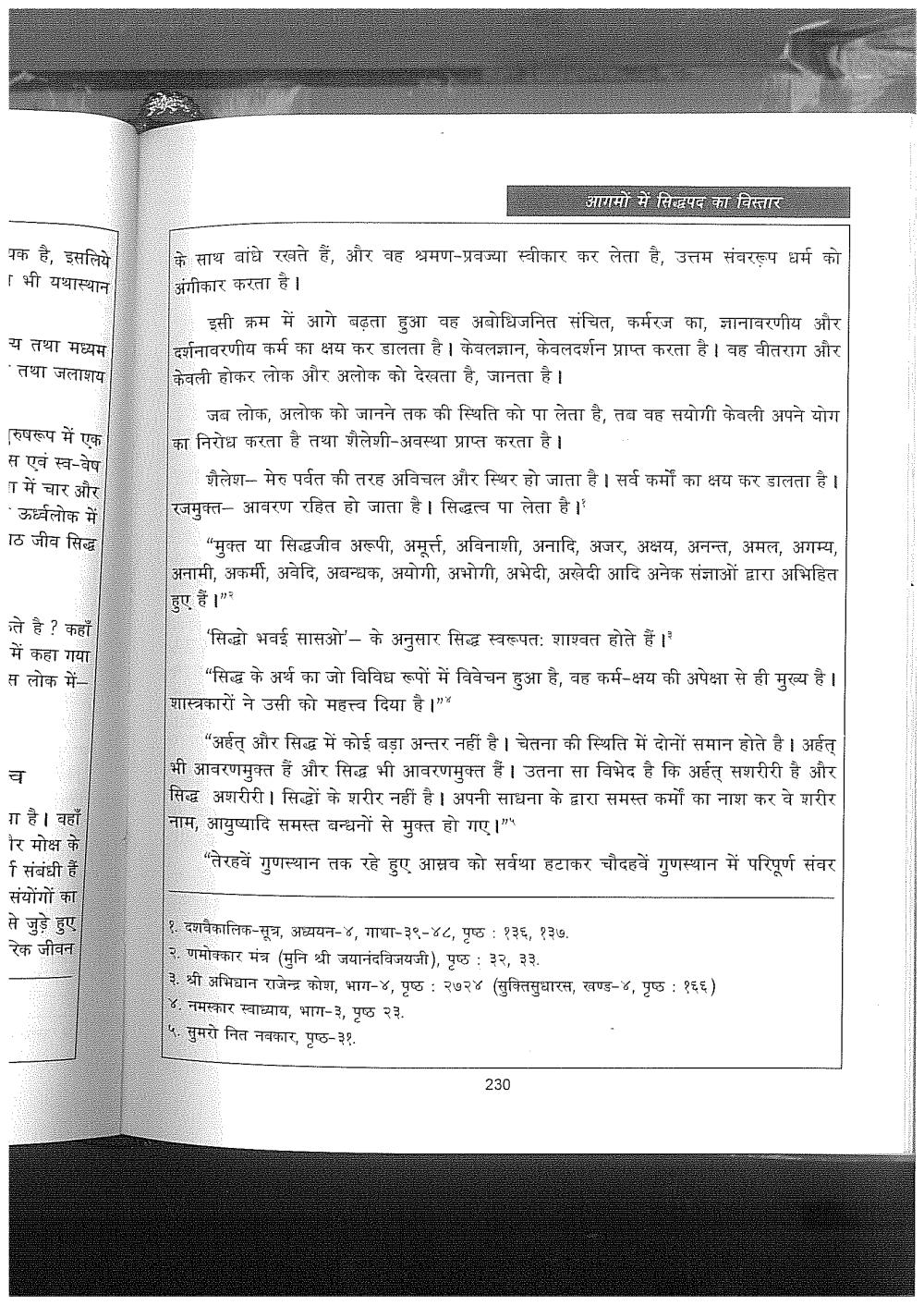________________
आगमों में सिद्धपद का विस्तार
पक है, इसलिये । भी यथास्थान
के साथ बांधे रखते हैं, और वह श्रमण-प्रवज्या स्वीकार कर लेता है, उत्तम संवररूप धर्म को अंगीकार करता है।
य तथा मध्यम तथा जलाशय
रुषरूप में एक स एवं स्व-वेष Tमें चार और ऊर्ध्वलोक में ठ जीव सिद्ध
इसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ वह अबोधिजनित संचित, कर्मरज का, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का क्षय कर डालता है। केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त करता है। वह वीतराग और केवली होकर लोक और अलोक को देखता है, जानता है।
जब लोक, अलोक को जानने तक की स्थिति को पा लेता है, तब वह सयोगी केवली अपने योग का निरोध करता है तथा शैलेशी-अवस्था प्राप्त करता है।
शैलेश- मेरु पर्वत की तरह अविचल और स्थिर हो जाता है। सर्व कर्मों का क्षय कर डालता है। रजमुक्त- आवरण रहित हो जाता है। सिद्धत्व पा लेता है।
"मुक्त या सिद्धजीव अरूपी, अमूर्त, अविनाशी, अनादि, अजर, अक्षय, अनन्त, अमल, अगम्य, अनामी, अकर्मी, अवेदि, अबन्धक, अयोगी, अभोगी, अभेदी, अखेदी आदि अनेक संज्ञाओं द्वारा अभिहित हुए हैं।"
'सिद्धो भवई सासओ'- के अनुसार सिद्ध स्वरूपत: शाश्वत होते हैं।'
"सिद्ध के अर्थ का जो विविध रूपों में विवेचन हुआ है, वह कर्म-क्षय की अपेक्षा से ही मुख्य है। शास्त्रकारों ने उसी को महत्त्व दिया है।" _ “अर्हत् और सिद्ध में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। चेतना की स्थिति में दोनों समान होते है। अर्हत् भी आवरणमुक्त हैं और सिद्ध भी आवरणमुक्त हैं। उतना सा विभेद है कि अर्हत् सशरीरी है और सिद्ध अशरीरी। सिद्धों के शरीर नहीं है। अपनी साधना के द्वारा समस्त कर्मों का नाश कर वे शरीर नाम, आयुष्यादि समस्त बन्धनों से मुक्त हो गए।"५
"तेरहवें गुणस्थान तक रहे हुए आनव को सर्वथा हटाकर चौदहवें गुणस्थान में परिपूर्ण संवर
ते है ? कहाँ में कहा गया स लोक में
च
ा है। वहाँ और मोक्ष के सिंबंधी हैं संयोंगों का से जुड़े हुए रेक जीवन
१. दशवैकालिक-सूत्र, अध्ययन-४, गाथा-३९-४८, पृष्ठ : १३६, १३७.
२. णमोक्कार मंत्र (मुनि श्री जयानंदविजयजी), पृष्ठ : ३२, ३३. | २. श्री अभिधान राजेन्द्र कोश, भाग-४, पृष्ठ : २७२४ (सुक्तिसुधारस, खण्ड-४, पृष्ठ : १६६)
४. नमस्कार स्वाध्याय, भाग-३, पृष्ठ २३. ५. सुमरो नित नवकार, पृष्ठ-३१.
230
SE