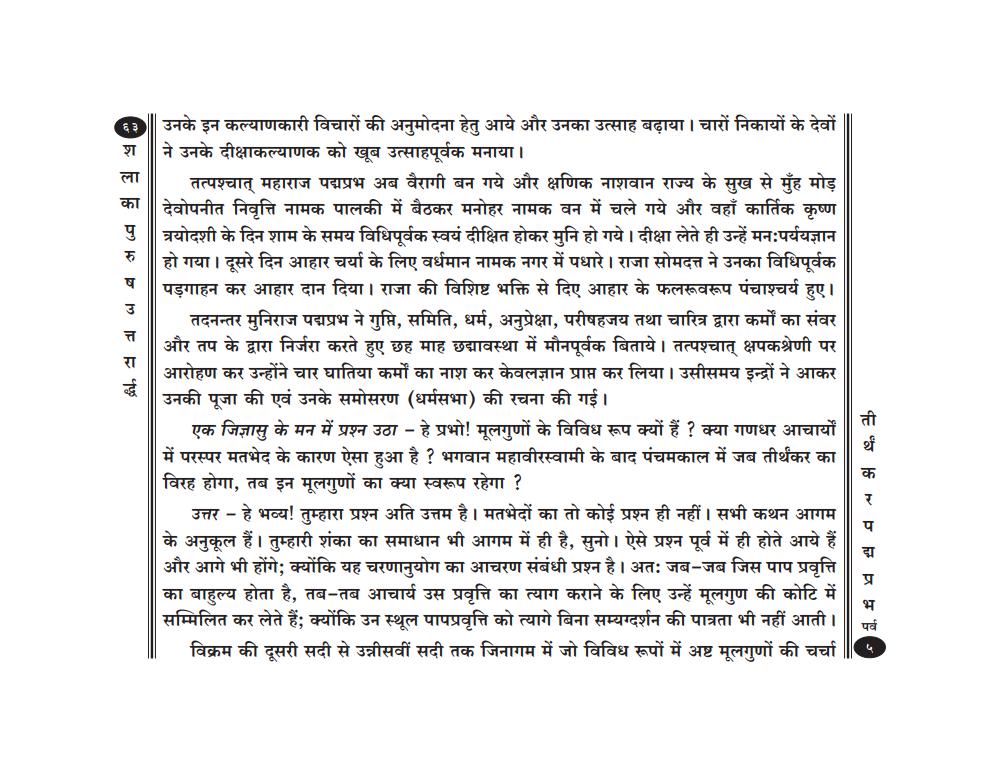________________
FEEFFFF 0
| उनके इन कल्याणकारी विचारों की अनुमोदना हेतु आये और उनका उत्साह बढ़ाया । चारों निकायों के देवों ने उनके दीक्षाकल्याणक को खूब उत्साहपूर्वक मनाया।
तत्पश्चात् महाराज पद्मप्रभ अब वैरागी बन गये और क्षणिक नाशवान राज्य के सुख से मुँह मोड़ देवोपनीत निवृत्ति नामक पालकी में बैठकर मनोहर नामक वन में चले गये और वहाँ कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन शाम के समय विधिपूर्वक स्वयं दीक्षित होकर मुनि हो गये । दीक्षा लेते ही उन्हें मन:पर्ययज्ञान हो गया। दूसरे दिन आहार चर्या के लिए वर्धमान नामक नगर में पधारे । राजा सोमदत्त ने उनका विधिपूर्वक पड़गाहन कर आहार दान दिया। राजा की विशिष्ट भक्ति से दिए आहार के फलरूवरूप पंचाश्चर्य हुए।
तदनन्तर मुनिराज पद्मप्रभ ने गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय तथा चारित्र द्वारा कर्मों का संवर और तप के द्वारा निर्जरा करते हुए छह माह छद्मावस्था में मौनपूर्वक बिताये। तत्पश्चात् क्षपकश्रेणी पर आरोहण कर उन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। उसीसमय इन्द्रों ने आकर उनकी पूजा की एवं उनके समोसरण (धर्मसभा) की रचना की गई।
एक जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठा - हे प्रभो! मूलगुणों के विविध रूप क्यों हैं ? क्या गणधर आचार्यों में परस्पर मतभेद के कारण ऐसा हुआ है ? भगवान महावीरस्वामी के बाद पंचमकाल में जब तीर्थंकर का विरह होगा, तब इन मूलगुणों का क्या स्वरूप रहेगा ?
उत्तर - हे भव्य! तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। मतभेदों का तो कोई प्रश्न ही नहीं। सभी कथन आगम के अनुकूल हैं। तुम्हारी शंका का समाधान भी आगम में ही है, सुनो। ऐसे प्रश्न पूर्व में ही होते आये हैं और आगे भी होंगे; क्योंकि यह चरणानुयोग का आचरण संबंधी प्रश्न है। अत: जब-जब जिस पाप प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है, तब-तब आचार्य उस प्रवृत्ति का त्याग कराने के लिए उन्हें मूलगुण की कोटि में सम्मिलित कर लेते हैं; क्योंकि उन स्थूल पापप्रवृत्ति को त्यागे बिना सम्यग्दर्शन की पात्रता भी नहीं आती।
विक्रम की दूसरी सदी से उन्नीसवीं सदी तक जिनागम में जो विविध रूपों में अष्ट मूलगुणों की चर्चा || ५
FFER