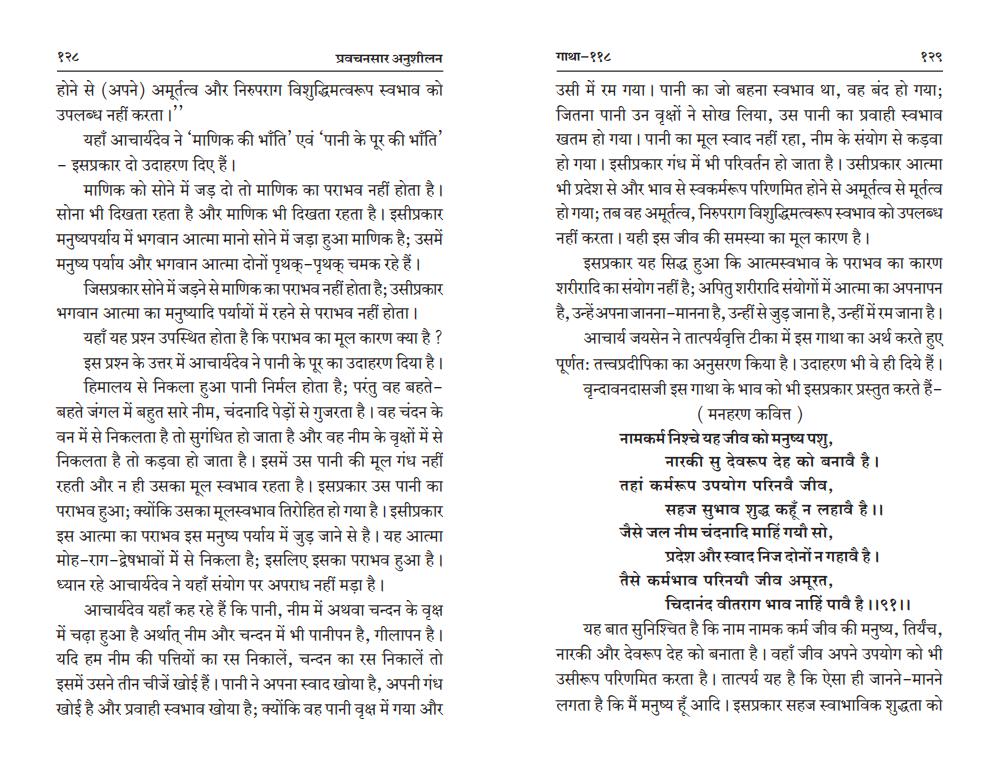________________
१२८
प्रवचनसार अनुशीलन
होने से (अपने) अमूर्तत्व और निरुपराग विशुद्धिमत्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता।"
यहाँ आचार्यदेव ने 'माणिक की भाँति' एवं 'पानी के पूर की भाँति ' - इसप्रकार दो उदाहरण दिए हैं।
माणिक को सोने में जड़ दो तो माणिक का पराभव नहीं होता है। सोना भी दिखता रहता है और माणिक भी दिखता रहता है। इसीप्रकार मनुष्यपर्याय में भगवान आत्मा मानो सोने में जड़ा हुआ माणिक है; उसमें मनुष्य पर्याय और भगवान आत्मा दोनों पृथक्-पृथक् चमक रहे हैं।
जिसप्रकार सोने में जड़ने से माणिक का पराभव नहीं होता है; उसीप्रकार भगवान आत्मा का मनुष्यादि पर्यायों में रहने से पराभव नहीं होता।
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पराभव का मूल कारण क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्यदेव ने पानी के पूर का उदाहरण दिया है। हिमालय से निकला हुआ पानी निर्मल होता है; परंतु वह बहतेबहते जंगल में बहुत सारे नीम, चंदनादि पेड़ों से गुजरता है। वह चंदन के वन में से निकलता है तो सुगंधित हो जाता है और वह नीम के वृक्षों में से निकलता है तो कड़वा हो जाता है। इसमें उस पानी की मूल गंध नहीं रहती और न ही उसका मूल स्वभाव रहता है। इसप्रकार उस पानी का पराभव हुआ; क्योंकि उसका मूलस्वभाव तिरोहित हो गया है। इसीप्रकार इस आत्मा का पराभव इस मनुष्य पर्याय में जुड़ जाने से है । यह आत्मा मोह-राग-द्वेषभावों में से निकला है; इसलिए इसका पराभव हुआ है। ध्यान रहे आचार्यदेव ने यहाँ संयोग पर अपराध नहीं मड़ा है।
आचार्यदेव यहाँ कह रहे हैं कि पानी, नीम में अथवा चन्दन के वृक्ष में चढ़ा हुआ है अर्थात् नीम और चन्दन में भी पानीपन है, गीलापन है। यदि हम नीम की पत्तियों का रस निकालें, चन्दन का रस निकालें तो इसमें उसने तीन चीजें खोई हैं। पानी ने अपना स्वाद खोया है, अपनी गंध खोई है और प्रवाही स्वभाव खोया है; क्योंकि वह पानी वृक्ष में गया और
गाथा - १९८
१२९
उसी में रम गया। पानी का जो बहना स्वभाव था, वह बंद हो गया; जितना पानी उन वृक्षों ने सोख लिया, उस पानी का प्रवाही स्वभाव खतम हो गया। पानी का मूल स्वाद नहीं रहा, नीम के संयोग से कड़वा हो गया। इसीप्रकार गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। उसीप्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्मरूप परिणमित होने से अमूर्तत्व से मूर्तत्व हो गया; तब वह अमूर्तत्व, निरुपराग विशुद्धिमत्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। यही इस जीव की समस्या का मूल कारण है।
इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि आत्मस्वभाव के पराभव का कारण शरीरादि का संयोग नहीं है, अपितु शरीरादि संयोगों में आत्मा का अपनापन है, उन्हें अपना जानना - मानना है, उन्हीं से जुड़ जाना है, उन्हीं में रम जाना है।
आचार्य जयसेन ने तात्पर्यवृत्ति टीका में इस गाथा का अर्थ करते हुए पूर्णत: तत्त्वप्रदीपिका का अनुसरण किया है। उदाहरण भी वे ही दिये हैं। वृन्दावनदासजी इस गाथा के भाव को भी इसप्रकार प्रस्तुत करते हैं( मनहरण कवित्त )
नामकर्म निश्चे यह जीव को मनुष्य पशु,
नारकी सु देवरूप देह को बनावै है । तहां कर्मरूप उपयोग परिनवे जीव,
सहज सुभाव शुद्ध कहूँ न लहावे है ।। जैसे जल नीम चंदनादि माहिं गयौ सो,
प्रदेश और स्वाद निज दोनों न गहावै है । तैसे कर्मभाव परिनयौ जीव अमूरत,
चिदानंद वीतराग भाव नाहिं पावै है ।।९१ ।। यह बात सुनिश्चित है कि नाम नामक कर्म जीव की मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देवरूप देह को बनाता है। वहाँ जीव अपने उपयोग को भी उसीरूप परिणमित करता है। तात्पर्य यह है कि ऐसा ही जानने-मानने लगता है कि मैं मनुष्य हूँ आदि। इसप्रकार सहज स्वाभाविक शुद्धता को