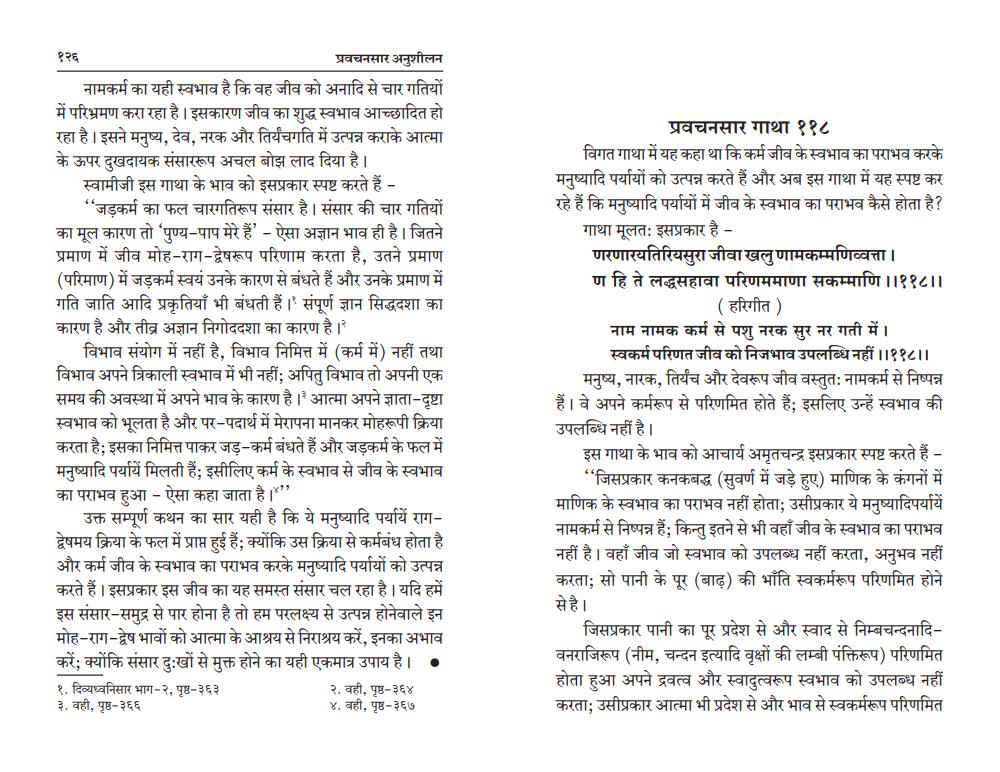________________
१२६
प्रवचनसार अनुशीलन __नामकर्म का यही स्वभाव है कि वह जीव को अनादि से चार गतियों में परिभ्रमण करा रहा है। इसकारण जीव का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है। इसने मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंचगति में उत्पन्न कराके आत्मा के ऊपर दुखदायक संसाररूप अचल बोझ लाद दिया है।
स्वामीजी इस गाथा के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं - __“जड़कर्म का फल चारगतिरूप संसार है। संसार की चार गतियों का मूल कारण तो 'पुण्य-पाप मेरे हैं' - ऐसा अज्ञान भाव ही है। जितने प्रमाण में जीव मोह-राग-द्वेषरूप परिणाम करता है, उतने प्रमाण (परिमाण) में जड़कर्म स्वयं उनके कारण से बंधते हैं और उनके प्रमाण में गति जाति आदि प्रकृतियाँ भी बंधती हैं। संपूर्ण ज्ञान सिद्धदशा का कारण है और तीव्र अज्ञान निगोददशा का कारण है।
विभाव संयोग में नहीं है, विभाव निमित्त में (कर्म में) नहीं तथा विभाव अपने त्रिकाली स्वभाव में भी नहीं; अपितु विभाव तो अपनी एक समय की अवस्था में अपने भाव के कारण है। आत्मा अपने ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव को भूलता है और पर-पदार्थ में मेरापना मानकर मोहरूपी क्रिया करता है; इसका निमित्त पाकर जड़-कर्म बंधते हैं और जड़कर्म के फल में मनुष्यादि पर्यायें मिलती हैं; इसीलिए कर्म के स्वभाव से जीव के स्वभाव का पराभव हुआ - ऐसा कहा जाता है।"
उक्त सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि ये मनुष्यादि पर्यायें रागद्वेषमय क्रिया के फल में प्राप्त हुई हैं; क्योंकि उस क्रिया से कर्मबंध होता है
और कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्यादि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं। इसप्रकार इस जीव का यह समस्त संसार चल रहा है। यदि हमें इस संसार-समुद्र से पार होना है तो हम परलक्ष्य से उत्पन्न होनेवाले इन मोह-राग-द्वेष भावों को आत्मा के आश्रय से निराश्रय करें, इनका अभाव करें; क्योंकि संसार दुःखों से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है। १. दिव्यध्वनिसार भाग-२, पृष्ठ-३६३
२. वही, पृष्ठ-३६४ ३. वहीं, पृष्ठ-३६६
४. वही, पृष्ठ-३६७
प्रवचनसार गाथा ११८ विगत गाथा में यह कहा था कि कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्यादि पर्यायों को उत्पन्न करते हैं और अब इस गाथा में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्यादि पर्यायों में जीव के स्वभाव का पराभव कैसे होता है? गाथा मूलतः इसप्रकार है - णरणारयतिरियसुरा जीवा खलुणामकम्मणिव्वत्ता । ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ।।११८।।
(हरिगीत) नाम नामक कर्म से पश नरक सर नर गती में।
स्वकर्म परिणत जीव को निजभाव उपलब्धि नहीं ।।११८।। मनुष्य, नारक, तिर्यंच और देवरूप जीव वस्तुत: नामकर्म से निष्पन्न हैं। वे अपने कर्मरूप से परिणमित होते हैं; इसलिए उन्हें स्वभाव की उपलब्धि नहीं है।
इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचन्द्र इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -
"जिसप्रकार कनकबद्ध (सुवर्ण में जड़े हुए) माणिक के कंगनों में माणिक के स्वभाव का पराभव नहीं होता; उसीप्रकार ये मनुष्यादिपर्यायें नामकर्म से निष्पन्न हैं; किन्तु इतने से भी वहाँ जीव के स्वभाव का पराभव नहीं है। वहाँ जीव जो स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, अनुभव नहीं करता; सो पानी के पूर (बाढ़) की भाँति स्वकर्मरूप परिणमित होने
जिसप्रकार पानी का पूर प्रदेश से और स्वाद से निम्बचन्दनादिवनराजिरूप (नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षों की लम्बी पंक्तिरूप) परिणमित होता हुआ अपने द्रवत्व और स्वादुत्वरूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता; उसीप्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्मरूप परिणमित