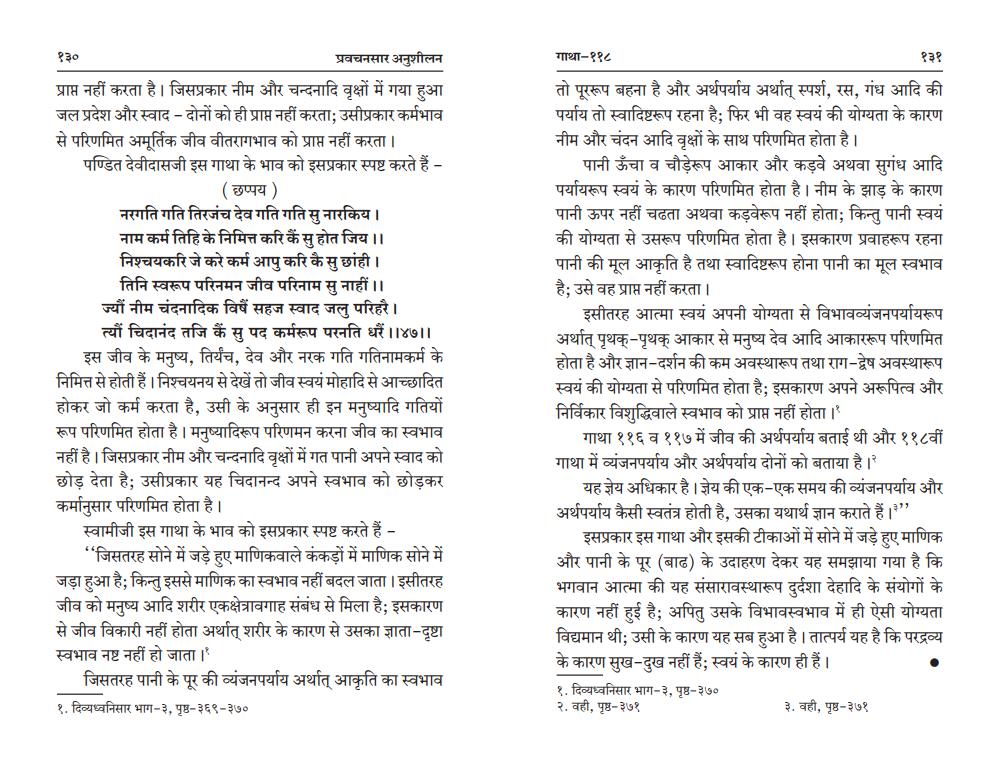________________
गाथा-११८
१३१
१३०
प्रवचनसार अनुशीलन प्राप्त नहीं करता है। जिसप्रकार नीम और चन्दनादि वृक्षों में गया हुआ जल प्रदेश और स्वाद - दोनों को ही प्राप्त नहीं करता; उसीप्रकार कर्मभाव से परिणमित अमूर्तिक जीव वीतरागभाव को प्राप्त नहीं करता । पण्डित देवीदासजी इस गाथा के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -
(छप्पय) नरगति गति तिरजंच देव गति गति सुनारकिय । नाम कर्म तिहि के निमित्त करि कैंसु होत जिय ।। निश्चयकरि जे करे कर्म आपु करि कै सु छांही। तिनि स्वरूप परिनमन जीव परिनाम सु नाहीं।। ज्यौं नीम चंदनादिक विर्षे सहज स्वाद जलु परिहरै।
त्यौं चिदानंद तजि कैं सु पद कर्मरूप परनति धरै ।।४७।। इस जीव के मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक गति गतिनामकर्म के निमित्त से होती हैं। निश्चयनय से देखें तो जीवस्वयं मोहादि से आच्छादित होकर जो कर्म करता है, उसी के अनुसार ही इन मनुष्यादि गतियों रूप परिणमित होता है। मनुष्यादिरूप परिणमन करना जीव का स्वभाव नहीं है। जिसप्रकार नीम और चन्दनादि वृक्षों में गत पानी अपने स्वाद को छोड़ देता है; उसीप्रकार यह चिदानन्द अपने स्वभाव को छोड़कर कर्मानुसार परिणमित होता है।
स्वामीजी इस गाथा के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं -
"जिसतरह सोने में जड़े हुए माणिकवाले कंकड़ों में माणिक सोने में जड़ा हुआ है; किन्तु इससे माणिक का स्वभाव नहीं बदल जाता । इसीतरह जीव को मनुष्य आदि शरीर एकक्षेत्रावगाह संबंध से मिला है; इसकारण से जीव विकारी नहीं होता अर्थात् शरीर के कारण से उसका ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता।
जिसतरह पानी के पूर की व्यंजनपर्याय अर्थात् आकृति का स्वभाव १. दिव्यध्वनिसार भाग-३, पृष्ठ-३६९-३७०
तो पूररूप बहना है और अर्थपर्याय अर्थात् स्पर्श, रस, गंध आदि की पर्याय तो स्वादिष्टरूप रहना है; फिर भी वह स्वयं की योग्यता के कारण नीम और चंदन आदि वृक्षों के साथ परिणमित होता है।
पानी ऊँचा व चौड़ेरूप आकार और कड़वे अथवा सुगंध आदि पर्यायरूप स्वयं के कारण परिणमित होता है। नीम के झाड़ के कारण पानी ऊपर नहीं चढता अथवा कड़वेरूप नहीं होता; किन्तु पानी स्वयं की योग्यता से उसरूप परिणमित होता है। इसकारण प्रवाहरूप रहना पानी की मूल आकृति है तथा स्वादिष्टरूप होना पानी का मूल स्वभाव है; उसे वह प्राप्त नहीं करता। ____ इसीतरह आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से विभावव्यंजनपर्यायरूप अर्थात् पृथक्-पृथक् आकार से मनुष्य देव आदि आकाररूप परिणमित होता है और ज्ञान-दर्शन की कम अवस्थारूप तथा राग-द्वेष अवस्थारूप स्वयं की योग्यता से परिणमित होता है; इसकारण अपने अरूपित्व और निर्विकार विशुद्धिवाले स्वभाव को प्राप्त नहीं होता।
गाथा ११६ व ११७ में जीव की अर्थपर्याय बताई थी और ११८वीं गाथा में व्यंजनपर्याय और अर्थपर्याय दोनों को बताया है।
यह ज्ञेय अधिकार है। ज्ञेय की एक-एक समय की व्यंजनपर्याय और अर्थपर्याय कैसी स्वतंत्र होती है, उसका यथार्थ ज्ञान कराते हैं।"
इसप्रकार इस गाथा और इसकी टीकाओं में सोने में जड़े हुए माणिक और पानी के पूर (बाढ) के उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि भगवान आत्मा की यह संसारावस्थारूप दुर्दशा देहादि के संयोगों के कारण नहीं हुई है; अपितु उसके विभावस्वभाव में ही ऐसी योग्यता विद्यमान थी; उसी के कारण यह सब हुआ है । तात्पर्य यह है कि परद्रव्य के कारण सुख-दुख नहीं हैं; स्वयं के कारण ही हैं। १. दिव्यध्वनिसार भाग-३, पृष्ठ-३७० २. वही, पृष्ठ-३७१
३. वही, पृष्ठ-३७१