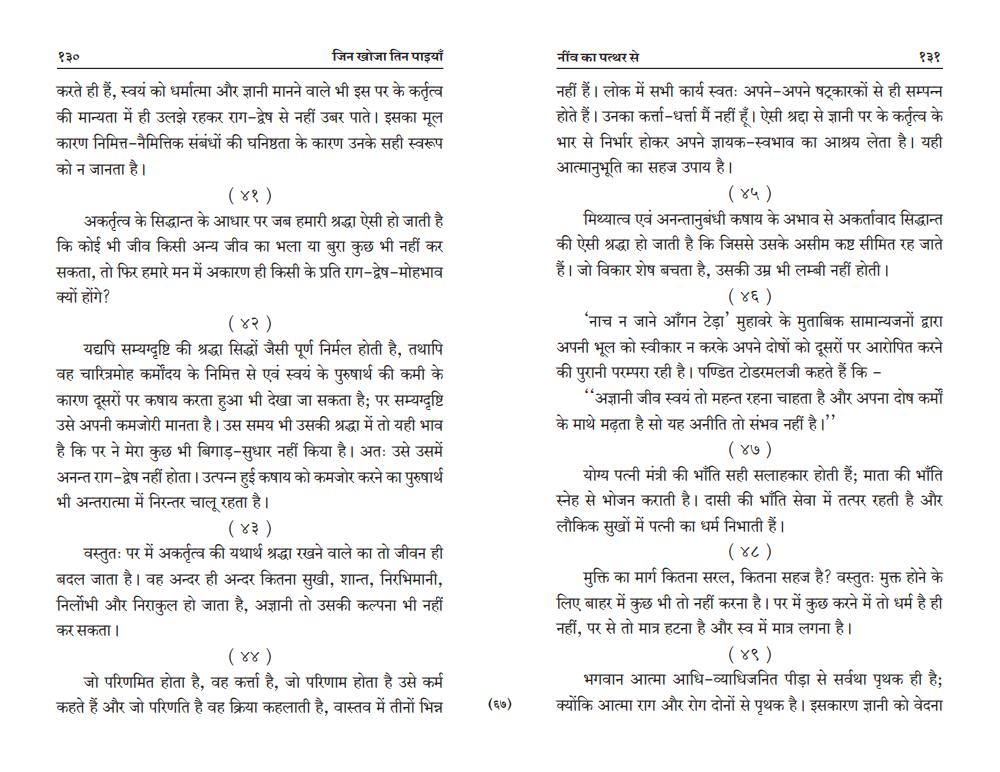________________
जिन खोजा तिन पाइयाँ
१३०
करते ही हैं, स्वयं को धर्मात्मा और ज्ञानी मानने वाले भी इस पर के कर्तृत्व की मान्यता में ही उलझे रहकर राग-द्वेष से नहीं उबर पाते। इसका मूल कारण निमित्तनैमित्तिक संबंधों की घनिष्ठता के कारण उनके सही स्वरूप को न जानता है।
( ४१ )
अकर्तृत्व के सिद्धान्त के आधार पर जब हमारी श्रद्धा ऐसी हो जाती है कि कोई भी जीव किसी अन्य जीव का भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर हमारे मन में अकारण ही किसी के प्रति राग-द्वेष-मोहभाव क्यों होंगे?
( ४२ )
यद्यपि सम्यग्दृष्टि की श्रद्धा सिद्धों जैसी पूर्ण निर्मल होती है, तथापि वह चारित्रमोह कर्मोंदय के निमित्त से एवं स्वयं के पुरुषार्थ की कमी के कारण दूसरों पर कषाय करता हुआ भी देखा जा सकता है; पर सम्यग्दृष्टि उसे अपनी कमजोरी मानता है। उस समय भी उसकी श्रद्धा में तो यही भाव है कि पर ने मेरा कुछ भी बिगाड़-सुधार नहीं किया है। अतः उसे उसमें अनन्त राग-द्वेष नहीं होता । उत्पन्न हुई कषाय को कमजोर करने का पुरुषार्थ भी अन्तरात्मा में निरन्तर चालू रहता है।
( ४३ )
वस्तुतः पर में अकर्तृत्व की यथार्थ श्रद्धा रखने वाले का तो जीवन ही बदल जाता है। वह अन्दर ही अन्दर कितना सुखी, शान्त, निरभिमानी, निर्लोभी और निराकुल हो जाता है, अज्ञानी तो उसकी कल्पना भी नहीं
कर सकता ।
( ४४ )
जो परिणमित होता है, वह कर्त्ता है, जो परिणाम होता है उसे कर्म कहते हैं और जो परिणति है वह क्रिया कहलाती है, वास्तव में तीनों भिन्न
(६७)
नींव का पत्थर से
नहीं हैं। लोक में सभी कार्य स्वतः अपने-अपने षट्कारकों से ही सम्पन्न होते हैं। उनका कर्ता-धर्ता मैं नहीं हूँ। ऐसी श्रद्दा से ज्ञानी पर के कर्तृत्व के भार से निर्भर होकर अपने ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेता है। यही आत्मानुभूति का सहज उपाय है।
१३१
(४५)
मिथ्यात्व एवं अनन्तानुबंधी कषाय के अभाव से अकर्तावाद सिद्धान्त की ऐसी श्रद्धा हो जाती है कि जिससे उसके असीम कष्ट सीमित रह जाते हैं। जो विकार शेष बचता है, उसकी उम्र भी लम्बी नहीं होती।
( ४६ )
'नाच न जाने आँगन टेड़ा' मुहावरे के मुताबिक सामान्यजनों द्वारा अपनी भूल को स्वीकार न करके अपने दोषों को दूसरों पर आरोपित करने की पुरानी परम्परा रही है। पण्डित टोडरमलजी कहते हैं कि -
“अज्ञानी जीव स्वयं तो महन्त रहना चाहता है और अपना दोष कर्मों के माथे मढ़ता है सो यह अनीति तो संभव नहीं है। "
( ४७ )
योग्य पत्नी मंत्री की भाँति सही सलाहकार होती हैं; माता की भाँति स्नेह से भोजन कराती है। दासी की भाँति सेवा में तत्पर रहती है और लौकिक सुखों में पत्नी का धर्म निभाती हैं।
( ४८ )
मुक्ति का मार्ग कितना सरल, कितना सहज है ? वस्तुतः मुक्त होने के लिए बाहर में कुछ भी तो नहीं करना है। पर में कुछ करने में तो धर्म है नहीं, पर से तो मात्र हटना है और स्व में मात्र लगना है।
( ४९ )
भगवान आत्मा आधि-व्याधिजनित पीड़ा से सर्वथा पृथक ही है; क्योंकि आत्मा राग और रोग दोनों से पृथक है। इसकारण ज्ञानी को वेदना