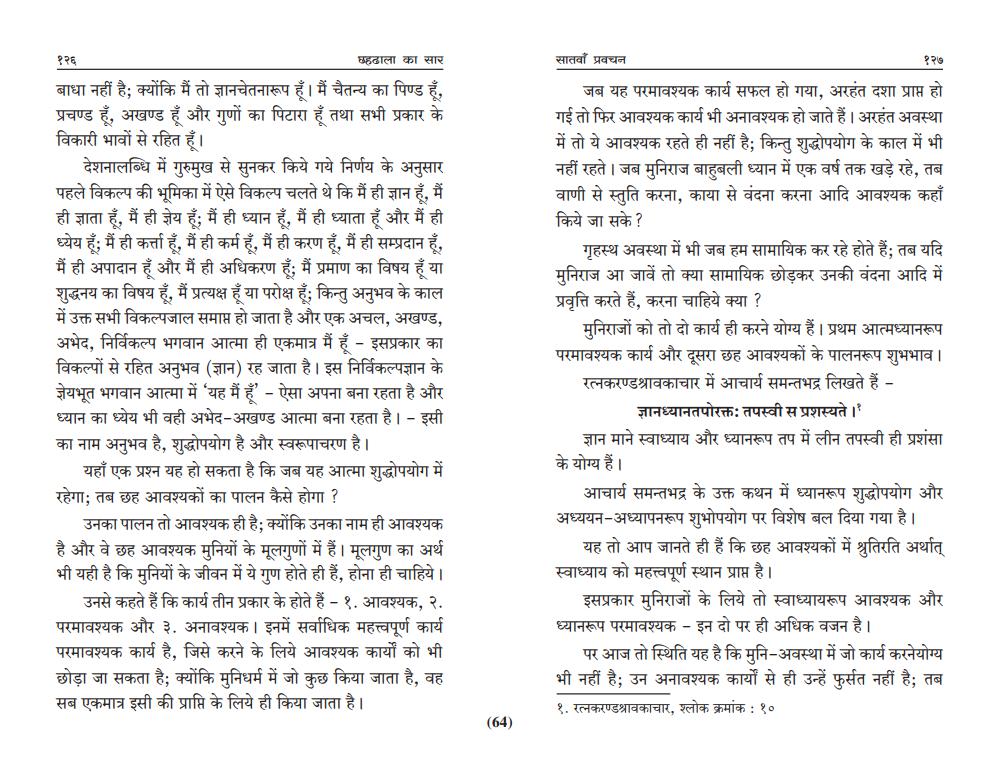________________
छहठाला का सार
सातवाँ प्रवचन
१२६ बाधा नहीं है; क्योंकि मैं तो ज्ञानचेतनारूप हूँ। मैं चैतन्य का पिण्ड हूँ, प्रचण्ड हूँ, अखण्ड हूँ और गुणों का पिटारा हूँ तथा सभी प्रकार के विकारी भावों से रहित हूँ।
देशनालब्धि में गुरुमुख से सुनकर किये गये निर्णय के अनुसार पहले विकल्प की भूमिका में ऐसे विकल्प चलते थे कि मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ; मैं ही ध्यान हूँ, मैं ही ध्याता हूँ और मैं ही ध्येय हूँ; मैं ही कर्ता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करण हूँ, मैं ही सम्प्रदान हूँ, मैं ही अपादान हूँ और मैं ही अधिकरण हूँ; मैं प्रमाण का विषय हूँ या शुद्धनय का विषय हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ या परोक्ष हूँ; किन्तु अनुभव के काल में उक्त सभी विकल्पजाल समाप्त हो जाता है और एक अचल, अखण्ड, अभेद, निर्विकल्प भगवान आत्मा ही एकमात्र मैं हूँ - इसप्रकार का विकल्पों से रहित अनुभव (ज्ञान) रह जाता है। इस निर्विकल्पज्ञान के ज्ञेयभूत भगवान आत्मा में 'यह मैं हूँ' - ऐसा अपना बना रहता है और ध्यान का ध्येय भी वही अभेद-अखण्ड आत्मा बना रहता है। - इसी का नाम अनुभव है, शुद्धोपयोग है और स्वरूपाचरण है।
यहाँ एक प्रश्न यह हो सकता है कि जब यह आत्मा शुद्धोपयोग में रहेगा; तब छह आवश्यकों का पालन कैसे होगा ?
उनका पालन तो आवश्यक ही है; क्योंकि उनका नाम ही आवश्यक है और वे छह आवश्यक मुनियों के मूलगुणों में हैं। मूलगुण का अर्थ भी यही है कि मुनियों के जीवन में ये गुण होते ही हैं, होना ही चाहिये।
उनसे कहते हैं कि कार्य तीन प्रकार के होते हैं - १. आवश्यक, २. परमावश्यक और ३. अनावश्यक । इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य परमावश्यक कार्य है, जिसे करने के लिये आवश्यक कार्यों को भी छोड़ा जा सकता है; क्योंकि मुनिधर्म में जो कुछ किया जाता है, वह सब एकमात्र इसी की प्राप्ति के लिये ही किया जाता है।
१२७ जब यह परमावश्यक कार्य सफल हो गया, अरहंत दशा प्राप्त हो गई तो फिर आवश्यक कार्य भी अनावश्यक हो जाते हैं। अरहंत अवस्था में तो ये आवश्यक रहते ही नहीं है; किन्तु शुद्धोपयोग के काल में भी नहीं रहते । जब मुनिराज बाहुबली ध्यान में एक वर्ष तक खड़े रहे, तब वाणी से स्तुति करना, काया से वंदना करना आदि आवश्यक कहाँ किये जा सके? ____ गृहस्थ अवस्था में भी जब हम सामायिक कर रहे होते हैं; तब यदि मुनिराज आ जावें तो क्या सामायिक छोड़कर उनकी वंदना आदि में प्रवृत्ति करते हैं, करना चाहिये क्या ?
मुनिराजों को तो दो कार्य ही करने योग्य हैं। प्रथम आत्मध्यानरूप परमावश्यक कार्य और दूसरा छह आवश्यकों के पालनरूप शुभभाव। रत्नकरण्डश्रावकाचार में आचार्य समन्तभद्र लिखते हैं -
ज्ञानध्यानतपोरक्त: तपस्वी स प्रशस्यते ।' ज्ञान माने स्वाध्याय और ध्यानरूप तप में लीन तपस्वी ही प्रशंसा के योग्य हैं।
आचार्य समन्तभद्र के उक्त कथन में ध्यानरूप शुद्धोपयोग और अध्ययन-अध्यापनरूप शुभोपयोग पर विशेष बल दिया गया है।
यह तो आप जानते ही हैं कि छह आवश्यकों में श्रुतिरति अर्थात् स्वाध्याय को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
इसप्रकार मुनिराजों के लिये तो स्वाध्यायरूप आवश्यक और ध्यानरूप परमावश्यक - इन दो पर ही अधिक वजन है।
पर आज तो स्थिति यह है कि मुनि-अवस्था में जो कार्य करनेयोग्य भी नहीं है; उन अनावश्यक कार्यों से ही उन्हें फुर्सत नहीं है; तब १. रत्नकरण्डश्रावकाचार, श्लोक क्रमांक : १०
(64)