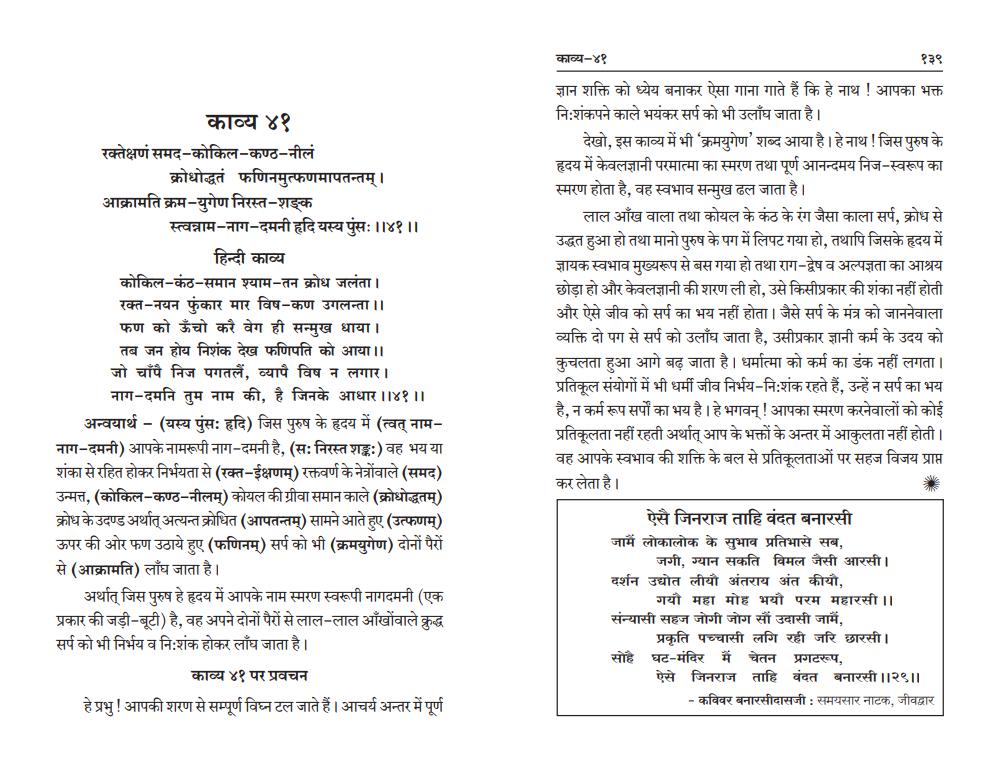________________
काव्य ४१
रक्तेक्षणं समद - कोकिल-कण्ठ-नीलं
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् । आक्रामति क्रम-युगेण निरस्त - शङ्क
स्त्वन्नाम - नाग- दमनी हृदि यस्य पुंसः । । ४१ ।। हिन्दी काव्य
कोकिल - कंठ - समान श्याम-तन क्रोध जलता । रक्त - नयन फुंकार मार विष-कण उगलन्ता ।। फण को ऊँचो करै वेग ही सन्मुख धाया । तब जन होय निशंक देख फणिपति को आया ।।
जो चाँपै निज पगतले, व्यापै विष न लगार ।
नाग - दमनि तुम नाम की, है जिनके आधार ।। ४१ ।। अन्वयार्थ - (यस्य पुंसः हृदि) जिस पुरुष के हृदय में (त्वत् नामनाग - दमनी) आपके नामरूपी नाग-दमनी है, (सः निरस्त शङ्कः) वह भय या शंका से रहित होकर निर्भयता से (रक्त ईक्षणम्) रक्तवर्ण के नेत्रोंवाले (समद) उन्मत्त, (कोकिल-कण्ठ-नीलम् ) कोयल की ग्रीवा समान काले (क्रोधोद्धतम्) क्रोध के उदण्ड अर्थात् अत्यन्त क्रोधित (आपतन्तम्) सामने आते हुए (उत्फणम्) ऊपर की ओर फण उठाये हुए (फणिनम् ) सर्प को भी (क्रमयुगेण) दोनों पैरों से (आक्रामति) लाँघ जाता है।
अर्थात् जिस पुरुष हे हृदय में आपके नाम स्मरण स्वरूपी नागदमनी (एक प्रकार की जड़ी-बूटी) है, वह अपने दोनों पैरों से लाल-लाल आँखोंवाले क्रुद्ध सर्प को भी निर्भय व निःशंक होकर लाँघ जाता है।
काव्य ४१ पर प्रवचन
हे प्रभु! आपकी शरण से सम्पूर्ण विघ्न टल जाते हैं। आचर्य अन्तर में पूर्ण
काव्य- ४१
१३९
ज्ञान शक्ति को ध्येय बनाकर ऐसा गाना गाते हैं कि हे नाथ ! आपका भक्त नि:शंकपने काले भयंकर सर्प को भी उलाँघ जाता है।
देखो, इस काव्य में भी 'क्रमयुगेण' शब्द आया है। हे नाथ ! जिस पुरुष के हृदय में केवलज्ञानी परमात्मा का स्मरण तथा पूर्ण आनन्दमय निज स्वरूप का स्मरण होता है, वह स्वभाव सन्मुख ढल जाता है।
लाल आँख वाला तथा कोयल के कंठ के रंग जैसा काला सर्प, क्रोध से उद्धत हुआ हो तथा मानो पुरुष के पग में लिपट गया हो, तथापि जिसके हृदय में ज्ञायक स्वभाव मुख्यरूप से बस गया हो तथा राग-द्वेष व अल्पज्ञता का आश्रय छोड़ा हो और केवलज्ञानी की शरण ली हो, उसे किसीप्रकार की शंका नहीं होती और ऐसे जीव को सर्प का भय नहीं होता। जैसे सर्प के मंत्र को जाननेवाला व्यक्ति दो पग से सर्प को उलाँघ जाता है, उसीप्रकार ज्ञानी कर्म के उदय को कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। धर्मात्मा को कर्म का डंक नहीं लगता। प्रतिकूल संयोगों में भी धर्मी जीव निर्भय-नि:शंक रहते हैं, उन्हें न सर्प का भय है, न कर्म रूप सर्पों का भय है। हे भगवन् ! आपका स्मरण करनेवालों को कोई प्रतिकूलता नहीं रहती अर्थात् आप के भक्तों के अन्तर में आकुलता नहीं होती । वह आपके स्वभाव की शक्ति के बल से प्रतिकूलताओं पर सहज विजय प्राप्त कर लेता है।
ऐसै जिनराज ताहि वंदत बनारसी जामैं लोकालोक के सुभाव प्रतिभासे सब,
जगी, ग्यान सकति विमल जैसी आरसी । दर्शन उद्योत लीयौ अंतराय अंत कीयौ,
गयौ महा मोह भयौ परम महारसी ।। संन्यासी सहज जोगी जोग साँ उदासी जामँ,
प्रकृति पच्चासी लगि रही जरि छारसी । सोहै घट मंदिर मैं चेतन प्रगटरूप,
ऐसे जिनराज ताहि वंदत बनारसी ||२९||
- कविवर बनारसीदासजी: समयसार नाटक, जीवद्वार