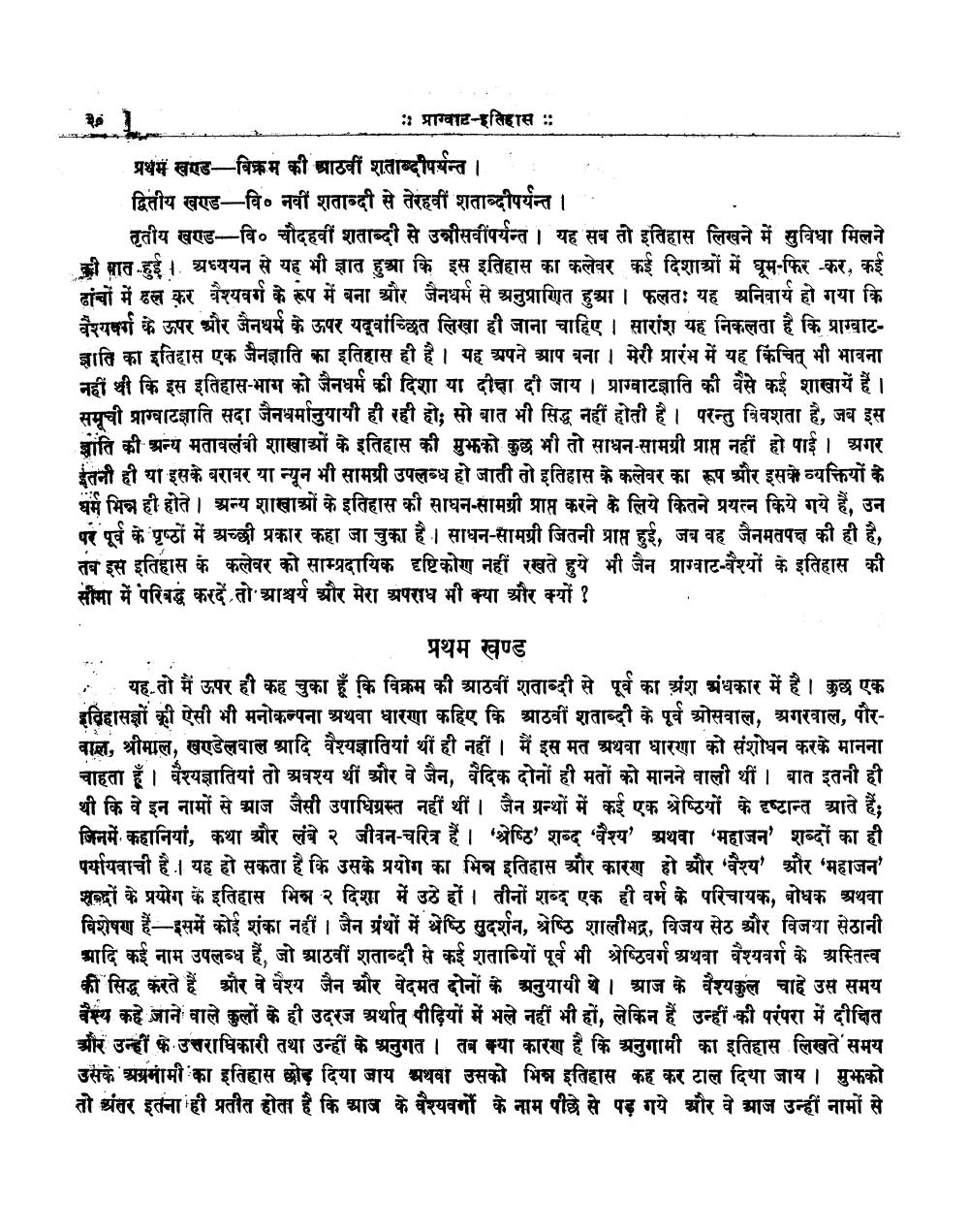________________
प्राग्वाट-इतिहास::
प्रथम खण्ड–विक्रम की पाठवीं शताब्दीपर्यन्त । द्वितीय खण्ड-वि० नवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दीपर्यन्त ।
तृतीय खण्ड-वि० चौदहवीं शताब्दी से उन्नीसवींपर्यन्त । यह सब तो इतिहास लिखने में सुविधा मिलने की मात हुई। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि इस इतिहास का कलेवर कई दिशाओं में घूम-फिर -कर, कई ढांचों में हल कर वैश्यवर्ग के रूप में बना और जैनधर्म से अनुप्राणित हुआ । फलतः यह अनिवार्य हो गया कि वैश्यवर्ग के ऊपर और जैनधर्म के ऊपर यद्वांच्छित लिखा ही जाना चाहिए । सारांश यह निकलता है कि प्राग्वाटजाति का इतिहास एक जैनज्ञाति का इतिहास ही है। यह अपने आप बना । मेरी प्रारंभ में यह किंचित् भी भावना नहीं थी कि इस इतिहास-भाग को जैनधर्म की दिशा या दीक्षा दी जाय । प्राग्वाटज्ञाति की वैसे कई शाखायें हैं। समची प्राग्वाटज्ञाति सदा जैनधर्मानुयायी ही रही हो; सो बात भी सिद्ध नहीं होती है। परन्तु विवशता है, जब इस शांति की अन्य मतावलंबी शाखाओं के इतिहास की मुझको कुछ भी तो साधन-सामग्री प्राप्त नहीं हो पाई। अगर इतनी ही या इसके बराबर या न्यून भी सामग्री उपलब्ध हो जाती तो इतिहास के कलेवर का रूप और इसके व्यक्तियों के धर्म भिन्न ही होते। अन्य शाखाओं के इतिहास की साधन-सामग्री प्राप्त करने के लिये कितने प्रयत्न पर पूर्व के पृष्ठों में अच्छी प्रकार कहा जा चुका है। साधन-सामग्री जितनी प्राप्त हुई, जब वह जैनमतपक्ष की ही है, तव इस इतिहास के कलेवर को साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं रखते हुये भी जैन प्राग्वाट-वैश्यों के इतिहास की सीमा में परिबद्ध करदें तो आश्चर्य और मेरा अपराध भी क्या और क्यों ?
प्रथम खण्ड , यह.तो मैं ऊपर ही कह चुका हूँ कि विक्रम की आठवीं शताब्दी से पूर्व का अंश अंधकार में है। कुछ एक इतिहासज्ञों की ऐसी भी मनोकल्पना अथवा धारणा कहिए कि आठवीं शताब्दी के पूर्व ओसवाल, अगरवाल, पौरवाल, श्रीमाल, खण्डेलवाल आदि वैश्यज्ञातियां थी ही नहीं। मैं इस मत अथवा धारणा को संशोधन करके मानना चाहता हूँ। वैश्यज्ञातियां तो अवश्य थीं और वे जैन, वैदिक दोनों ही मतों को मानने वाली थीं। बात इतनी ही थी कि वे इन नामों से आज जैसी उपाधिग्रस्त नहीं थीं। जैन ग्रन्थों में कई एक श्रेष्ठियों के दृष्टान्त आते हैं; जिनमें कहानियां, कथा और लंबे २ जीवन-चरित्र हैं। 'श्रेष्ठि' शब्द 'वैश्य' अथवा 'महाजन' शब्दों का ही पर्यायवाची है । यह हो सकता है कि उसके प्रयोग का भिन्न इतिहास और कारण हो और 'वैश्य' और 'महाजन' शब्दों के प्रयोग के इतिहास भिन्न २ दिशा में उठे हों। तीनों शब्द एक ही वर्म के परिचायक, बोधक अथवा विशेषण हैं-इसमें कोई शंका नहीं । जैन ग्रंथों में श्रेष्ठि सुदर्शन, श्रेष्ठि शालीभद्र, विजय सेठ और विजया सेठानी
आदि कई नाम उपलब्ध हैं, जो आठवीं शताब्दी से कई शताव्यिों पूर्व भी श्रेष्ठिवर्ग अथवा वैश्यवर्ग के अस्तित्व की सिद्ध करते हैं और वे वैश्य जैन और वेदमत दोनों के अनुयायी थे। आज के वैश्यकुल चाहे उस समय वैस्य कहे जाने वाले कुलों के ही उदरज अर्थात पीढियों में भले नहीं भी हों. लेकिन हैं उन्हीं की परंपरा में दीक्षित
और उन्हीं के उत्तराधिकारी तथा उन्हीं के अनुगत । तब क्या कारण है कि अनुगामी का इतिहास लिखते समय उसके अग्रमामी का इतिहास छोड़ दिया जाय अथवा उसको भिन्न इतिहास कह कर टाल दिया जाय । मुझको तो अंतर इतना ही प्रतीत होता है कि आज के वैश्यवर्गों के नाम पीछे से पड़ गये और वे आज उन्हीं नामों से