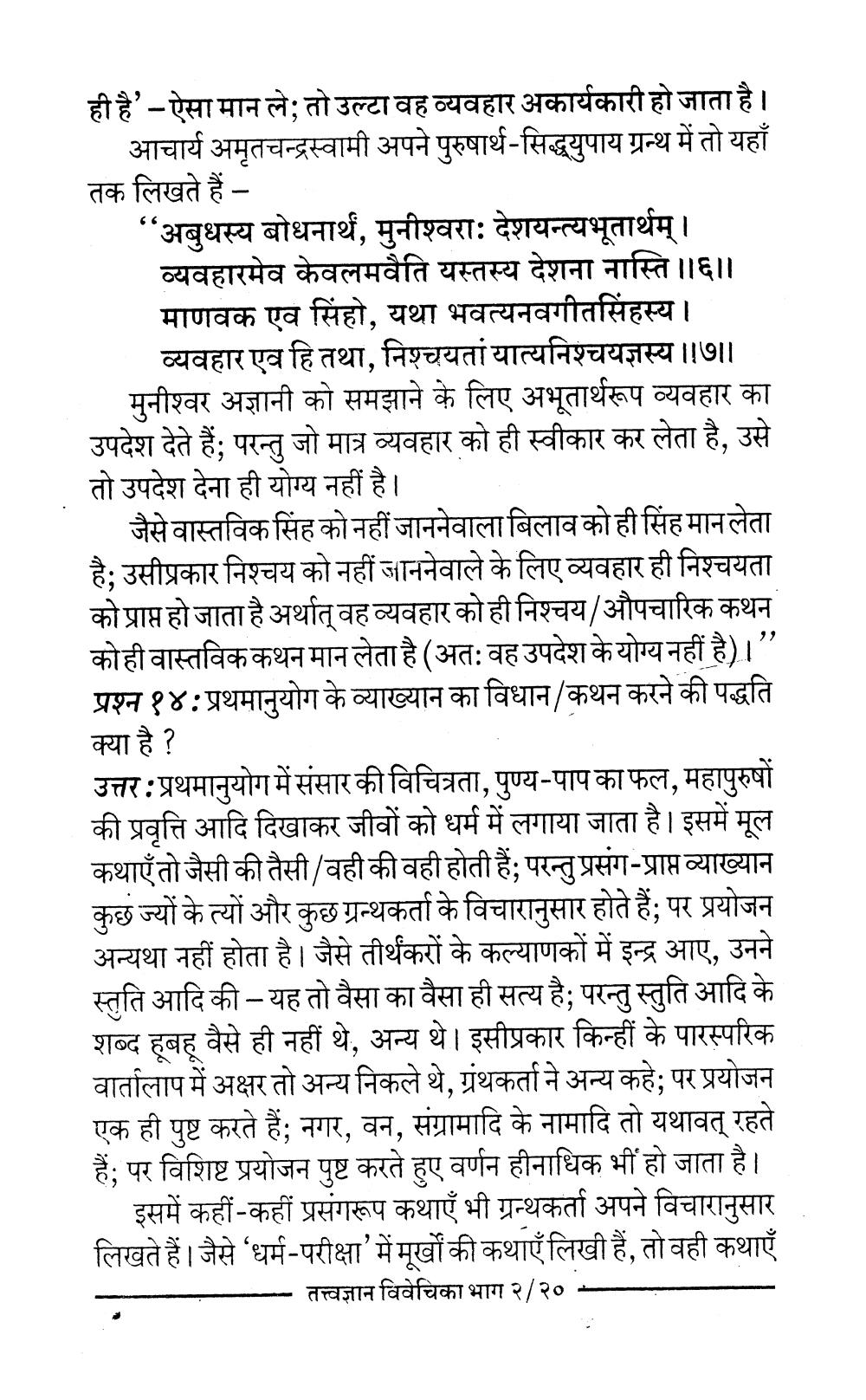________________
ही है' - ऐसा मान ले; तो उल्टा वह व्यवहार अकार्यकारी हो जाता है । आचार्य अमृतचन्द्रस्वामी अपने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ग्रन्थ में तो यहाँ तक लिखते हैं.
-
"अबुधस्य बोधनार्थं, मुनीश्वराः देशयन्त्यभूतार्थम् । व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥ माणवक एव सिंहो, यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य । व्यवहार एव हि तथा, निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥ मुनीश्वर अज्ञानी को समझाने के लिए अभूतार्थरूप व्यवहार का उपदेश देते हैं; परन्तु जो मात्र व्यवहार को ही स्वीकार कर लेता है, उसे तो उपदेश देना ही योग्य नहीं है।
जैसे वास्तविक सिंह को नहीं जाननेवाला बिलाव को ही सिंह मान लेता है; उसीप्रकार निश्चय को नहीं जाननेवाले के लिए व्यवहार ही निश्चयता को प्राप्त हो जाता है अर्थात् वह व्यवहार को ही निश्चय / औपचारिक कथन को ही वास्तविक कथन मान लेता है (अत: वह उपदेश के योग्य नहीं है)। ' प्रश्न १४ : प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान / कथन करने की पद्धति क्या है ?
99
उत्तर : प्रथमानुयोग में संसार की विचित्रता, पुण्य-पाप का फल, महापुरुषों की प्रवृत्ति आदि दिखाकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है। इसमें मूल कथाएँ तो जैसी की तैसी / वही की वही होती हैं; परन्तु प्रसंग प्राप्त व्याख्यान कुछ ज्यों के त्यों और कुछ ग्रन्थकर्ता के विचारानुसार होते हैं; पर प्रयोजन अन्यथा नहीं होता है। जैसे तीर्थंकरों के कल्याणकों में इन्द्र आए, उनने स्तुति आदि की - यह तो वैसा का वैसा ही सत्य है; परन्तु स्तुति आदि के शब्द हूबहू वैसे ही नहीं थे, अन्य थे। इसीप्रकार किन्हीं के पारस्परिक वार्तालाप में अक्षर तो अन्य निकले थे, ग्रंथकर्ता ने अन्य कहे; पर प्रयोजन एक ही पुष्ट करते हैं; नगर, वन, संग्रामादि के नामादि तो यथावत् रहते हैं; पर विशिष्ट प्रयोजन पुष्ट करते हुए वर्णन हीनाधिक भी हो जाता है।
इसमें कहीं-कहीं प्रसंगरूप कथाएँ भी ग्रन्थकर्ता अपने विचारानुसार लिखते हैं। जैसे 'धर्म-परीक्षा' में मूर्खों की कथाएँ लिखी हैं, तो वही कथाएँ तत्त्वज्ञान विवेचिका भाग २ /२०