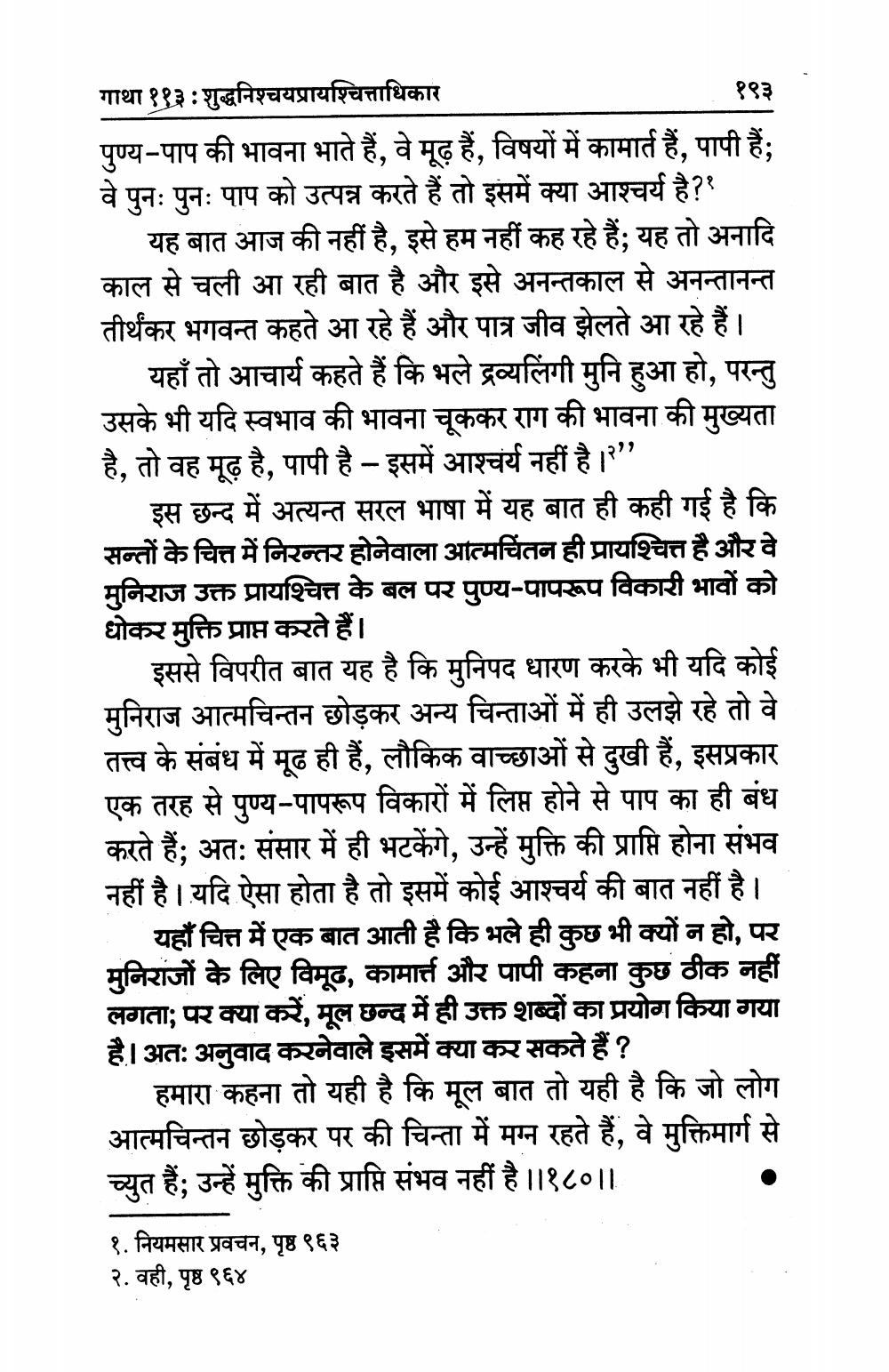________________
गाथा १९३ :
शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकार
१९३
पुण्य-पाप की भावना भाते हैं, वे मूढ़ हैं, विषयों में कामार्त हैं, पापी हैं; वे पुनः पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है ? १
यह बात आज की नहीं है, इसे हम नहीं कह रहे हैं; यह तो अनादि काल से चली आ रही बात है और इसे अनन्तकाल से अनन्तानन्त तीर्थंकर भगवन्त कहते आ रहे हैं और पात्र जीव झेलते आ रहे हैं।
यहाँ तो आचार्य कहते हैं कि भले द्रव्यलिंगी मुनि हुआ हो, परन्तु उसके भी यदि स्वभाव की भावना चूककर राग की भावना की मुख्यता है, तो वह मूढ़ है, पापी है - इसमें आश्चर्य नहीं है।"
इस छन्द में अत्यन्त सरल भाषा में यह बात ही कही गई है कि सन्तों के चित्त में निरन्तर होनेवाला आत्मचिंतन ही प्रायश्चित्त है और वे मुनिराज उक्त प्रायश्चित्त के बल पर पुण्य-पापरूप विकारी भावों को धोकर मुक्ति प्राप्त करते हैं।
इससे विपरीत बात यह है कि मुनिपद धारण करके भी यदि कोई मुनिराज आत्मचिन्तन छोड़कर अन्य चिन्ताओं में ही उलझे रहे तो वे तत्त्व के संबंध में मूढ ही हैं, लौकिक वाच्छाओं से दुखी हैं, इसप्रकार एक तरह से पुण्य-पापरूप विकारों में लिप्त होने से पाप का ही बंध करते हैं; अत: संसार में ही भटकेंगे, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
यहाँ चित्त में एक बात आती है कि भले ही कुछ भी क्यों न हो, पर मुनिराजों के लिए विमूढ, कामार्त्त और पापी कहना कुछ ठीक नहीं लगता; पर क्या करें, मूल छन्द में ही उक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। अत: अनुवाद करनेवाले इसमें क्या कर सकते हैं ?
हमारा कहना तो यही है कि मूल बात तो यही है कि जो लोग आत्मचिन्तन छोड़कर पर की चिन्ता में मग्न रहते हैं, वे मुक्तिमार्ग से च्युत हैं; उन्हें मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है ।। १८० ।।
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ ९६३ २. वही, पृष्ठ ९६४