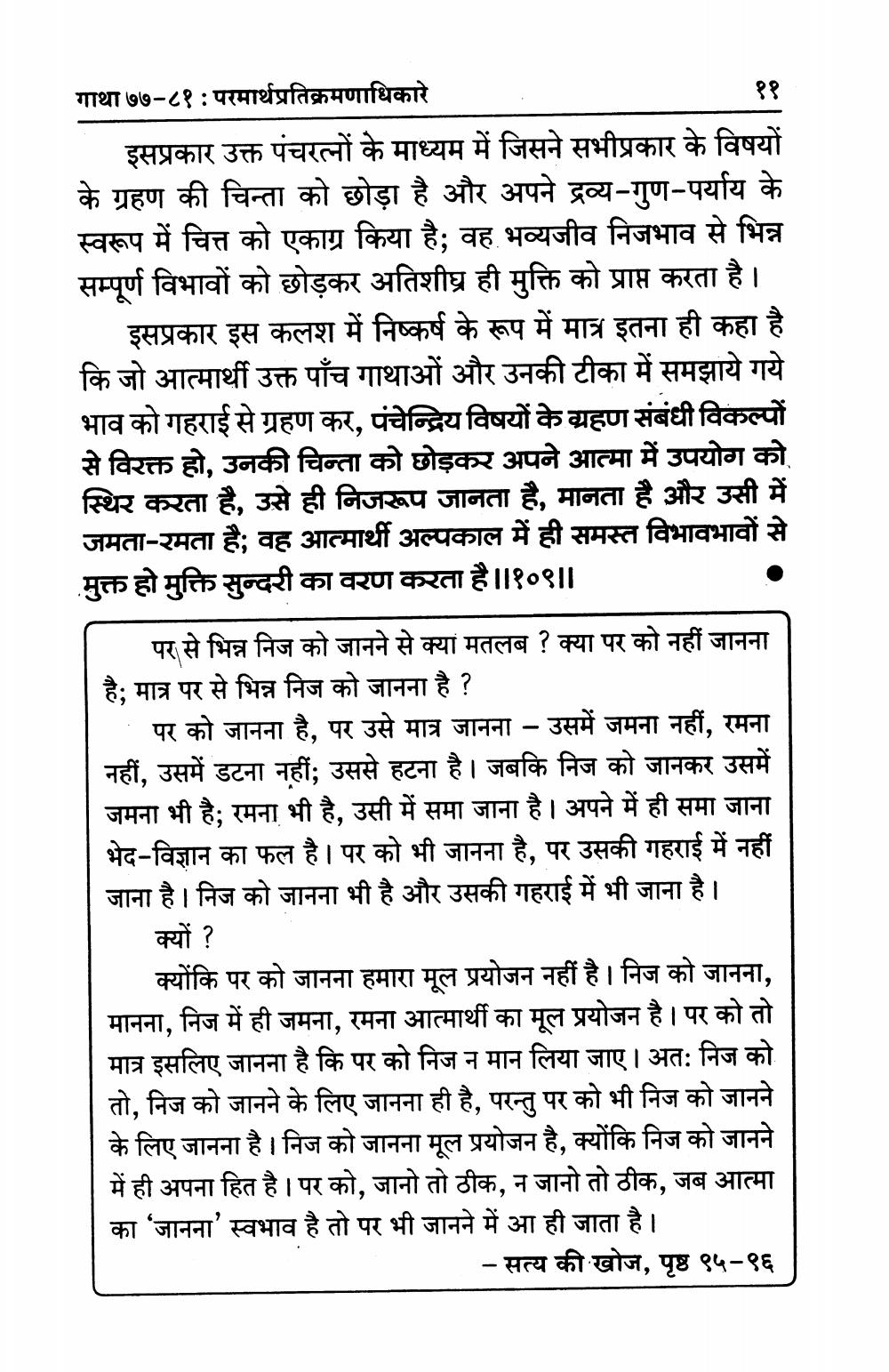________________
गाथा ७७-८१ : परमार्थप्रतिक्रमणाधिकारे
इसप्रकार उक्त पंचरत्नों के माध्यम में जिसने सभीप्रकार के विषयों के ग्रहण की चिन्ता को छोड़ा है और अपने द्रव्य-गुण-पर्याय के स्वरूप में चित्त को एकाग्र किया है; वह भव्यजीव निजभाव से भिन्न सम्पूर्ण विभावों को छोड़कर अतिशीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है।
इसप्रकार इस कलश में निष्कर्ष के रूप में मात्र इतना ही कहा है कि जो आत्मार्थी उक्त पाँच गाथाओं और उनकी टीका में समझाये गये भाव को गहराई से ग्रहण कर, पंचेन्द्रिय विषयों के ग्रहण संबंधी विकल्पों से विरक्त हो, उनकी चिन्ता को छोड़कर अपने आत्मा में उपयोग को स्थिर करता है, उसे ही निजरूप जानता है, मानता है और उसी में जमता-रमता है; वह आत्मार्थी अल्पकाल में ही समस्त विभावभावों से मुक्त हो मुक्ति सुन्दरी का वरण करता है।।१०९||
पर से भिन्न निज को जानने से क्या मतलब ? क्या पर को नहीं जानना है; मात्र पर से भिन्न निज को जानना है ?
- पर को जानना है, पर उसे मात्र जानना – उसमें जमना नहीं, रमना नहीं, उसमें डटना नहीं; उससे हटना है। जबकि निज को जानकर उसमें जमना भी है; रमना भी है, उसी में समा जाना है। अपने में ही समा जाना भेद-विज्ञान का फल है। पर को भी जानना है, पर उसकी गहराई में नहीं जाना है। निज को जानना भी है और उसकी गहराई में भी जाना है।
क्यों ?
क्योंकि पर को जानना हमारा मूल प्रयोजन नहीं है। निज को जानना, मानना, निज में ही जमना, रमना आत्मार्थी का मूल प्रयोजन है। पर को तो मात्र इसलिए जानना है कि पर को निज न मान लिया जाए। अत: निज को तो, निज को जानने के लिए जानना ही है, परन्तु पर को भी निज को जानने के लिए जानना है। निज को जानना मूल प्रयोजन है, क्योंकि निज को जानने में ही अपना हित है । पर को, जानो तो ठीक, न जानो तो ठीक, जब आत्मा का ‘जानना' स्वभाव है तो पर भी जानने में आ ही जाता है।
- सत्य की खोज, पृष्ठ ९५-९६ |