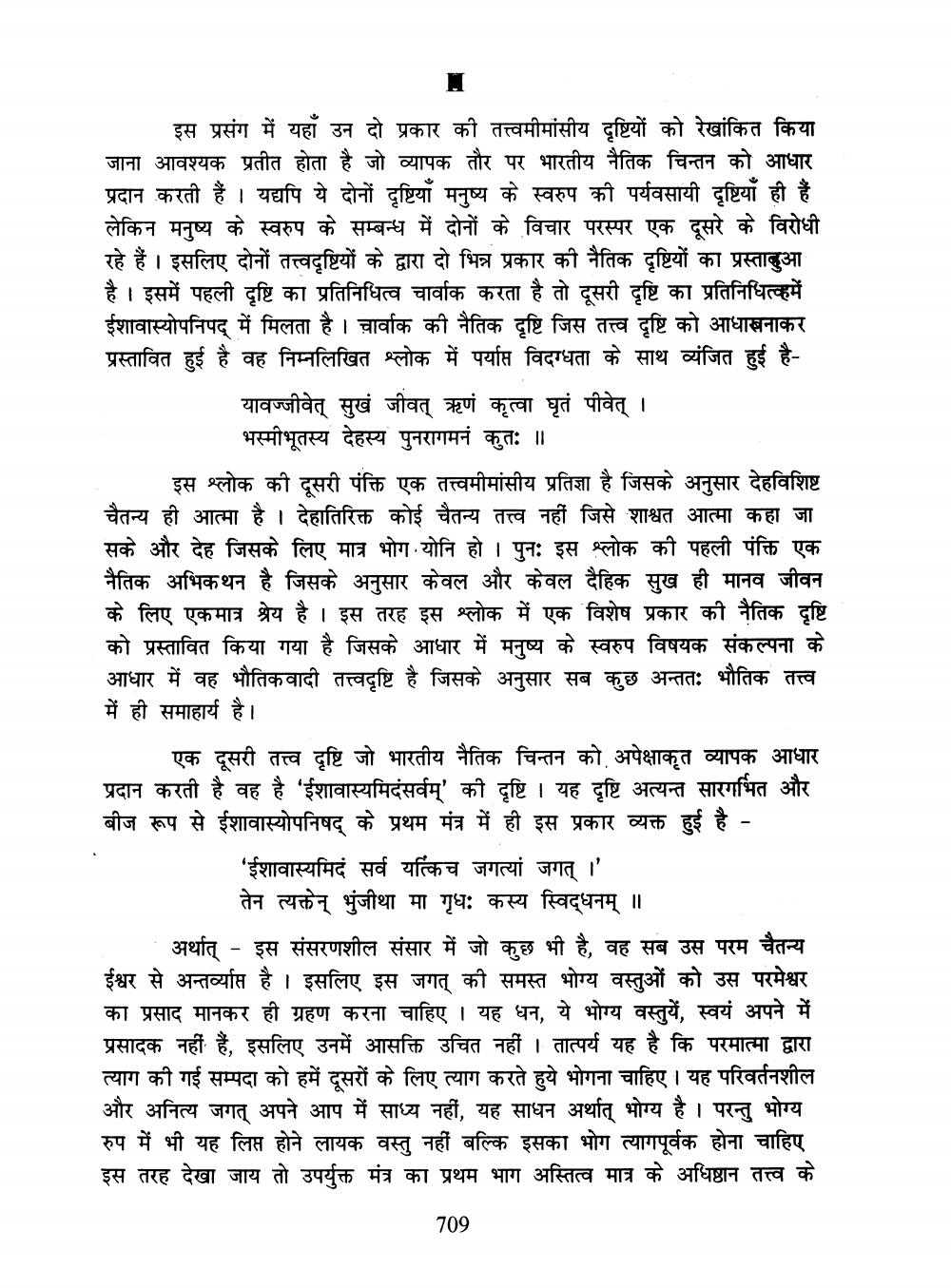________________
इस प्रसंग में यहाँ उन दो प्रकार की तत्त्वमीमांसीय दृष्टियों को रेखांकित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है जो व्यापक तौर पर भारतीय नैतिक चिन्तन को आधार प्रदान करती हैं । यद्यपि ये दोनों दृष्टियाँ मनुष्य के स्वरुप की पर्यवसायी दृष्टियाँ ही हैं लेकिन मनुष्य के स्वरुप के सम्बन्ध में दोनों के विचार परस्पर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं । इसलिए दोनों तत्त्वदृष्टियों के द्वारा दो भिन्न प्रकार की नैतिक दृष्टियों का प्रस्ताबुआ है। इसमें पहली दृष्टि का प्रतिनिधित्व चार्वाक करता है तो दूसरी दृष्टि का प्रतिनिधित्व्हमें ईशावास्योपनिपद् में मिलता है। चार्वाक की नैतिक दृष्टि जिस तत्त्व दृष्टि को आधाखनाकर प्रस्तावित हुई है वह निम्नलिखित श्लोक में पर्याप्त विदग्धता के साथ व्यंजित हुई है
यावज्जीवेत् सुखं जीवत् ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ इस श्लोक की दूसरी पंक्ति एक तत्त्वमीमांसीय प्रतिज्ञा है जिसके अनुसार देहविशिष्ट चैतन्य ही आत्मा है । देहातिरिक्त कोई चैतन्य तत्त्व नहीं जिसे शाश्वत आत्मा कहा जा सके और देह जिसके लिए मात्र भोग योनि हो । पुनः इस श्लोक की पहली पंक्ति एक नैतिक अभिकथन है जिसके अनुसार केवल और केवल दैहिक सुख ही मानव जीवन के लिए एकमात्र श्रेय है । इस तरह इस श्लोक में एक विशेष प्रकार की नैतिक दृष्टि को प्रस्तावित किया गया है जिसके आधार में मनुष्य के स्वरुप विषयक संकल्पना के आधार में वह भौतिकवादी तत्त्वदृष्टि है जिसके अनुसार सब कुछ अन्ततः भौतिक तत्त्व में ही समाहार्य है।
एक दूसरी तत्त्व दृष्टि जो भारतीय नैतिक चिन्तन को अपेक्षाकृत व्यापक आधार प्रदान करती है वह है 'ईशावास्यमिदंसर्वम्' की दृष्टि । यह दृष्टि अत्यन्त सारगर्भित और बीज रूप से ईशावास्योपनिषद् के प्रथम मंत्र में ही इस प्रकार व्यक्त हुई है -
'ईशावास्यमिदं सर्व यत्किच जगत्यां जगत् ।' ।
तेन त्यक्तेन् भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥ अर्थात् - इस संसरणशील संसार में जो कुछ भी है, वह सब उस परम चैतन्य ईश्वर से अन्तर्व्याप्त है। इसलिए इस जगत् की समस्त भोग्य वस्तुओं को उस परमेश्वर का प्रसाद मानकर ही ग्रहण करना चाहिए । यह धन, ये भोग्य वस्तुयें, स्वयं अपने में प्रसादक नहीं हैं, इसलिए उनमें आसक्ति उचित नहीं । तात्पर्य यह है कि परमात्मा द्वारा त्याग की गई सम्पदा को हमें दूसरों के लिए त्याग करते हुये भोगना चाहिए । यह परिवर्तनशील
और अनित्य जगत् अपने आप में साध्य नहीं, यह साधन अर्थात् भोग्य है । परन्तु भोग्य रुप में भी यह लिप्त होने लायक वस्तु नहीं बल्कि इसका भोग त्यागपूर्वक होना चाहिए इस तरह देखा जाय तो उपर्युक्त मंत्र का प्रथम भाग अस्तित्व मात्र के अधिष्ठान तत्त्व के
709