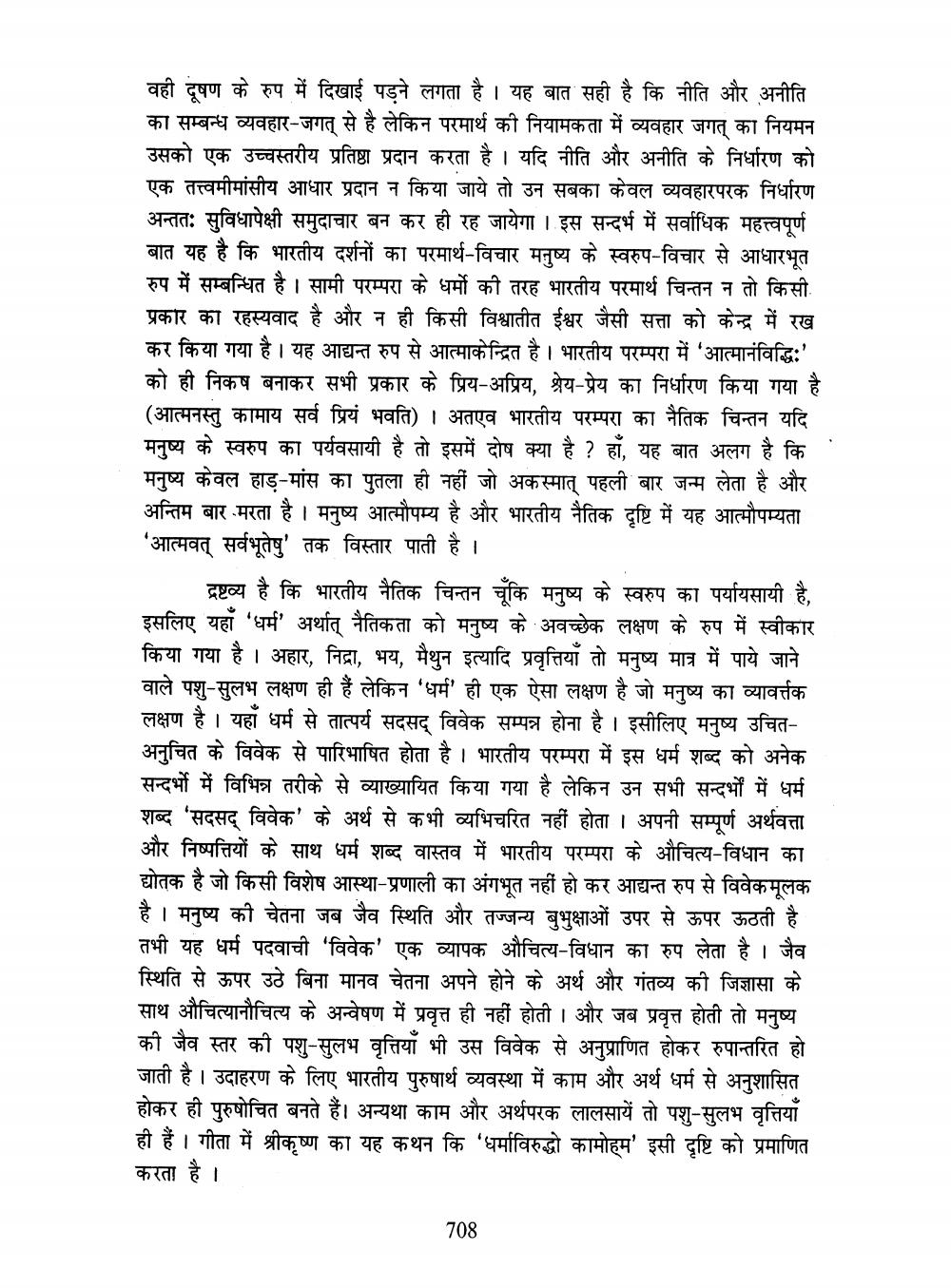________________
वही दूषण के रुप में दिखाई पड़ने लगता है । यह बात सही है कि नीति और अनीति का सम्बन्ध व्यवहार-जगत् से है लेकिन परमार्थ की नियामकता में व्यवहार जगत् का नियमन उसको एक उच्चस्तरीय प्रतिष्ठा प्रदान करता है । यदि नीति और अनीति के निर्धारण को एक तत्त्वमीमांसीय आधार प्रदान न किया जाये तो उन सबका केवल व्यवहारपरक निर्धारण अन्ततः सुविधापेक्षी समुदाचार बन कर ही रह जायेगा । इस सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय दर्शनों का परमार्थ-विचार मनुष्य के स्वरुप-विचार से आधारभूत रुप में सम्बन्धित है । सामी परम्परा के धर्मो की तरह भारतीय परमार्थ चिन्तन न तो किसी प्रकार का रहस्यवाद है और न ही किसी विश्वातीत ईश्वर जैसी सत्ता को केन्द्र में रख कर किया गया है। यह आद्यन्त रुप से आत्माकेन्द्रित है । भारतीय परम्परा में 'आत्मानंविद्धिः' को ही निकष बनाकर सभी प्रकार के प्रिय-अप्रिय, श्रेय-प्रेय का निर्धारण किया गया है (आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति) । अतएव भारतीय परम्परा का नैतिक चिन्तन यदि मनुष्य के स्वरुप का पर्यवसायी है तो इसमें दोष क्या है ? हाँ, यह बात अलग है कि मनुष्य केवल हाड़-मांस का पुतला ही नहीं जो अकस्मात् पहली बार जन्म लेता है और अन्तिम बार मरता है । मनुष्य आत्मौपम्य है और भारतीय नैतिक दृष्टि में यह आत्मौपम्यता 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' तक विस्तार पाती है ।
द्रष्टव्य है कि भारतीय नैतिक चिन्तन चूँकि मनुष्य के स्वरुप का पर्यायसायी है, इसलिए यहाँ 'धर्म' अर्थात् नैतिकता को मनुष्य के अवच्छेक लक्षण के रुप में स्वीकार किया गया है । अहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि प्रवृत्तिया तो मनुष्य मात्र में पाये जाने वाले पशु-सुलभ लक्षण ही हैं लेकिन 'धर्म' ही एक ऐसा लक्षण है जो मनुष्य का व्यावर्तक लक्षण है । यहा धर्म से तात्पर्य सदसद् विवेक सम्पन्न होना है। इसीलिए मनुष्य उचितअनुचित के विवेक से पारिभाषित होता है । भारतीय परम्परा में इस धर्म शब्द को अनेक सन्दर्भो में विभिन्न तरीके से व्याख्यायित किया गया है लेकिन उन सभी सन्दर्भो में धर्म शब्द 'सदसद् विवेक' के अर्थ से कभी व्यभिचरित नहीं होता । अपनी सम्पूर्ण अर्थवत्ता और निष्पत्तियों के साथ धर्म शब्द वास्तव में भारतीय परम्परा के औचित्य-विधान का द्योतक है जो किसी विशेष आस्था-प्रणाली का अंगभूत नहीं हो कर आद्यन्त रुप से विवेकमूलक है । मनुष्य की चेतना जब जैव स्थिति और तज्जन्य बुभुक्षाओं उपर से ऊपर ऊठती है तभी यह धर्म पदवाची 'विवेक' एक व्यापक औचित्य-विधान का रुप लेता है । जैव स्थिति से ऊपर उठे बिना मानव चेतना अपने होने के अर्थ और गंतव्य की जिज्ञासा के साथ औचित्यानौचित्य के अन्वेषण में प्रवृत्त ही नहीं होती । और जब प्रवृत्त होती तो मनुष्य की जैव स्तर की पशु-सुलभ वृत्तियाँ भी उस विवेक से अनुप्राणित होकर रुपान्तरित हो जाती है। उदाहरण के लिए भारतीय पुरुषार्थ व्यवस्था में काम और अर्थ धर्म से अनुशासित होकर ही पुरुषोचित बनते हैं। अन्यथा काम और अर्थपरक लालसायें तो पशु-सुलभ वृत्तियाँ ही हैं । गीता में श्रीकृष्ण का यह कथन कि 'धर्माविरुद्धो कामोम' इसी दृष्टि को प्रमाणित करता है।
708