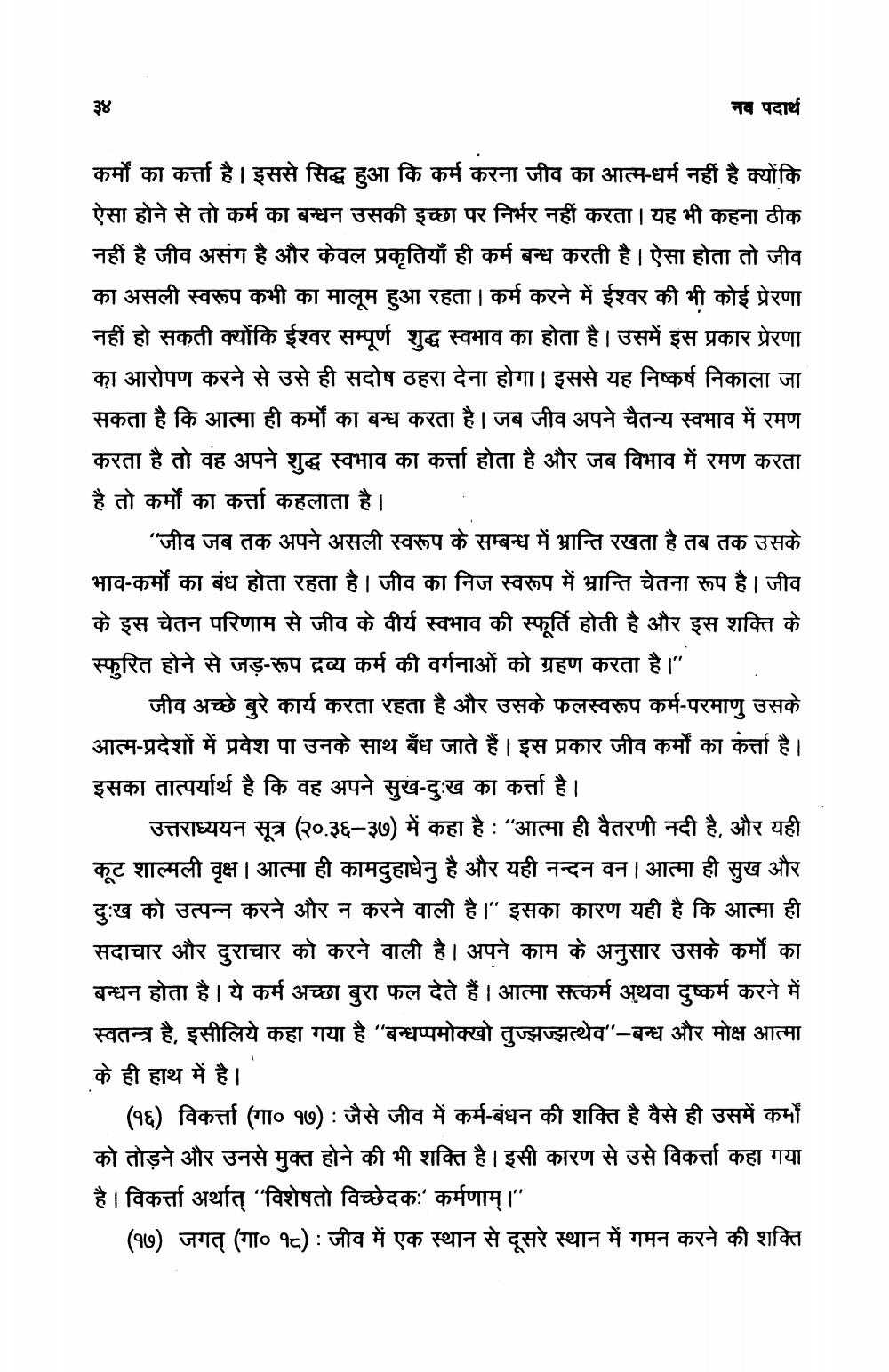________________
३४
नव पदार्थ
कर्मों का कर्त्ता है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म करना जीव का आत्म-धर्म नहीं है क्योंकि ऐसा होने से तो कर्म का बन्धन उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता । यह भी कहना ठीक नहीं है जीव असंग है और केवल प्रकृतियाँ ही कर्म बन्ध करती है। ऐसा होता तो जीव का असली स्वरूप कभी का मालूम हुआ रहता । कर्म करने में ईश्वर की भी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर सम्पूर्ण शुद्ध स्वभाव का होता है। उसमें इस प्रकार प्रेरणा का आरोपण करने से उसे ही सदोष ठहरा देना होगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आत्मा ही कर्मों का बन्ध करता है। जब जीव अपने चैतन्य स्वभाव में रमण करता है तो वह अपने शुद्ध स्वभाव का कर्त्ता होता है और जब विभाव में रमण करता है तो कर्मों का कर्त्ता कहलाता है ।
"जीव जब तक अपने असली स्वरूप के सम्बन्ध में भ्रान्ति रखता है तब तक उसके भाव-कर्मों का बंध होता रहता है। जीव का निज स्वरूप में भ्रान्ति चेतना रूप है । जीव के इस चेतन परिणाम से जीव के वीर्य स्वभाव की स्फूर्ति होती है और इस शक्ति के स्फुरित होने से जड़ - रूप द्रव्य कर्म की वर्गनाओं को ग्रहण करता है।"
जीव अच्छे बुरे कार्य करता रहता है और उसके फलस्वरूप कर्म-परमाणु उसके आत्म-प्रदेशों में प्रवेश पा उनके साथ बँध जाते हैं। इस प्रकार जीव कर्मों का कर्त्ता है। इसका तात्पर्यार्थ है कि वह अपने सुख-दुःख का कर्त्ता है ।
उत्तराध्ययन सूत्र (२०.३६-३७) कहा है : "आत्मा ही वैतरणी नदी है, और यही कूट शाल्मली वृक्ष | आत्मा ही कामदुहाधेनु है और यही नन्दन वन । आत्मा ही सुख और दुःख को उत्पन्न करने और न करने वाली है।" इसका कारण यही है कि आत्मा ही सदाचार और दुराचार को करने वाली है। अपने काम के अनुसार उसके कर्मों का बन्धन होता है। ये कर्म अच्छा बुरा फल देते हैं। आत्मा सत्कर्म अथवा दुष्कर्म करने में स्वतन्त्र है, इसीलिये कहा गया है "बन्धप्पमोक्खो तुज्झज्झत्थेव " - बन्ध और मोक्ष आत्मा के ही हाथ में है ।
1
(१६) विकर्त्ता ( गा० १७ ) : जैसे जीव में कर्म-बंधन की शक्ति है वैसे ही उसमें कर्मों को तोड़ने और उनसे मुक्त होने की भी शक्ति है। इसी कारण से उसे विकर्त्ता कहा गया है । विकर्त्ता अर्थात् "विशेषतो विच्छेदकः' कर्मणाम् ।"
(१७) जगत् ( गा० १८ ) : जीव में एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने की शक्ति