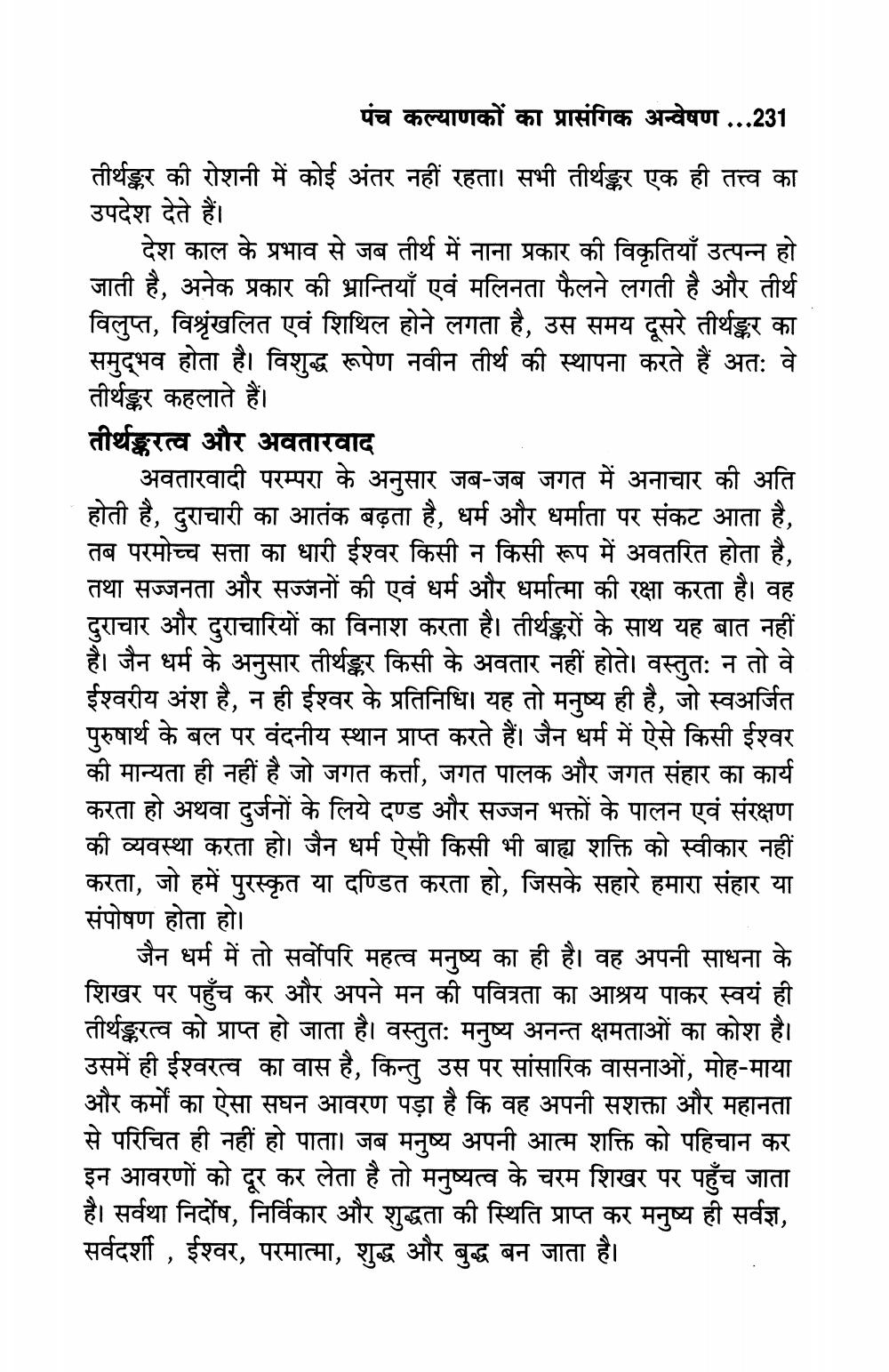________________
पंच कल्याणकों का प्रासंगिक अन्वेषण ... 231 तीर्थङ्कर की रोशनी में कोई अंतर नहीं रहता। सभी तीर्थङ्कर एक ही तत्त्व का उपदेश देते हैं।
देश काल के प्रभाव से जब तीर्थ में नाना प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ एवं मलिनता फैलने लगती है और तीर्थ विलुप्त, विश्रृंखलित एवं शिथिल होने लगता है, उस समय दूसरे तीर्थङ्कर का समुद्भव होता है। विशुद्ध रूपेण नवीन तीर्थ की स्थापना करते हैं अतः वे तीर्थङ्कर कहलाते हैं।
तीर्थङ्करत्व और अवतारवाद
अवतारवादी परम्परा के अनुसार जब-जब जगत में अनाचार की अति होती है, दुराचारी का आतंक बढ़ता है, धर्म और धर्माता पर संकट आता है, तब परमोच्च सत्ता का धारी ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होता है, तथा सज्जनता और सज्जनों की एवं धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करता है। वह दुराचार और दुराचारियों का विनाश करता है। तीर्थङ्करों के साथ यह बात नहीं है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थङ्कर किसी के अवतार नहीं होते । वस्तुतः न तो वे ईश्वरीय अंश है, न ही ईश्वर के प्रतिनिधि । यह तो मनुष्य ही है, जो स्वअर्जित पुरुषार्थ के बल पर वंदनीय स्थान प्राप्त करते हैं। जैन धर्म में ऐसे किसी ईश्वर की मान्यता ही नहीं है जो जगत कर्त्ता, जगत पालक और जगत संहार का कार्य करता हो अथवा दुर्जनों के लिये दण्ड और सज्जन भक्तों के पालन एवं संरक्षण की व्यवस्था करता हो । जैन धर्म ऐसी किसी भी बाह्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता, जो हमें पुरस्कृत या दण्डित करता हो, जिसके सहारे हमारा संहार या संपोषण होता हो।
जैन धर्म में तो सर्वोपरि महत्व मनुष्य का ही है । वह अपनी साधना के शिखर पर पहुँच कर और अपने मन की पवित्रता का आश्रय पाकर स्वयं ही तीर्थङ्करत्व को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः मनुष्य अनन्त क्षमताओं का कोश है। उसमें ही ईश्वरत्व का वास है, किन्तु उस पर सांसारिक वासनाओं, मोह-माया और कर्मों का ऐसा सघन आवरण पड़ा है कि वह अपनी सशक्ता और महानता से परिचित ही नहीं हो पाता। जब मनुष्य अपनी आत्म शक्ति को पहिचान कर इन आवरणों को दूर कर लेता है तो मनुष्यत्व के चरम शिखर पर पहुँच जाता है। सर्वथा निर्दोष, निर्विकार और शुद्धता की स्थिति प्राप्त कर मनुष्य ही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, ईश्वर, परमात्मा, शुद्ध और बुद्ध बन जाता है।