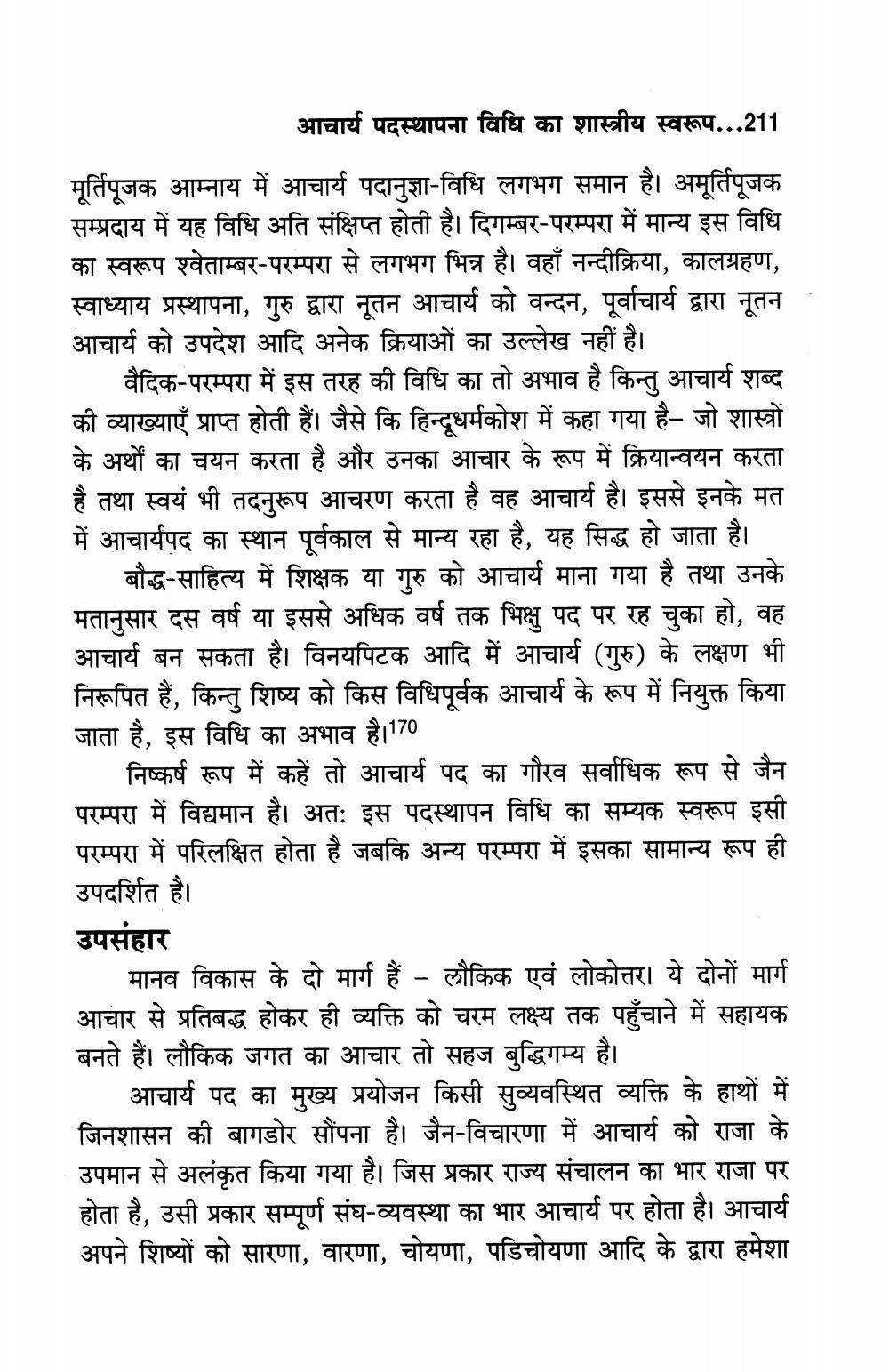________________
आचार्य पदस्थापना विधि का शास्त्रीय स्वरूप...211
मूर्तिपूजक आम्नाय में आचार्य पदानुज्ञा-विधि लगभग समान है। अमूर्तिपूजक सम्प्रदाय में यह विधि अति संक्षिप्त होती है। दिगम्बर-परम्परा में मान्य इस विधि का स्वरूप श्वेताम्बर-परम्परा से लगभग भिन्न है। वहाँ नन्दीक्रिया, कालग्रहण, स्वाध्याय प्रस्थापना, गुरु द्वारा नूतन आचार्य को वन्दन, पूर्वाचार्य द्वारा नूतन आचार्य को उपदेश आदि अनेक क्रियाओं का उल्लेख नहीं है। __ वैदिक-परम्परा में इस तरह की विधि का तो अभाव है किन्तु आचार्य शब्द की व्याख्याएँ प्राप्त होती हैं। जैसे कि हिन्दूधर्मकोश में कहा गया है- जो शास्त्रों के अर्थों का चयन करता है और उनका आचार के रूप में क्रियान्वयन करता है तथा स्वयं भी तदनुरूप आचरण करता है वह आचार्य है। इससे इनके मत में आचार्यपद का स्थान पूर्वकाल से मान्य रहा है, यह सिद्ध हो जाता है।
बौद्ध-साहित्य में शिक्षक या गुरु को आचार्य माना गया है तथा उनके मतानुसार दस वर्ष या इससे अधिक वर्ष तक भिक्षु पद पर रह चुका हो, वह आचार्य बन सकता है। विनयपिटक आदि में आचार्य (गुरु) के लक्षण भी निरूपित हैं, किन्तु शिष्य को किस विधिपूर्वक आचार्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, इस विधि का अभाव है।170
निष्कर्ष रूप में कहें तो आचार्य पद का गौरव सर्वाधिक रूप से जैन परम्परा में विद्यमान है। अत: इस पदस्थापन विधि का सम्यक स्वरूप इसी परम्परा में परिलक्षित होता है जबकि अन्य परम्परा में इसका सामान्य रूप ही उपदर्शित है। उपसंहार
मानव विकास के दो मार्ग हैं - लौकिक एवं लोकोत्तर। ये दोनों मार्ग आचार से प्रतिबद्ध होकर ही व्यक्ति को चरम लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक बनते हैं। लौकिक जगत का आचार तो सहज बुद्धिगम्य है।
आचार्य पद का मुख्य प्रयोजन किसी सुव्यवस्थित व्यक्ति के हाथों में जिनशासन की बागडोर सौंपना है। जैन-विचारणा में आचार्य को राजा के उपमान से अलंकृत किया गया है। जिस प्रकार राज्य संचालन का भार राजा पर होता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण संघ-व्यवस्था का भार आचार्य पर होता है। आचार्य अपने शिष्यों को सारणा, वारणा, चोयणा, पडिचोयणा आदि के द्वारा हमेशा