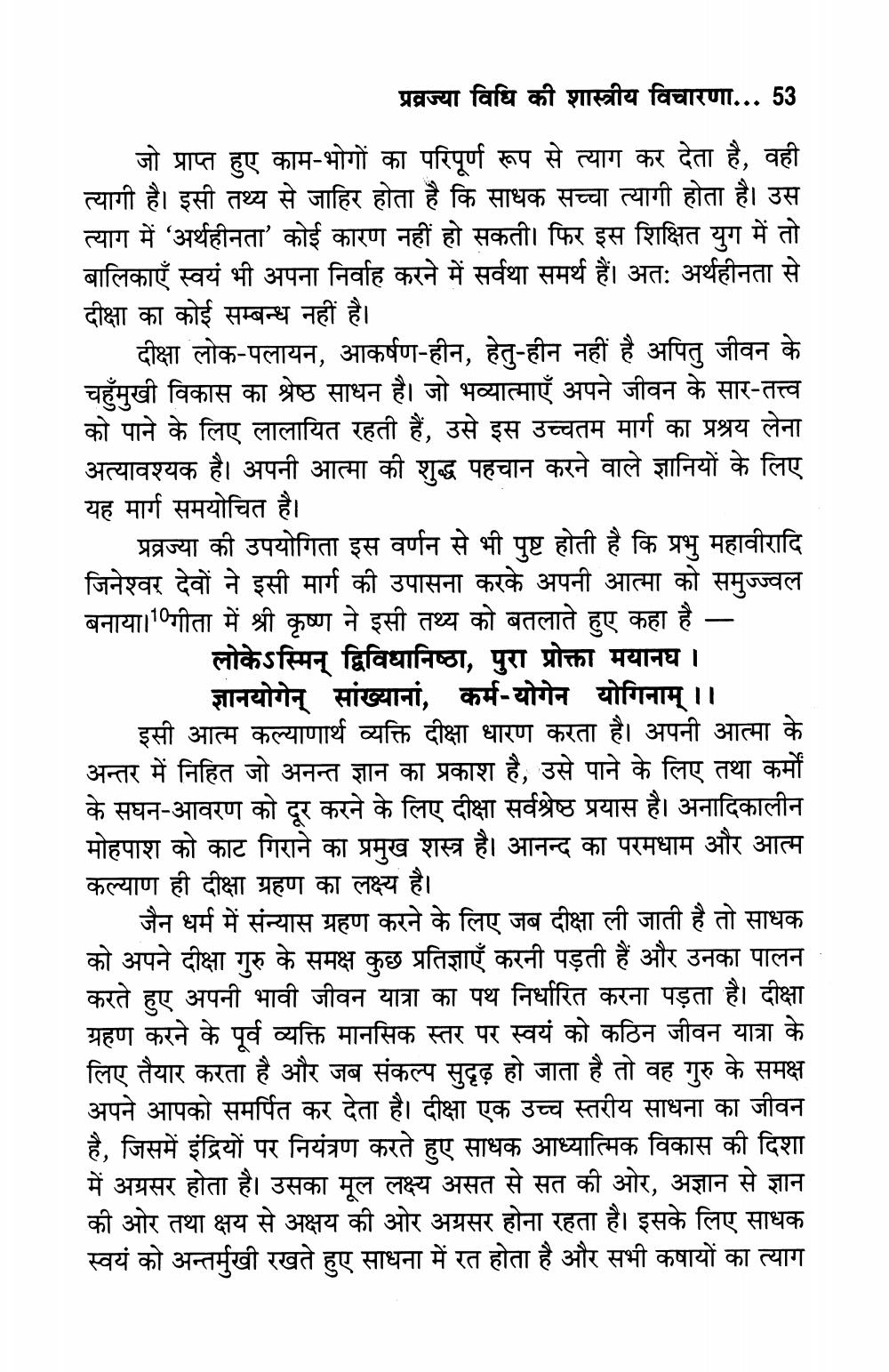________________
प्रव्रज्या विधि की शास्त्रीय विचारणा... 53
जो प्राप्त हुए काम-भोगों का परिपूर्ण रूप से त्याग कर देता है, वही त्यागी है। इसी तथ्य से जाहिर होता है कि साधक सच्चा त्यागी होता है। उस त्याग में 'अर्थहीनता' कोई कारण नहीं हो सकती। फिर इस शिक्षित युग में तो बालिकाएँ स्वयं भी अपना निर्वाह करने में सर्वथा समर्थ हैं। अत: अर्थहीनता से दीक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है।
दीक्षा लोक-पलायन, आकर्षण-हीन, हेतु-हीन नहीं है अपितु जीवन के चहुंमुखी विकास का श्रेष्ठ साधन है। जो भव्यात्माएँ अपने जीवन के सार-तत्त्व को पाने के लिए लालायित रहती हैं, उसे इस उच्चतम मार्ग का प्रश्रय लेना अत्यावश्यक है। अपनी आत्मा की शुद्ध पहचान करने वाले ज्ञानियों के लिए यह मार्ग समयोचित है।
प्रव्रज्या की उपयोगिता इस वर्णन से भी पुष्ट होती है कि प्रभु महावीरादि जिनेश्वर देवों ने इसी मार्ग की उपासना करके अपनी आत्मा को समुज्ज्वल बनाया। गीता में श्री कृष्ण ने इसी तथ्य को बतलाते हुए कहा है -
लोकेऽस्मिन् द्विविधानिष्ठा, पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन् सांख्यानां, कर्म-योगेन योगिनाम् ।। इसी आत्म कल्याणार्थ व्यक्ति दीक्षा धारण करता है। अपनी आत्मा के अन्तर में निहित जो अनन्त ज्ञान का प्रकाश है, उसे पाने के लिए तथा कर्मों के सघन-आवरण को दूर करने के लिए दीक्षा सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। अनादिकालीन मोहपाश को काट गिराने का प्रमुख शस्त्र है। आनन्द का परमधाम और आत्म कल्याण ही दीक्षा ग्रहण का लक्ष्य है।
जैन धर्म में संन्यास ग्रहण करने के लिए जब दीक्षा ली जाती है तो साधक को अपने दीक्षा गुरु के समक्ष कुछ प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ती हैं और उनका पालन करते हुए अपनी भावी जीवन यात्रा का पथ निर्धारित करना पड़ता है। दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व व्यक्ति मानसिक स्तर पर स्वयं को कठिन जीवन यात्रा के लिए तैयार करता है और जब संकल्प सुदृढ़ हो जाता है तो वह गुरु के समक्ष अपने आपको समर्पित कर देता है। दीक्षा एक उच्च स्तरीय साधना का जीवन है, जिसमें इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए साधक आध्यात्मिक विकास की दिशा में अग्रसर होता है। उसका मूल लक्ष्य असत से सत की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा क्षय से अक्षय की ओर अग्रसर होना रहता है। इसके लिए साधक स्वयं को अन्तर्मुखी रखते हुए साधना में रत होता है और सभी कषायों का त्याग