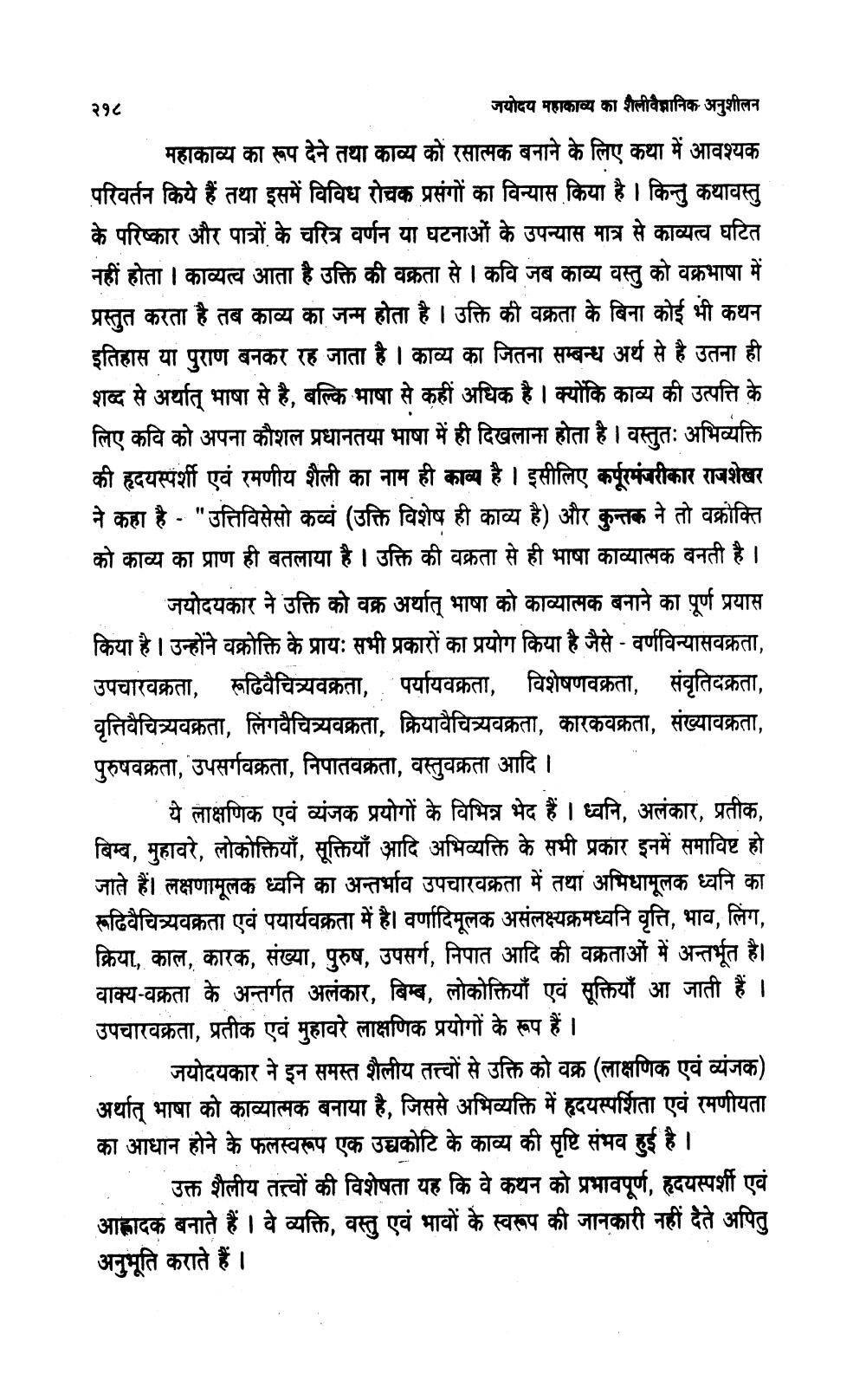________________
२१८
जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ___महाकाव्य का रूप देने तथा काव्य को रसात्मक बनाने के लिए कथा में आवश्यक परिवर्तन किये हैं तथा इसमें विविध रोचक प्रसंगों का विन्यास किया है । किन्तु कथावस्तु के परिष्कार और पात्रों के चरित्र वर्णन या घटनाओं के उपन्यास मात्र से काव्यत्व घटित नहीं होता । काव्यत्व आता है उक्ति की वक्रता से । कवि जब काव्य वस्तु को वक्रभाषा में प्रस्तुत करता है तब काव्य का जन्म होता है । उक्ति की वक्रता के बिना कोई भी कथन इतिहास या पुराण बनकर रह जाता है । काव्य का जितना सम्बन्ध अर्थ से है उतना ही शब्द से अर्थात् भाषा से है, बल्कि भाषा से कहीं अधिक है। क्योंकि काव्य की उत्पत्ति के लिए कवि को अपना कौशल प्रधानतया भाषा में ही दिखलाना होता है । वस्तुतः अभिव्यक्ति की हृदयस्पर्शी एवं रमणीय शैली का नाम ही काव्य है । इसीलिए कर्पूरमंजरीकार राजशेखर ने कहा है - "उत्तिविसेसो कव्वं (उक्ति विशेष ही काव्य है) और कुन्तक ने तो वक्रोक्ति को काव्य का प्राण ही बतलाया है । उक्ति की वक्रता से ही भाषा काव्यात्मक बनती है |
जयोदयकार ने उक्ति को वक्र अर्थात् भाषा को काव्यात्मक बनाने का पूर्ण प्रयास किया है । उन्होंने वक्रोक्ति के प्रायः सभी प्रकारों का प्रयोग किया है जैसे - वर्णविन्यासवक्रता, उपचारवक्रता, रूढिवैचित्र्यवक्रता, पर्यायवक्रता, विशेषणवक्रता, संवृतिवक्रता, वृत्तिवैचित्र्यवक्रता, लिंगवैचित्र्यवक्रता, क्रियावैचित्र्यवक्रता, कारकवक्रता, संख्यावक्रता, पुरुषवक्रता, उपसर्गवक्रता, निपातवक्रता, वस्तुवक्रता आदि ।
ये लाक्षणिक एवं व्यंजक प्रयोगों के विभिन्न भेद हैं । ध्वनि, अलंकार, प्रतीक, बिम्ब, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ आदि अभिव्यक्ति के सभी प्रकार इनमें समाविष्ट हो जाते हैं। लक्षणामूलक ध्वनि का अन्तर्भाव उपचारवक्रता में तथा अभिधामूलक ध्वनि का रूढिवैचित्र्यवक्रता एवं पयार्यवक्रता में है। वर्णादिमूलक असंलक्ष्यक्रमध्वनि वृत्ति, भाव, लिंग, क्रिया, काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपसर्ग, निपात आदि की वक्रताओं में अन्तर्भूत है। वाक्य-वक्रता के अन्तर्गत अलंकार, बिम्ब, लोकोक्तियाँ एवं सूक्तियाँ आ जाती हैं । उपचारवक्रता, प्रतीक एवं मुहावरे लाक्षणिक प्रयोगों के रूप हैं।
जयोदयकार ने इन समस्त शैलीय तत्त्वों से उक्ति को वक्र (लाक्षणिक एवं व्यंजक) अर्थात् भाषा को काव्यात्मक बनाया है, जिससे अभिव्यक्ति में हृदयस्पर्शिता एवं रमणीयता का आधान होने के फलस्वरूप एक उच्चकोटि के काव्य की सृष्टि संभव हुई है । . उक्त शैलीय तत्त्वों की विशेषता यह कि वे कथन को प्रभावपूर्ण, हृदयस्पर्शी एवं आह्लादक बनाते हैं । वे व्यक्ति, वस्तु एवं भावों के स्वरूप की जानकारी नहीं देते अपितु अनुभूति कराते हैं।