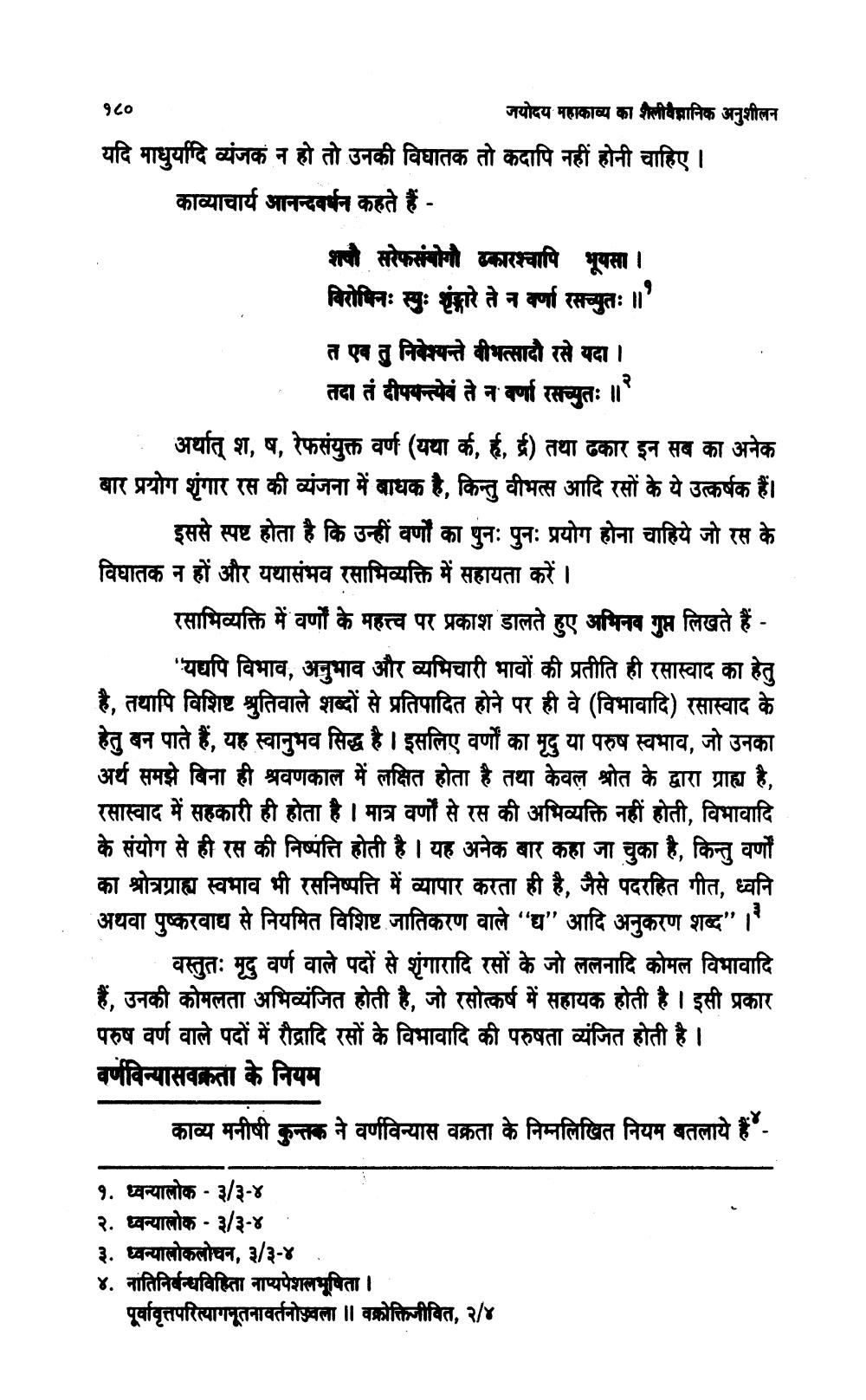________________
१८०
जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन यदि माधुर्यादि व्यंजक न हो तो उनकी विघातक तो कदापि नहीं होनी चाहिए । काव्याचार्य आनन्दवर्षन कहते हैं -
शवो सरेफसंयोगी डकारश्चापि भूयसा । विरोधिनः स्युः शृंगारे ते न वर्णा रसच्युतः ॥' त एव तु निवेश्यन्ते वीभत्सादौ रसे यदा ।
तदा तं दीपपन्त्येवं ते न वर्णा रसच्युतः ॥२ . अर्थात् श, ष, रेफसंयुक्त वर्ण (यथा र्क, ह, द्र) तथा ढकार इन सब का अनेक बार प्रयोग शृंगार रस की व्यंजना में बाधक है, किन्तु वीभत्स आदि रसों के ये उत्कर्षक हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि उन्हीं वों का पुनः पुनः प्रयोग होना चाहिये जो रस के विघातक न हों और यथासंभव रसाभिव्यक्ति में सहायता करें ।
रसाभिव्यक्ति में वर्गों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए अभिनव गुप्त लिखते हैं -
"यद्यपि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों की प्रतीति ही रसास्वाद का हेतु है, तथापि विशिष्ट श्रुतिवाले शब्दों से प्रतिपादित होने पर ही वे (विभावादि) रसास्वाद के हेतु बन पाते हैं, यह स्वानुभव सिद्ध है। इसलिए वर्णों का मृदु या परुष स्वभाव, जो उनका अर्थ समझे बिना ही श्रवणकाल में लक्षित होता है तथा केवल श्रोत के द्वारा ग्राह्य है, रसास्वाद में सहकारी ही होता है । मात्र वर्णों से रस की अभिव्यक्ति नहीं होती, विभावादि के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है । यह अनेक बार कहा जा चुका है, किन्तु वर्णों का श्रोत्रग्राह्य स्वभाव भी रसनिष्पत्ति में व्यापार करता ही है, जैसे पदरहित गीत, ध्वनि अथवा पुष्करवाध से नियमित विशिष्ट जातिकरण वाले "घ" आदि अनुकरण शब्द" ।'
वस्तुतः मृदु वर्ण वाले पदों से शृंगारादि रसों के जो ललनादि कोमल विभावादि हैं, उनकी कोमलता अभिव्यंजित होती है, जो रसोत्कर्ष में सहायक होती है । इसी प्रकार परुष वर्ण वाले पदों में रौद्रादि रसों के विभावादि की परुषता व्यंजित होती है । वर्णविन्यासवक्रता के नियम
__काव्य मनीषी कुन्तक ने वर्णविन्यास वक्रता के निम्नलिखित नियम बतलाये हैं.
१. ध्वन्यालोक - ३/३-४ २. ध्वन्यालोक - ३/३.४ ३. ध्वन्यालोकलोचन, ३/३-४ ४. नातिनिर्वन्धविहिता नाप्यपेशलभूषिता ।
पूर्वावृत्तपरित्यागनूतनावर्तनोज्वला || वक्रोक्तिजीवित, २/४