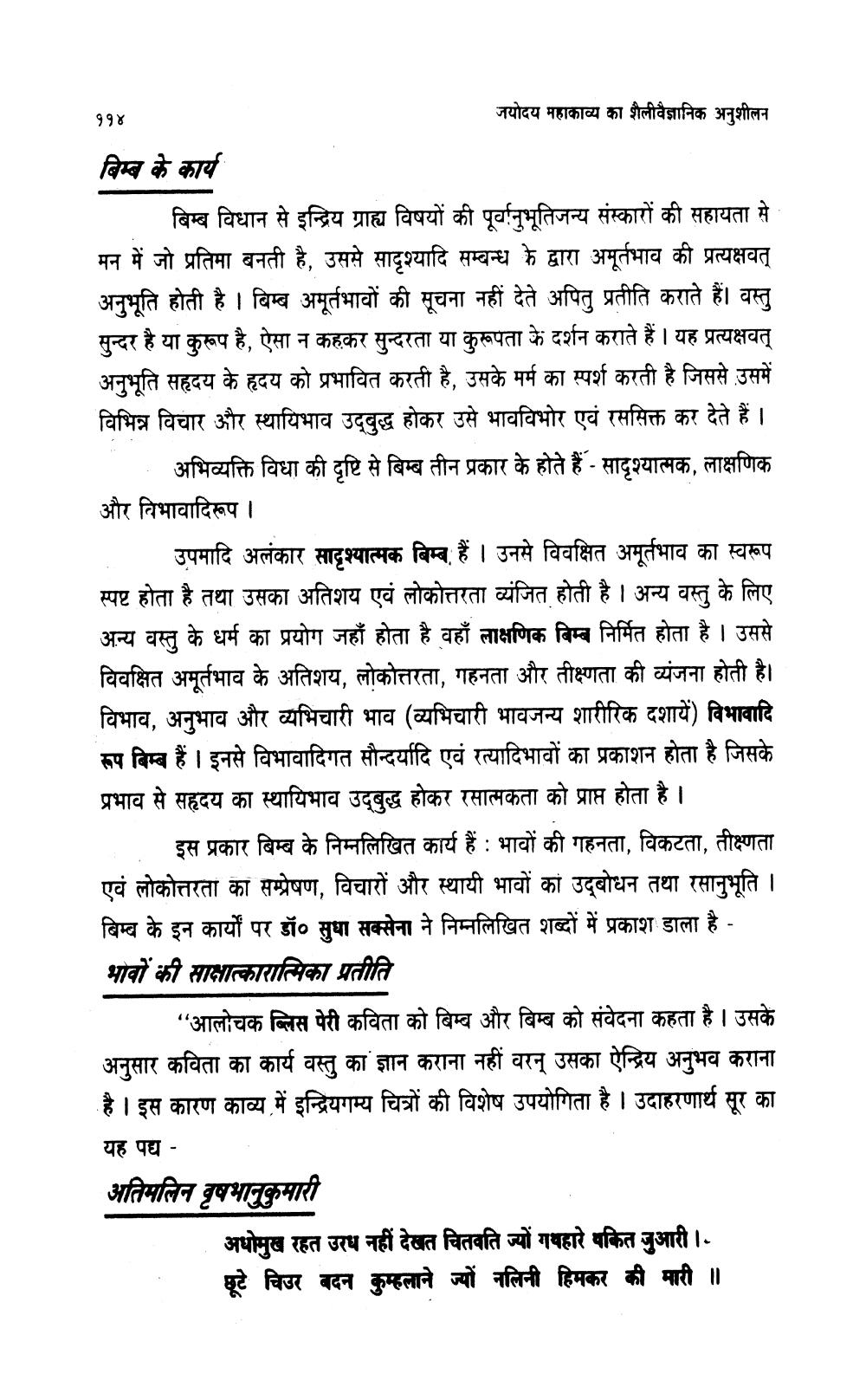________________
११४
बिम्ब के कार्य
बिम्ब विधान से इन्द्रिय ग्राह्य विषयों की पूर्वानुभूतिजन्य संस्कारों की सहायता से मन में जो प्रतिमा बनती है, उससे सादृश्यादि सम्बन्ध के द्वारा अमूर्तभाव की प्रत्यक्षवत् अनुभूति होती है । बिम्ब अमूर्तभावों की सूचना नहीं देते अपितु प्रतीति कराते हैं। वस्तु सुन्दर है या कुरूप है, ऐसा न कहकर सुन्दरता या कुरूपता के दर्शन कराते हैं। यह प्रत्यक्षवत् अनुभूति सहृदय के हृदय को प्रभावित करती है, उसके मर्म का स्पर्श करती है जिससे उसमें विभिन्न विचार और स्थायिभाव उबुद्ध होकर उसे भावविभोर एवं रससिक्त कर देते हैं । अभिव्यक्ति विधा की दृष्टि से बिम्ब तीन प्रकार के होते हैं - सादृश्यात्मक, लाक्षणिक और विभावादिरूप |
जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन
उपमादि अलंकार सादृश्यात्मक बिम्ब हैं। उनसे विवक्षित अमूर्तभाव का स्वरूप स्पष्ट होता है तथा उसका अतिशय एवं लोकोत्तरता व्यंजित होती है। अन्य वस्तु के लिए अन्य वस्तु के धर्म का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ लाक्षणिक बिम्ब निर्मित होता है। उससे विवक्षित अमूर्तभाव के अतिशय, लोकोत्तरता, गहनता और तीक्ष्णता की व्यंजना होती है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ( व्यभिचारी भावजन्य शारीरिक दशायें) विभावादि रूप बिम्ब हैं । इनसे विभावादिगत सौन्दर्यादि एवं रत्यादिभावों का प्रकाशन होता है जिसके प्रभाव से सहृदय का स्थायिभाव उद्बुद्ध होकर रसात्मकता को प्राप्त होता है ।
इस प्रकार बिम्ब के निम्नलिखित कार्य हैं : भावों की गहनता, विकटता, तीक्ष्णता एवं लोकोत्तरता का सम्प्रेषण, विचारों और स्थायी भावों का उद्बोधन तथा रसानुभूति । बिम्ब के इन कार्यों पर डॉ० सुधा सक्सेना ने निम्नलिखित शब्दों में प्रकाश डाला है - भावों की साक्षात्कारात्मिका प्रतीति
"आलोचक ब्लिस पेरी कविता को बिम्ब और बिम्ब को संवेदना कहता है। उसके अनुसार कविता का कार्य वस्तु का ज्ञान कराना नहीं वरन् उसका ऐन्द्रिय अनुभव कराना है। इस कारण काव्य में इन्द्रियगम्य चित्रों की विशेष उपयोगिता है । उदाहरणार्थ सूर का
यह पद्य
अतिमलिन वृषभानुकुमारी
-
अधोमुख रहत उरध नहीं देखत चितवति ज्यों गधहारे थकित जुआरी । -
छूटे चिउर बदन कुम्हलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी ॥