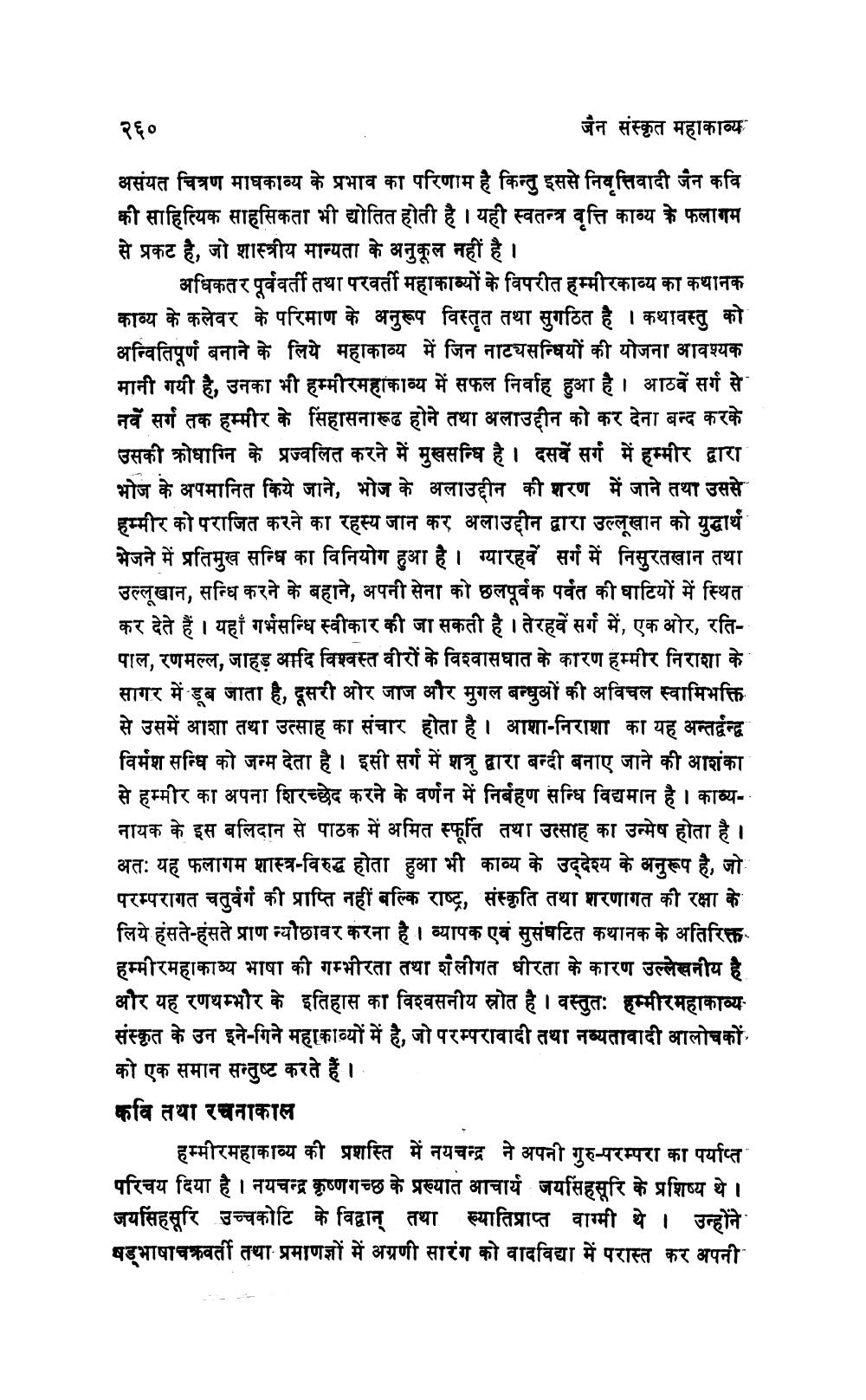________________
२६०
जैन संस्कृत महाकाव्य
असंयत चित्रण माघकाव्य के प्रभाव का परिणाम है किन्तु इससे निवृत्तिवादी जन कवि की साहित्यिक साहसिकता भी धोतित होती है । यही स्वतन्त्र वृत्ति काव्य के फलागम से प्रकट है, जो शास्त्रीय मान्यता के अनुकूल नहीं है।
अधिकतर पूर्ववर्ती तथा परवर्ती महाकाव्यों के विपरीत हम्मीरकाव्य का कथानक काव्य के कलेवर के परिमाण के अनुरूप विस्तृत तथा सुगठित है । कथावस्तु को अन्वितिपूर्ण बनाने के लिये महाकाव्य में जिन नाटयसन्धियों की योजना आवश्यक मानी गयी है, उनका भी हम्मीरमहाकाव्य में सफल निर्वाह हुआ है। आठवें सर्ग से नवे सर्ग तक हम्मीर के सिंहासनारूढ होने तथा अलाउद्दीन को कर देना बन्द करके उसकी क्रोधाग्नि के प्रज्वलित करने में मुखसन्धि है। दसवें सर्ग में हम्मीर द्वारा भोज के अपमानित किये जाने, भोज के अलाउद्दीन की शरण में जाने तथा उससे हम्मीर को पराजित करने का रहस्य जान कर अलाउद्दीन द्वारा उल्लूखान को युद्धार्थ भेजने में प्रतिमुख सन्धि का विनियोग हुआ है। ग्यारहवें सर्ग में निसुरतखान तथा उल्लूखान, सन्धि करने के बहाने, अपनी सेना को छलपूर्वक पर्वत की घाटियों में स्थित कर देते हैं । यहाँ गर्भसन्धि स्वीकार की जा सकती है । तेरहवें सर्ग में, एक ओर, रतिपाल, रणमल्ल, जाहड़ आदि विश्वस्त वीरों के विश्वासघात के कारण हम्मीर निराशा के सागर में डूब जाता है, दूसरी ओर जाज और मुगल बन्धुओं की अविचल स्वामिभक्ति से उसमें आशा तथा उत्साह का संचार होता है। आशा-निराशा का यह अन्तर्द्वन्द्व विर्मश सन्धि को जन्म देता है। इसी सर्ग में शत्रु द्वारा बन्दी बनाए जाने की आशंका से हम्मीर का अपना शिरच्छेद करने के वर्णन में निर्बहण सन्धि विद्यमान है । काव्यनायक के इस बलिदान से पाठक में अमित स्फूर्ति तथा उत्साह का उन्मेष होता है। अतः यह फलागम शास्त्र-विरुद्ध होता हुआ भी काव्य के उद्देश्य के अनुरूप है, जो परम्परागत चतुर्वर्ग की प्राप्ति नहीं बल्कि राष्ट्र, संस्कृति तथा शरणागत की रक्षा के लिये हंसते-हंसते प्राण न्योछावर करना है । व्यापक एवं सुसंघटित कथानक के अतिरिक्त हम्मीरमहाकाव्य भाषा की गम्भीरता तथा शैलीगत धीरता के कारण उल्लेखनीय है और यह रणथम्भौर के इतिहास का विश्वसनीय स्रोत है । वस्तुतः हम्मीरमहाकाव्य संस्कृत के उन इने-गिने महाकाव्यों में है, जो परम्परावादी तथा नव्यतावादी आलोचकों को एक समान सन्तुष्ट करते हैं। कवि तथा रचनाकाल
____ हम्मीरमहाकाव्य की प्रशस्ति में नयचन्द्र ने अपनी गुरु-परम्परा का पर्याप्त परिचय दिया है । नयचन्द्र कृष्णगच्छ के प्रख्यात आचार्य जयसिंहसूरि के प्रशिष्य थे। जयसिंहसूरि उच्चकोटि के विद्वान् तथा ख्यातिप्राप्त वाग्मी थे । उन्होंने षड्भाषाचक्रवर्ती तथा प्रमाणज्ञों में अग्रणी सारंग को वादविद्या में परास्त कर अपनी