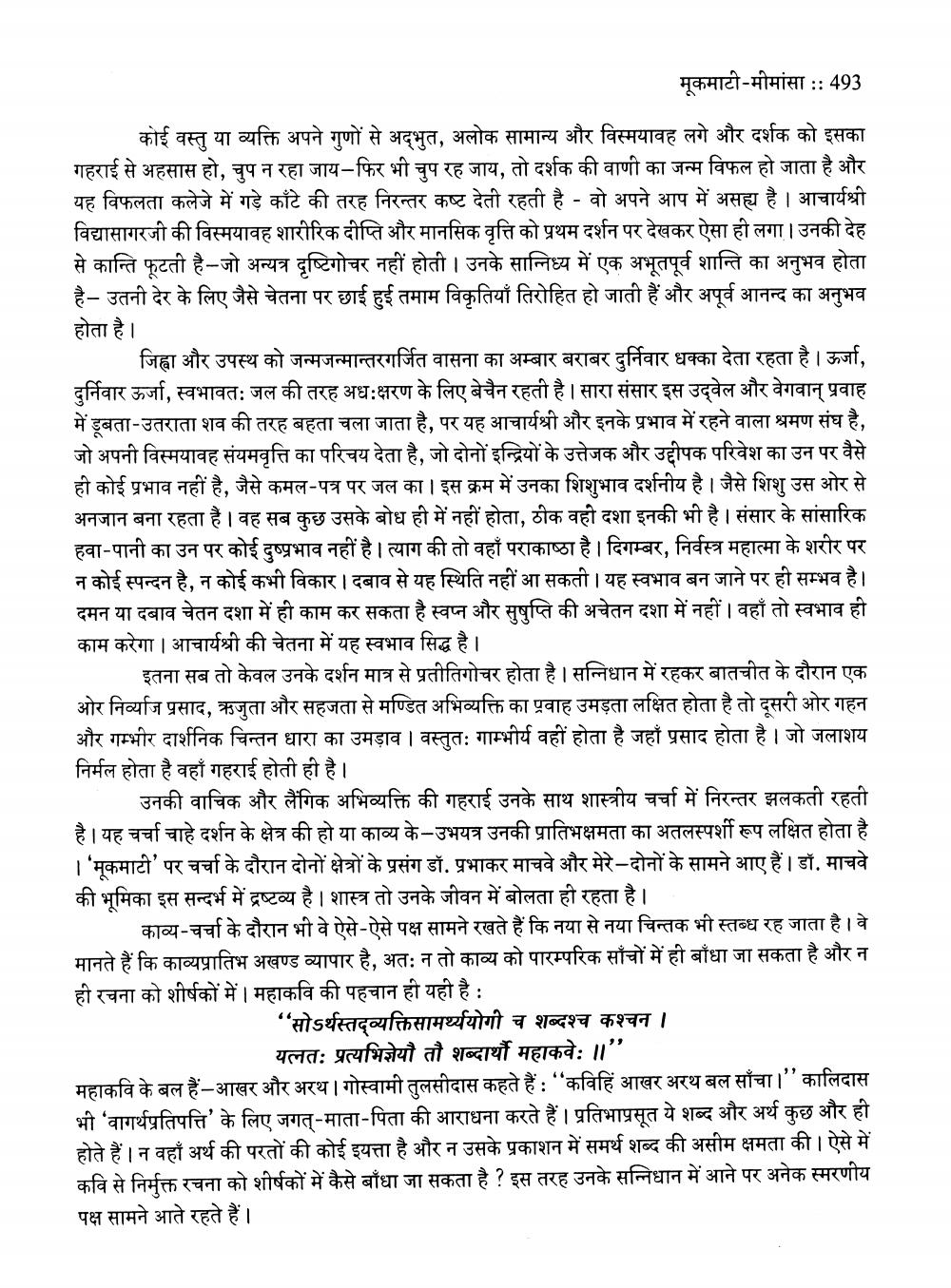________________
मूकमाटी-मीमांसा :: 493
कोई वस्तु या व्यक्ति अपने गुणों से अद्भुत, अलोक सामान्य और विस्मयावह लगे और दर्शक को इसका गहराई से अहसास हो, चुप न रहा जाय-फिर भी चुप रह जाय, तो दर्शक की वाणी का जन्म विफल हो जाता है और यह विफलता कलेजे में गड़े काँटे की तरह निरन्तर कष्ट देती रहती है - वो अपने आप में असह्य है । आचार्यश्री विद्यासागरजी की विस्मयावह शारीरिक दीप्ति और मानसिक वृत्ति को प्रथम दर्शन पर देखकर ऐसा ही लगा। उनकी देह से कान्ति फूटती है-जो अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होती । उनके सान्निध्य में एक अभूतपूर्व शान्ति का अनुभव होता है- उतनी देर के लिए जैसे चेतना पर छाई हुई तमाम विकृतियाँ तिरोहित हो जाती हैं और अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है।
जिह्वा और उपस्थ को जन्मजन्मान्तरगर्जित वासना का अम्बार बराबर दुर्निवार धक्का देता रहता है । ऊर्जा, दुर्निवार ऊर्जा, स्वभावत: जल की तरह अध:क्षरण के लिए बेचैन रहती है । सारा संसार इस उद्वेल और वेगवान् प्रवाह में डूबता-उतराता शव की तरह बहता चला जाता है, पर यह आचार्यश्री और इनके प्रभाव में रहने वाला श्रमण संघ है, जो अपनी विस्मयावह संयमवृत्ति का परिचय देता है, जो दोनों इन्द्रियों के उत्तेजक और उद्दीपक परिवेश का उन पर वैसे ही कोई प्रभाव नहीं है, जैसे कमल-पत्र पर जल का। इस क्रम में उनका शिशुभाव दर्शनीय है। जैसे शिशु उस ओर से अनजान बना रहता है । वह सब कुछ उसके बोध ही में नहीं होता, ठीक वही दशा इनकी भी है । संसार के सांसारिक हवा-पानी का उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है । त्याग की तो वहाँ पराकाष्ठा है । दिगम्बर, निर्वस्त्र महात्मा के शरीर पर न कोई स्पन्दन है, न कोई कभी विकार । दबाव से यह स्थिति नहीं आ सकती। यह स्वभाव बन जाने पर ही सम्भव है। दमन या दबाव चेतन दशा में ही काम कर सकता है स्वप्न और सुषुप्ति की अचेतन दशा में नहीं। वहाँ तो स्वभाव ही काम करेगा । आचार्यश्री की चेतना में यह स्वभाव सिद्ध है।
इतना सब तो केवल उनके दर्शन मात्र से प्रतीतिगोचर होता है । सन्निधान में रहकर बातचीत के दौरान एक ओर निर्व्याज प्रसाद, ऋजुता और सहजता से मण्डित अभिव्यक्ति का प्रवाह उमड़ता लक्षित होता है तो दूसरी ओर गहन और गम्भीर दार्शनिक चिन्तन धारा का उमड़ाव । वस्तुत: गाम्भीर्य वहीं होता है जहाँ प्रसाद होता है । जो जलाशय निर्मल होता है वहाँ गहराई होती ही है।
उनकी वाचिक और लैंगिक अभिव्यक्ति की गहराई उनके साथ शास्त्रीय चर्चा में निरन्तर झलकती रहती है। यह चर्चा चाहे दर्शन के क्षेत्र की हो या काव्य के-उभयत्र उनकी प्रातिभक्षमता का अतलस्पर्शी रूप लक्षित होता है । 'मूकमाटी' पर चर्चा के दौरान दोनों क्षेत्रों के प्रसंग डॉ. प्रभाकर माचवे और मेरे-दोनों के सामने आए हैं। डॉ. माचवे की भमिका इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है। शास्त्र तो उनके जीवन में बोलता ही रहता है।
काव्य-चर्चा के दौरान भी वे ऐसे-ऐसे पक्ष सामने रखते हैं कि नया से नया चिन्तक भी स्तब्ध रह जाता है । वे मानते हैं कि काव्यप्रातिभ अखण्ड व्यापार है, अत: न तो काव्य को पारम्परिक साँचों में ही बाँधा जा सकता है और न ही रचना को शीर्षकों में । महाकवि की पहचान ही यही है :
"सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी च शब्दश्च कश्चन ।
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थो महाकवेः ॥" महाकवि के बल हैं-आखर और अरथ । गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं : “कविहिं आखर अरथ बल साँचा।" कालिदास भी वागर्थप्रतिपत्ति' के लिए जगत्-माता-पिता की आराधना करते हैं । प्रतिभाप्रसूत ये शब्द और अर्थ कुछ और ही होते हैं । न वहाँ अर्थ की परतों की कोई इयत्ता है और न उसके प्रकाशन में समर्थ शब्द की असीम क्षमता की। ऐसे में कवि से निर्मुक्त रचना को शीर्षकों में कैसे बाँधा जा सकता है ? इस तरह उनके सन्निधान में आने पर अनेक स्मरणीय पक्ष सामने आते रहते हैं।