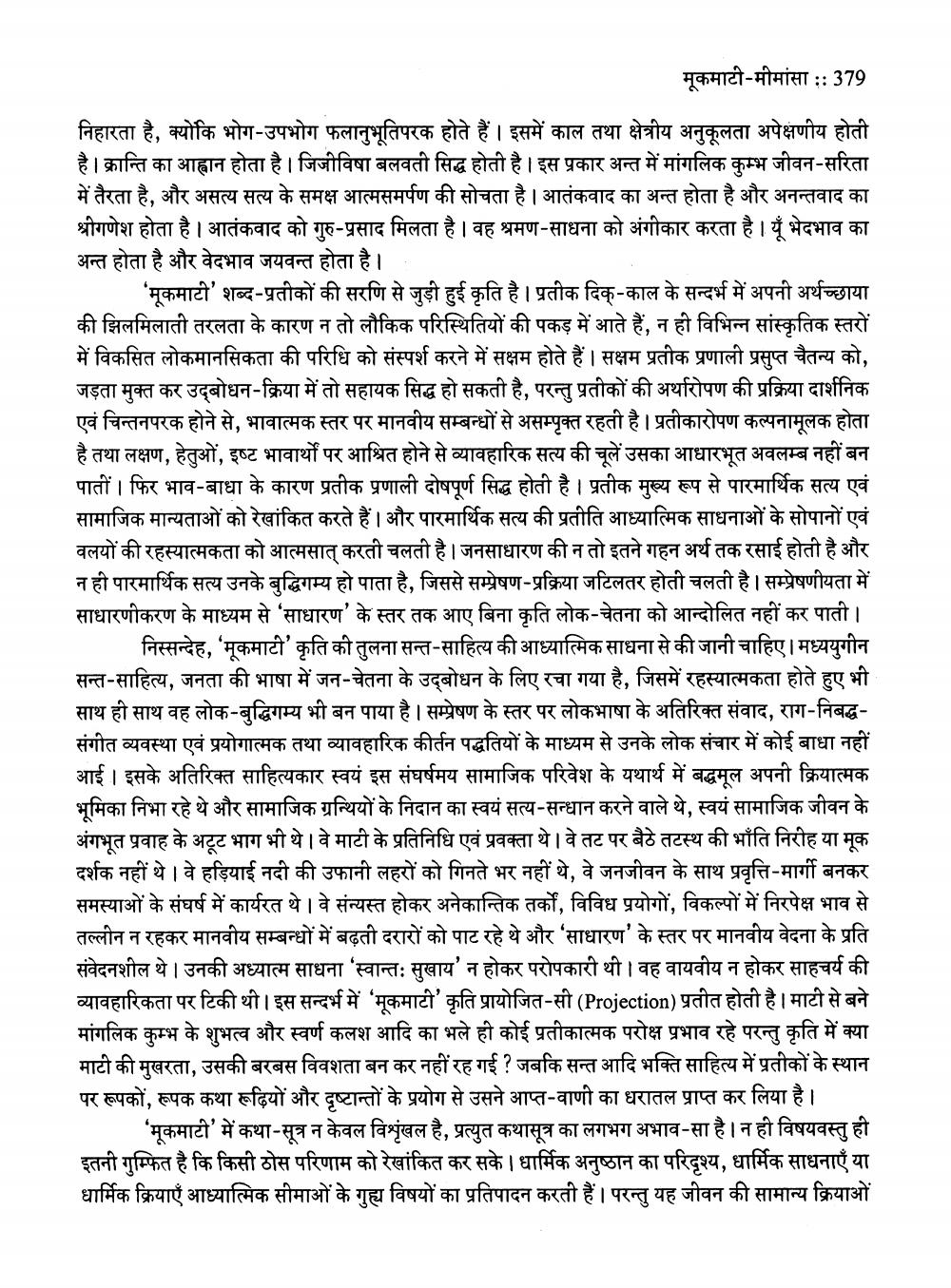________________
मूकमाटी-मीमांसा :: 379
निहारता है, क्योंकि भोग-उपभोग फलानुभूतिपरक होते हैं । इसमें काल तथा क्षेत्रीय अनुकूलता अपेक्षणीय होती है । क्रान्ति का आह्वान होता है । जिजीविषा बलवती सिद्ध होती है। इस प्रकार अन्त में मांगलिक कुम्भ जीवन-सरिता में तैरता है, और असत्य सत्य के समक्ष आत्मसमर्पण की सोचता है । आतंकवाद का अन्त होता है और अनन्तवाद का श्रीगणेश होता है। आतंकवाद को गुरु प्रसाद मिलता है । वह श्रमण - साधना को अंगीकार करता है। यूँ भेदभाव का अन्त होता है और वेदभाव जयवन्त होता है ।
'मूकमाटी' शब्द-प्रतीकों की सरणि से जुड़ी हुई कृति है । प्रतीक दिक्-काल के सन्दर्भ में अपनी अर्थच्छाया की झिलमिलाती तरलता के कारण न तो लौकिक परिस्थितियों की पकड़ में आते हैं, न ही विभिन्न सांस्कृतिक स्तरों में विकसित लोकमानसिकता की परिधि को संस्पर्श करने में सक्षम होते हैं । सक्षम प्रतीक प्रणाली प्रसुप्त चैतन्य को, जड़ता मुक्त कर उद्बोधन - क्रिया में तो सहायक सिद्ध हो सकती है, परन्तु प्रतीकों की अर्थारोपण की प्रक्रिया दार्शनिक एवं चिन्तनपरक होने से, भावात्मक स्तर पर मानवीय सम्बन्धों से असम्पृक्त रहती है। प्रतीकारोपण कल्पनामूलक होता है तथा लक्षण, हेतुओं, इष्ट भावार्थों पर आश्रित होने से व्यावहारिक सत्य की चूलें उसका आधारभूत अवलम्ब नहीं बन पातीं । फिर भाव-बाधा के कारण प्रतीक प्रणाली दोषपूर्ण सिद्ध होती है । प्रतीक मुख्य रूप से पारमार्थिक सत्य एवं सामाजिक मान्यताओं को रेखांकित करते हैं । और पारमार्थिक सत्य की प्रतीति आध्यात्मिक साधनाओं के सोपानों एवं वलयों की रहस्यात्मकता को आत्मसात् करती चलती है। जनसाधारण की न तो इतने गहन अर्थ तक रसाई होती है और न ही पारमार्थिक सत्य उनके बुद्धिगम्य हो पाता है, जिससे सम्प्रेषण-प्रक्रिया जटिलतर होती चलती है। सम्प्रेषणीयता में साधारणीकरण के माध्यम से 'साधारण' के स्तर तक आए बिना कृति लोक चेतना को आन्दोलित नहीं कर पाती ।
निस्सन्देह, ‘मूकमाटी' कृति की तुलना सन्त-साहित्य की आध्यात्मिक साधना से की जानी चाहिए । मध्ययुगीन सन्त-साहित्य, जनता की भाषा में जन-चेतना के उद्बोधन के लिए रचा गया है, जिसमें रहस्यात्मकता होते हुए भी साथ ही साथ वह लोक - बुद्धिगम्य भी बन पाया है । सम्प्रेषण के स्तर पर लोकभाषा के अतिरिक्त संवाद, राग-निबद्धसंगीत व्यवस्था एवं प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक कीर्तन पद्धतियों के माध्यम से उनके लोक संचार में कोई बाधा नहीं आई । इसके अतिरिक्त साहित्यकार स्वयं इस संघर्षमय सामाजिक परिवेश के यथार्थ में बद्धमूल अपनी क्रियात्मक भूमिका निभा रहे थे और सामाजिक ग्रन्थियों के निदान का स्वयं सत्य-सन्धान करने वाले थे, स्वयं सामाजिक जीवन के अंगभूत प्रवाह के अटूट भाग भी थे । वे माटी के प्रतिनिधि एवं प्रवक्ता थे । वे तट पर बैठे तटस्थ की भाँति निरीह या मूक दर्शक नहीं थे । वे हड़ियाई नदी की उफानी लहरों को गिनते भर नहीं थे, वे जनजीवन के साथ प्रवृत्ति-मार्गी बनकर समस्याओं के संघर्ष में कार्यरत थे । वे संन्यस्त होकर अनेकान्तिक तर्कों, विविध प्रयोगों, विकल्पों में निरपेक्ष भाव से तल्लीन न रहकर मानवीय सम्बन्धों में बढ़ती दरारों को पाट रहे थे और 'साधारण' के स्तर पर मानवीय वेदना के प्रति संवेदनशील थे । उनकी अध्यात्म साधना 'स्वान्तः सुखाय' न होकर परोपकारी थी। वह वायवीय न होकर साहचर्य की व्यावहारिकता पर टिकी थी । इस सन्दर्भ में 'मूकमाटी' कृति प्रायोजित - सी (Projection) प्रतीत होती है। माटी से बने मांगलिक कुम्भ के शुभत्व और स्वर्ण कलश आदि का भले ही कोई प्रतीकात्मक परोक्ष प्रभाव रहे परन्तु कृति में क्या माटी की मुखरता, उसकी बरबस विवशता बन कर नहीं रह गई ? जबकि सन्त आदि भक्ति साहित्य में प्रतीकों के स्थान पर रूपकों, रूपक कथा रूढ़ियों और दृष्टान्तों के प्रयोग से उसने आप्त-वाणी का धरातल प्राप्त कर लिया है।
'मूकमाटी' में कथा - सूत्र न केवल विशृंखल है, प्रत्युत कथासूत्र का लगभग अभाव-सा है। न ही विषयवस्तु ही इतनी गुम्फित है कि किसी ठोस परिणाम को रेखांकित कर सके । धार्मिक अनुष्ठान का परिदृश्य, धार्मिक साधनाएँ या धार्मिक क्रियाएँ आध्यात्मिक सीमाओं के गुह्य विषयों का प्रतिपादन करती हैं । परन्तु यह जीवन की सामान्य क्रियाओं