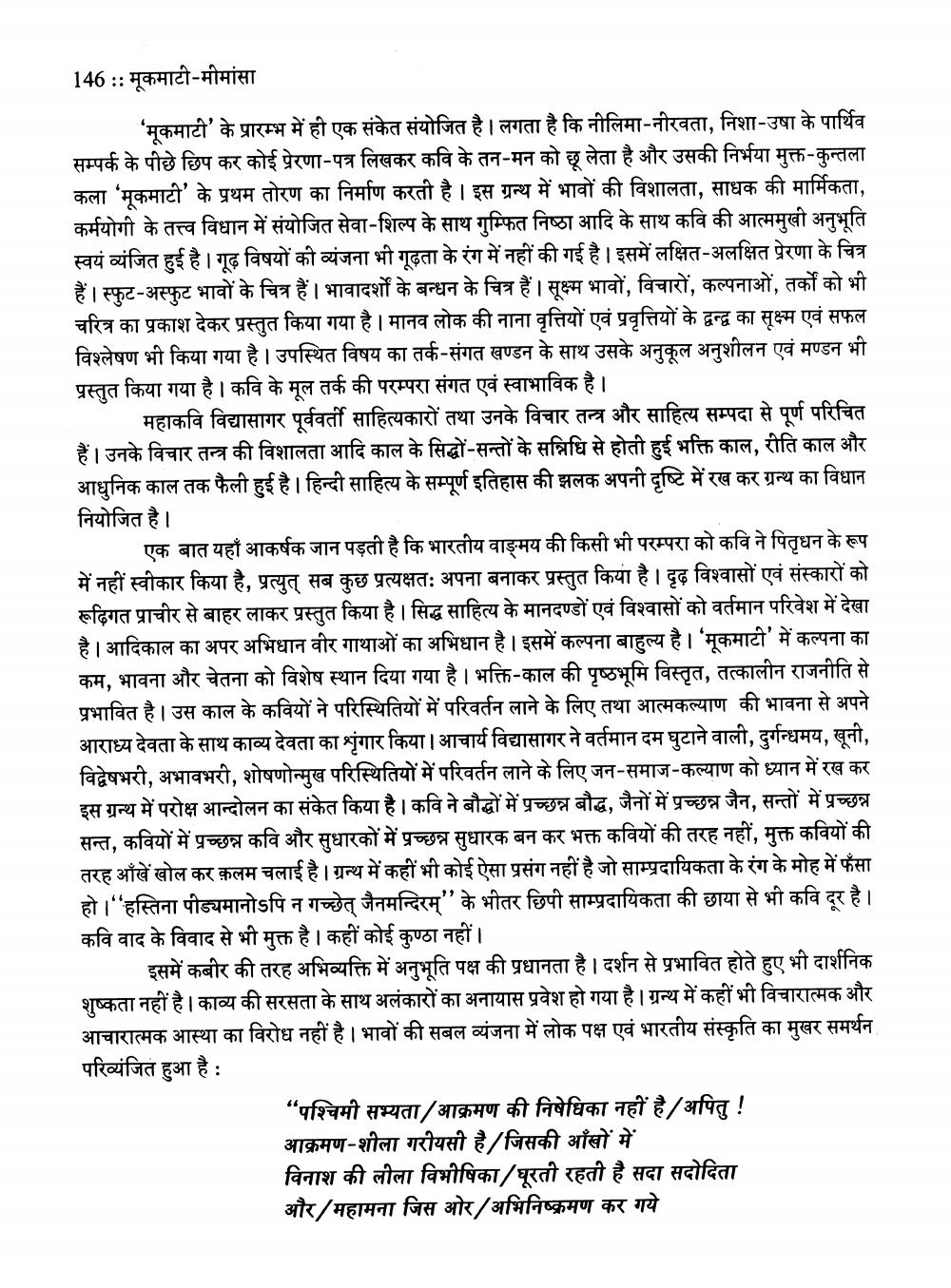________________
146 :: मूकमाटी-मीमांसा
'मूकमाटी' के प्रारम्भ में ही एक संकेत संयोजित है। लगता है कि नीलिमा-नीरवता, निशा-उषा के पार्थिव सम्पर्क के पीछे छिप कर कोई प्रेरणा-पत्र लिखकर कवि के तन-मन को छू लेता है और उसकी निर्भया मुक्त-कुन्तला कला 'मूकमाटी' के प्रथम तोरण का निर्माण करती है । इस ग्रन्थ में भावों की विशालता, साधक की मार्मिकता, कर्मयोगी के तत्त्व विधान में संयोजित सेवा-शिल्प के साथ गुम्फित निष्ठा आदि के साथ कवि की आत्ममुखी अनुभूति स्वयं व्यंजित हुई है । गूढ विषयों की व्यंजना भी गूढ़ता के रंग में नहीं की गई है। इसमें लक्षित-अलक्षित प्रेरणा के चित्र हैं। स्फुट-अस्फुट भावों के चित्र हैं। भावादर्शों के बन्धन के चित्र हैं । सूक्ष्म भावों, विचारों, कल्पनाओं, तर्को को भी चरित्र का प्रकाश देकर प्रस्तुत किया गया है। मानव लोक की नाना वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के द्वन्द्व का सूक्ष्म एवं सफल विश्लेषण भी किया गया है। उपस्थित विषय का तर्क-संगत खण्डन के साथ उसके अनुकूल अनुशीलन एवं मण्डन भी प्रस्तुत किया गया है। कवि के मूल तर्क की परम्परा संगत एवं स्वाभाविक है।
महाकवि विद्यासागर पूर्ववर्ती साहित्यकारों तथा उनके विचार तन्त्र और साहित्य सम्पदा से पूर्ण परिचित हैं। उनके विचार तन्त्र की विशालता आदि काल के सिद्धों-सन्तों के सन्निधि से होती हुई भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तक फैली हुई है । हिन्दी साहित्य के सम्पूर्ण इतिहास की झलक अपनी दृष्टि में रख कर ग्रन्थ का विधान नियोजित है।
एक बात यहाँ आकर्षक जान पड़ती है कि भारतीय वाङ्मय की किसी भी परम्परा को कवि ने पितृधन के रूप में नहीं स्वीकार किया है, प्रत्युत् सब कुछ प्रत्यक्षत: अपना बनाकर प्रस्तुत किया है । दृढ़ विश्वासों एवं संस्कारों को रूढ़िगत प्राचीर से बाहर लाकर प्रस्तुत किया है । सिद्ध साहित्य के मानदण्डों एवं विश्वासों को वर्तमान परिवेश में देखा है। आदिकाल का अपर अभिधान वीर गाथाओं का अभिधान है । इसमें कल्पना बाहुल्य है। 'मूकमाटी' में कल्पना का कम, भावना और चेतना को विशेष स्थान दिया गया है । भक्ति-काल की पृष्ठभूमि विस्तृत, तत्कालीन राजनीति से प्रभावित है । उस काल के कवियों ने परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए तथा आत्मकल्याण की भावना से अपने आराध्य देवता के साथ काव्य देवता का शृंगार किया। आचार्य विद्यासागर ने वर्तमान दम घुटाने वाली, दुर्गन्धमय, खूनी, विद्वेषभरी, अभावभरी, शोषणोन्मुख परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए जन-समाज-कल्याण को ध्यान में रख कर इस ग्रन्थ में परोक्ष आन्दोलन का संकेत किया है । कवि ने बौद्धों में प्रच्छन्न बौद्ध, जैनों में प्रच्छन्न जैन, सन्तों में प्रच्छन्न सन्त, कवियों में प्रच्छन्न कवि और सुधारकों में प्रच्छन्न सुधारक बन कर भक्त कवियों की तरह नहीं, मुक्त कवियों की तरह आँखें खोल कर क़लम चलाई है । ग्रन्थ में कहीं भी कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो साम्प्रदायिकता के रंग के मोह में फंसा हो । 'हस्तिना पीड्यमानोऽपि न गच्छेत् जैनमन्दिरम्" के भीतर छिपी साम्प्रदायिकता की छाया से भी कवि दूर है। कवि वाद के विवाद से भी मुक्त है। कहीं कोई कुण्ठा नहीं।
इसमें कबीर की तरह अभिव्यक्ति में अनुभूति पक्ष की प्रधानता है । दर्शन से प्रभावित होते हुए भी दार्शनिक शुष्कता नहीं है । काव्य की सरसता के साथ अलंकारों का अनायास प्रवेश हो गया है। ग्रन्थ में कहीं भी विचारात्मक और आचारात्मक आस्था का विरोध नहीं है । भावों की सबल व्यंजना में लोक पक्ष एवं भारतीय संस्कृति का मुखर समर्थन परिव्यंजित हुआ है :
“पश्चिमी सभ्यता/आक्रमण की निषेधिका नहीं है/अपितु ! आक्रमण-शीला गरीयसी है/जिसकी आँखों में । विनाश की लीला विभीषिका/घूरती रहती है सदा सदोदिता और/महामना जिस ओर/अभिनिष्क्रमण कर गये