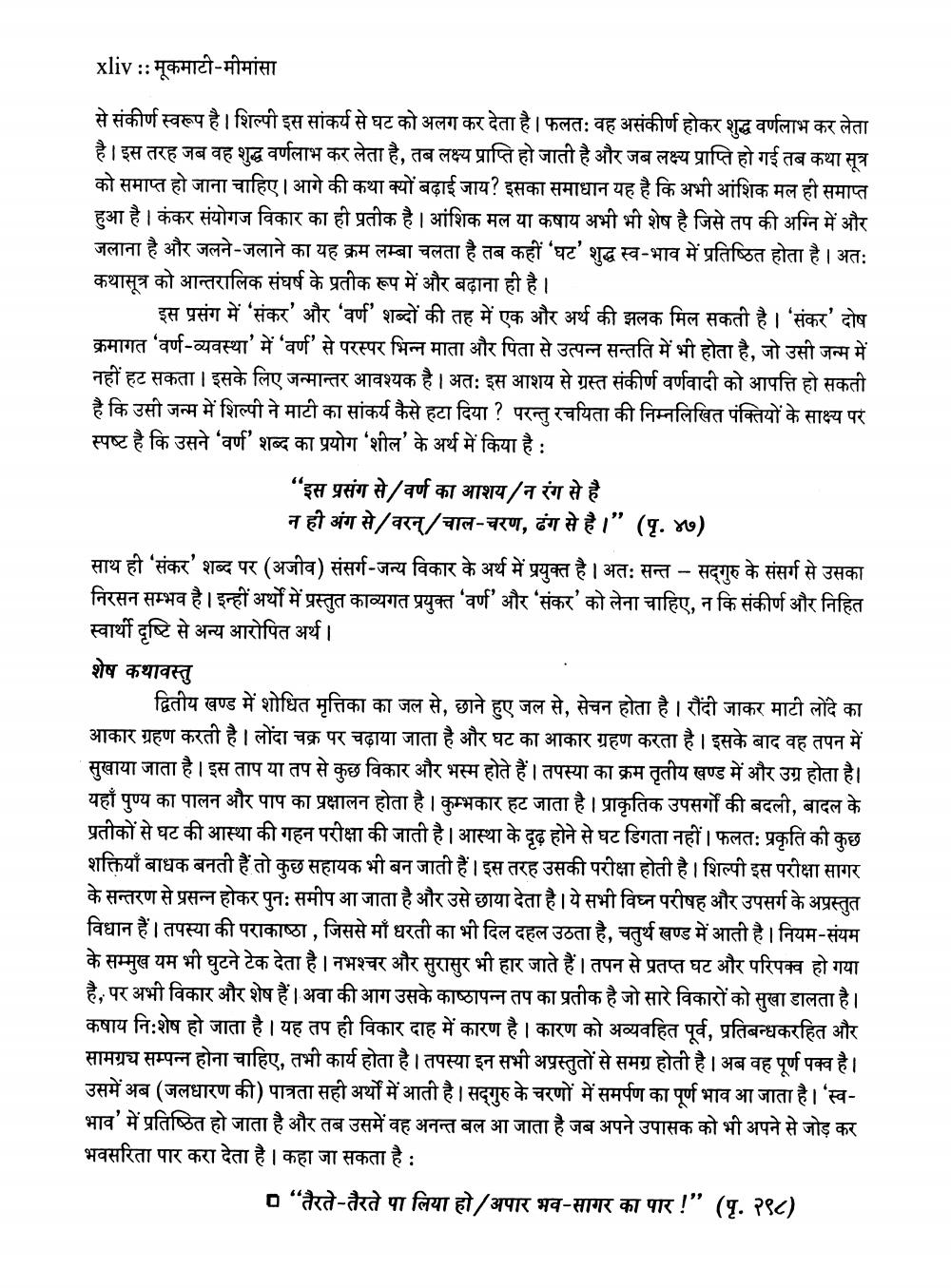________________
xliv :: मूकमाटी-मीमांसा से संकीर्ण स्वरूप है। शिल्पी इस सांकर्य से घट को अलग कर देता है । फलत: वह असंकीर्ण होकर शुद्ध वर्णलाभ कर लेता है। इस तरह जब वह शुद्ध वर्णलाभ कर लेता है, तब लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है और जब लक्ष्य प्राप्ति हो गई तब कथा सूत्र को समाप्त हो जाना चाहिए। आगे की कथा क्यों बढ़ाई जाय? इसका समाधान यह है कि अभी आंशिक मल ही समाप्त हुआ है। कंकर संयोगज विकार का ही प्रतीक है । आंशिक मल या कषाय अभी भी शेष है जिसे तप की अग्नि में और जलाना है और जलने-जलाने का यह क्रम लम्बा चलता है तब कहीं 'घट' शुद्ध स्व-भाव में प्रतिष्ठित होता है । अत: कथासूत्र को आन्तरालिक संघर्ष के प्रतीक रूप में और बढ़ाना ही है।
इस प्रसंग में 'संकर' और 'वर्ण' शब्दों की तह में एक और अर्थ की झलक मिल सकती है। 'संकर' दोष क्रमागत 'वर्ण-व्यवस्था' में 'वर्ण' से परस्पर भिन्न माता और पिता से उत्पन्न सन्तति में भी होता है, जो उसी जन्म में नहीं हट सकता । इसके लिए जन्मान्तर आवश्यक है । अत: इस आशय से ग्रस्त संकीर्ण वर्णवादी को आपत्ति हो सकती है कि उसी जन्म में शिल्पी ने माटी का सांकर्य कैसे हटा दिया? परन्तु रचयिता की निम्नलिखित पंक्तियों के साक्ष्य पर स्पष्ट है कि उसने 'वर्ण' शब्द का प्रयोग 'शील' के अर्थ में किया है :
"इस प्रसंग से/वर्ण का आशय/न रंग से है
न ही अंग से/वरन्/चाल-चरण, ढंग से है ।" (पृ. ४७) साथ ही 'संकर' शब्द पर (अजीव) संसर्ग-जन्य विकार के अर्थ में प्रयुक्त है । अत: सन्त - सद्गुरु के संसर्ग से उसका निरसन सम्भव है। इन्हीं अर्थों में प्रस्तुत काव्यगत प्रयुक्त वर्ण' और 'संकर' को लेना चाहिए, न कि संकीर्ण और निहित स्वार्थी दृष्टि से अन्य आरोपित अर्थ । शेष कथावस्तु
द्वितीय खण्ड में शोधित मृत्तिका का जल से, छाने हुए जल से, सेचन होता है । रौंदी जाकर माटी लोंदे का आकार ग्रहण करती है । लोंदा चक्र पर चढ़ाया जाता है और घट का आकार ग्रहण करता है । इसके बाद वह तपन में सुखाया जाता है । इस ताप या तप से कुछ विकार और भस्म होते हैं। तपस्या का क्रम तृतीय खण्ड में और उग्र होता है। यहाँ पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन होता है । कुम्भकार हट जाता है । प्राकृतिक उपसर्गों की बदली, बादल के प्रतीकों से घट की आस्था की गहन परीक्षा की जाती है । आस्था के दृढ़ होने से घट डिगता नहीं। फलत: प्रकृति की कुछ शक्तियाँ बाधक बनती हैं तो कुछ सहायक भी बन जाती हैं। इस तरह उसकी परीक्षा होती है। शिल्पी इस परीक्षा सागर के सन्तरण से प्रसन्न होकर पुन: समीप आ जाता है और उसे छाया देता है। ये सभी विघ्न परीषह और उपसर्ग के अप्रस्तुत विधान हैं। तपस्या की पराकाष्ठा , जिससे माँ धरती का भी दिल दहल उठता है, चतुर्थ खण्ड में आती है। नियम-संयम के सम्मुख यम भी घुटने टेक देता है । नभश्चर और सुरासुर भी हार जाते हैं । तपन से प्रतप्त घट और परिपक्व हो गया है, पर अभी विकार और शेष हैं। अवा की आग उसके काष्ठापन्न तप का प्रतीक है जो सारे विकारों को सुखा डालता है। कषाय नि:शेष हो जाता है। यह तप ही विकार दाह में कारण है । कारण को अव्यवहित पूर्व, प्रतिबन्धकरहित और सामग्रय सम्पन्न होना चाहिए, तभी कार्य होता है । तपस्या इन सभी अप्रस्तुतों से समग्र होती है । अब वह पूर्ण पक्व है। उसमें अब (जलधारण की) पात्रता सही अर्थों में आती है। सद्गुरु के चरणों में समर्पण का पूर्ण भाव आ जाता है। स्वभाव' में प्रतिष्ठित हो जाता है और तब उसमें वह अनन्त बल आ जाता है जब अपने उपासक को भी अपने से जोड़ कर भवसरिता पार करा देता है । कहा जा सकता है :
0 “तैरते-तैरते पा लिया हो/अपार भव-सागर का पार!" (पृ. २९८)