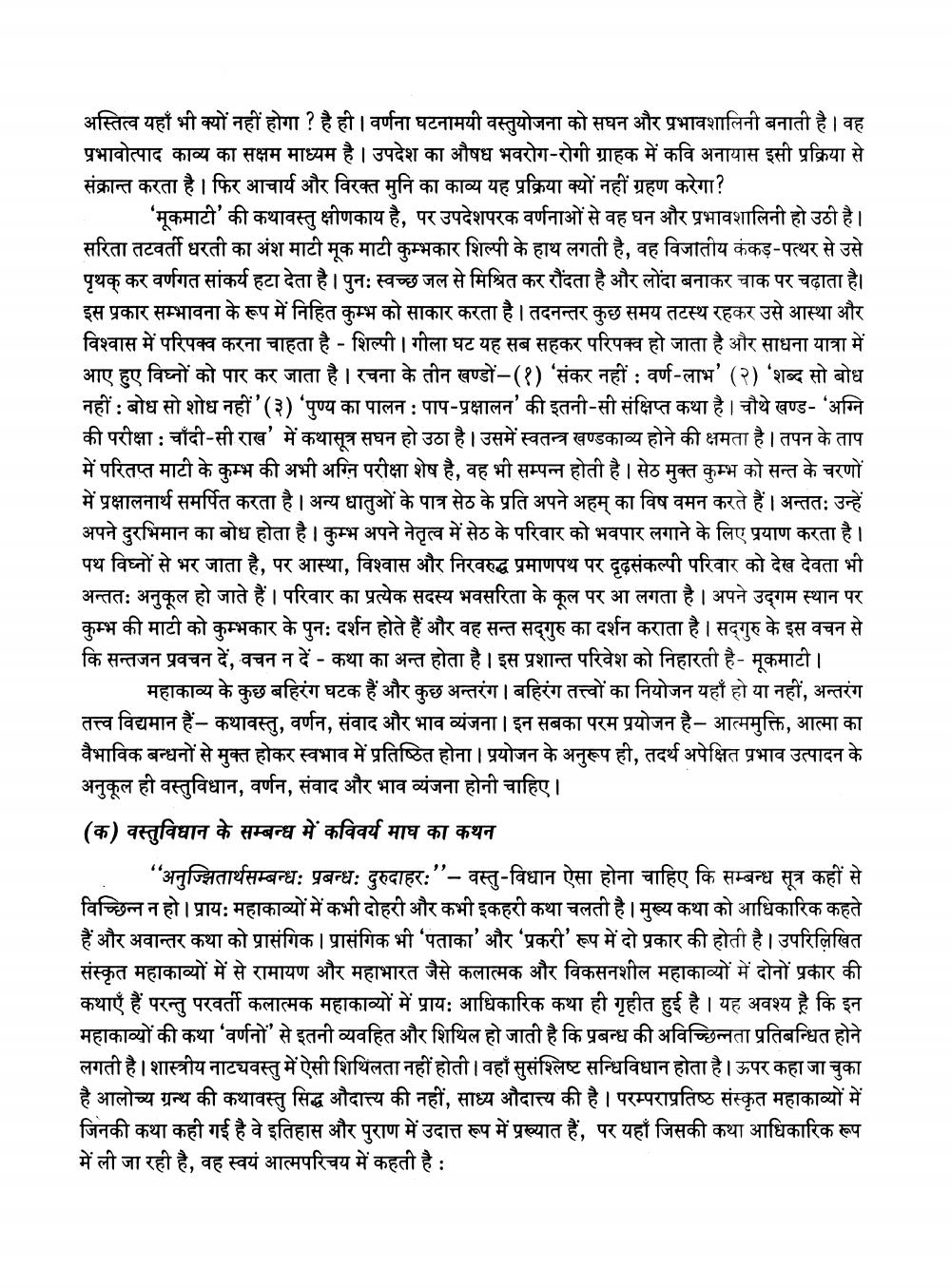________________
अस्तित्व यहाँ भी क्यों नहीं होगा ? है ही । वर्णना घटनामयी वस्तुयोजना को सघन और प्रभावशालिनी बनाती है। वह प्रभावोत्पाद काव्य का सक्षम माध्यम है । उपदेश का औषध भवरोग-रोगी ग्राहक में कवि अनायास इसी प्रक्रिया से संक्रान्त करता है । फिर आचार्य और विरक्त मुनि का काव्य यह प्रक्रिया क्यों नहीं ग्रहण करेगा?
'मूकमाटी' की कथावस्तु क्षीणकाय है, पर उपदेशपरक वर्णनाओं से वह घन और प्रभावशालिनी हो उठी है। सरिता तटवर्ती धरती का अंश माटी मूक माटी कुम्भकार शिल्पी के हाथ लगती है, वह विजातीय कंकड़-पत्थर से उसे पृथक् कर वर्णगत सांकर्य हटा देता है । पुनः स्वच्छ जल से मिश्रित कर रौंदता है और लोंदा बनाकर चाक पर चढ़ाता है। इस प्रकार सम्भावना के रूप में निहित कुम्भ को साकार करता है । तदनन्तर कुछ समय तटस्थ रहकर उसे आस्था और विश्वास में परिपक्व करना चाहता है - शिल्पी । गीला घट यह सब सहकर परिपक्व हो जाता है और साधना यात्रा में आए हुए विघ्नों को पार कर जाता है । रचना के तीन खण्डों-(१) संकर नहीं : वर्ण-लाभ' (२) 'शब्द सो बोध नहीं : बोध सो शोध नहीं' (३) 'पुण्य का पालन : पाप-प्रक्षालन' की इतनी-सी संक्षिप्त कथा है। चौथे खण्ड- ‘अग्नि की परीक्षा : चाँदी-सी राख' में कथासूत्र सघन हो उठा है। उसमें स्वतन्त्र खण्डकाव्य होने की क्षमता है । तपन के ताप में परितप्त माटी के कुम्भ की अभी अग्नि परीक्षा शेष है, वह भी सम्पन्न होती है । सेठ मुक्त कुम्भ को सन्त के चरणों में प्रक्षालनार्थ समर्पित करता है । अन्य धातुओं के पात्र सेठ के प्रति अपने अहम् का विष वमन करते हैं । अन्तत: उन्हें अपने दुरभिमान का बोध होता है । कुम्भ अपने नेतृत्व में सेठ के परिवार को भवपार लगाने के लिए प्रयाण करता है। पथ विघ्नों से भर जाता है, पर आस्था, विश्वास और निरवरुद्ध प्रमाणपथ पर दृढ़संकल्पी परिवार को देख देवता भी अन्तत: अनुकूल हो जाते हैं । परिवार का प्रत्येक सदस्य भवसरिता के कूल पर आ लगता है । अपने उद्गम स्थान पर कुम्भ की माटी को कुम्भकार के पुन: दर्शन होते हैं और वह सन्त सद्गुरु का दर्शन कराता है । सद्गुरु के इस वचन से कि सन्तजन प्रवचन दें, वचन न दें - कथा का अन्त होता है । इस प्रशान्त परिवेश को निहारती है- मूकमाटी।
महाकाव्य के कुछ बहिरंग घटक हैं और कुछ अन्तरंग । बहिरंग तत्त्वों का नियोजन यहाँ हो या नहीं, अन्तरंग तत्त्व विद्यमान हैं- कथावस्त. वर्णन. संवाद और भाव व्यंजना। इन सबका परम प्रयोजन है- आत्ममुक्ति, आत्मा का वैभाविक बन्धनों से मुक्त होकर स्वभाव में प्रतिष्ठित होना । प्रयोजन के अनुरूप ही, तदर्थ अपेक्षित प्रभाव उत्पादन के अनुकूल ही वस्तुविधान, वर्णन, संवाद और भाव व्यंजना होनी चाहिए। (क) वस्तुविधान के सम्बन्ध में कविवर्य माघ का कथन
___ "अनुज्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धः दुरुदाहरः"- वस्तु-विधान ऐसा होना चाहिए कि सम्बन्ध सूत्र कहीं से विच्छिन्न न हो । प्राय: महाकाव्यों में कभी दोहरी और कभी इकहरी कथा चलती है। मुख्य कथा को आधिकारिक कहते हैं और अवान्तर कथा को प्रासंगिक । प्रासंगिक भी पताका' और 'प्रकरी' रूप में दो प्रकार की होती है। उपरिलिखित संस्कृत महाकाव्यों में से रामायण और महाभारत जैसे कलात्मक और विकसनशील महाकाव्यों में दोनों प्रकार की कथाएँ हैं परन्तु परवर्ती कलात्मक महाकाव्यों में प्रायः आधिकारिक कथा ही गृहीत हुई है । यह अवश्य है कि इन महाकाव्यों की कथा वर्णनों से इतनी व्यवहित और शिथिल हो जाती है कि प्रबन्ध की अविच्छिन्नता प्रतिबन्धित होने लगती है। शास्त्रीय नाट्यवस्तु में ऐसी शिथिलता नहीं होती। वहाँ सुसंश्लिष्ट सन्धिविधान होता है। ऊपर कहा जा चुका है आलोच्य ग्रन्थ की कथावस्तु सिद्ध औदात्त्य की नहीं, साध्य औदात्त्य की है । परम्पराप्रतिष्ठ संस्कृत महाकाव्यों में जिनकी कथा कही गई है वे इतिहास और पुराण में उदात्त रूप में प्रख्यात हैं, पर यहाँ जिसकी कथा आधिकारिक रूप में ली जा रही है, वह स्वयं आत्मपरिचय में कहती है :