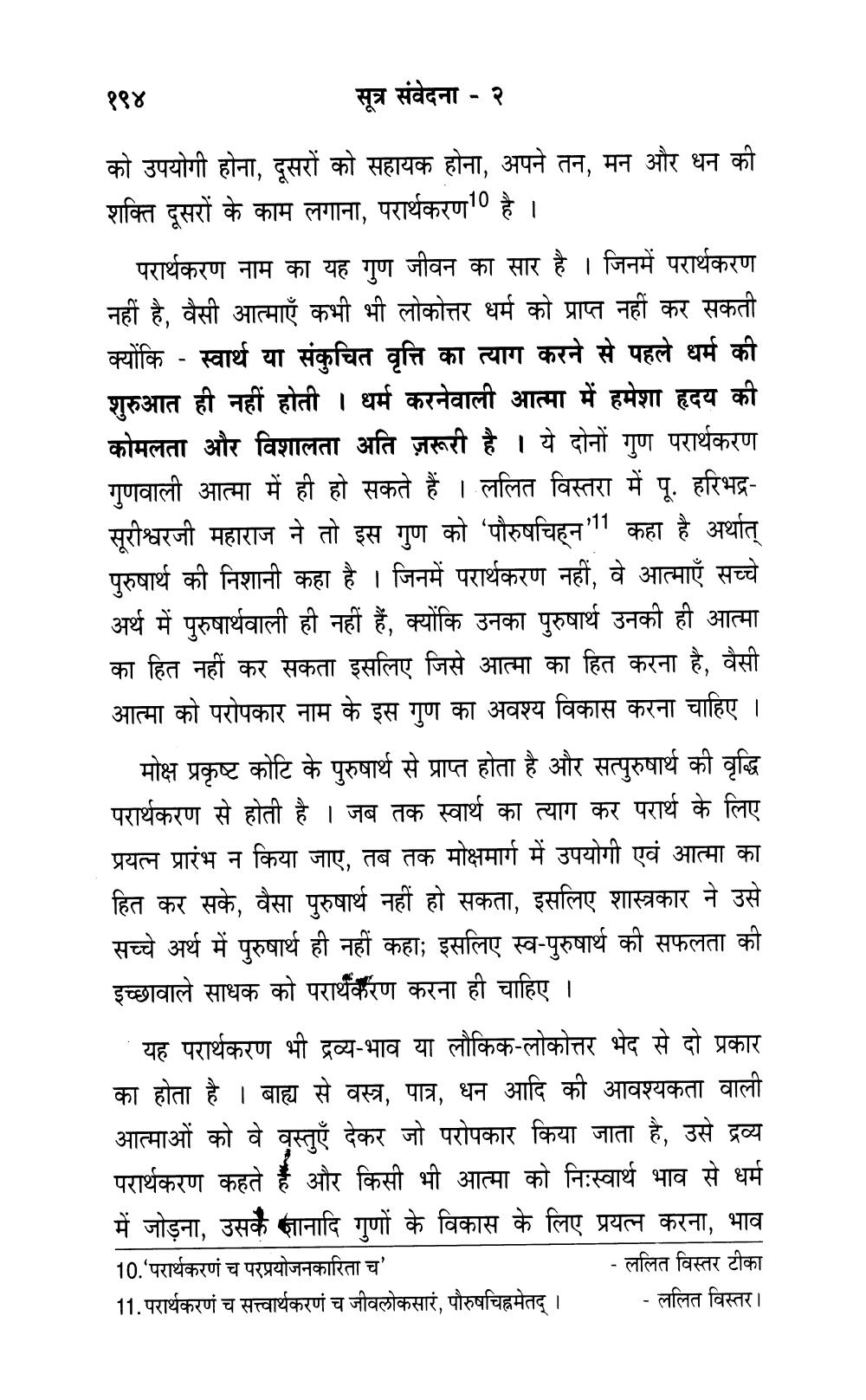________________
१९४
सूत्र संवेदना - २
को उपयोगी होना, दूसरों को सहायक होना, अपने तन, मन और धन की शक्ति दूसरों के काम लगाना, परार्थकरण है ।
परार्थकरण नाम का यह गुण जीवन का सार है । जिनमें परार्थकरण नहीं है, वैसी आत्माएँ कभी भी लोकोत्तर धर्म को प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि - स्वार्थ या संकुचित वृत्ति का त्याग करने से पहले धर्म की शुरुआत ही नहीं होती । धर्म करनेवाली आत्मा में हमेशा हृदय की कोमलता और विशालता अति ज़रूरी है । ये दोनों गुण परार्थकरण गुणवाली आत्मा में ही हो सकते हैं । ललित विस्तरा में पू. हरिभद्रसूरीश्वरजी महाराज ने तो इस गुण को 'पौरुषचिह्न 11 कहा है अर्थात् पुरुषार्थ की निशानी कहा है । जिनमें परार्थकरण नहीं, वे आत्माएँ सच्चे अर्थ में पुरुषार्थवाली ही नहीं हैं, क्योंकि उनका पुरुषार्थ उनकी ही आत्मा का हित नहीं कर सकता इसलिए जिसे आत्मा का हित करना है, वैसी आत्मा को परोपकार नाम के इस गुण का अवश्य विकास करना चाहिए ।
मोक्ष प्रकृष्ट कोटि के पुरुषार्थ से प्राप्त होता है और सत्पुरुषार्थ की वृद्धि परार्थकरण से होती है । जब तक स्वार्थ का त्याग कर परार्थ के लिए प्रयत्न प्रारंभ न किया जाए, तब तक मोक्षमार्ग में उपयोगी एवं आत्मा का हित कर सके, वैसा पुरुषार्थ नहीं हो सकता, इसलिए शास्त्रकार ने उसे सच्चे अर्थ में पुरुषार्थ ही नहीं कहा; इसलिए स्व-पुरुषार्थ की सफलता की इच्छावाले साधक को पराकरण करना ही चाहिए ।
यह परार्थकरण भी द्रव्य-भाव या लौकिक-लोकोत्तर भेद से दो प्रकार का होता है । बाह्य से वस्त्र, पात्र, धन आदि की आवश्यकता वाली आत्माओं को वे वस्तुएँ देकर जो परोपकार किया जाता है, उसे द्रव्य परार्थकरण कहते हैं और किसी भी आत्मा को निःस्वार्थ भाव से धर्म में जोडना, उसके ज्ञानादि गणों के विकास के लिए प्रयत्न करना, भाव 10. परार्थकरणं च परप्रयोजनकारिता च'
- ललित विस्तर टीका 11. परार्थकरणं च सत्त्वार्थकरणं च जीवलोकसारं, पौरुषचिह्नमेतद् । - ललित विस्तर।