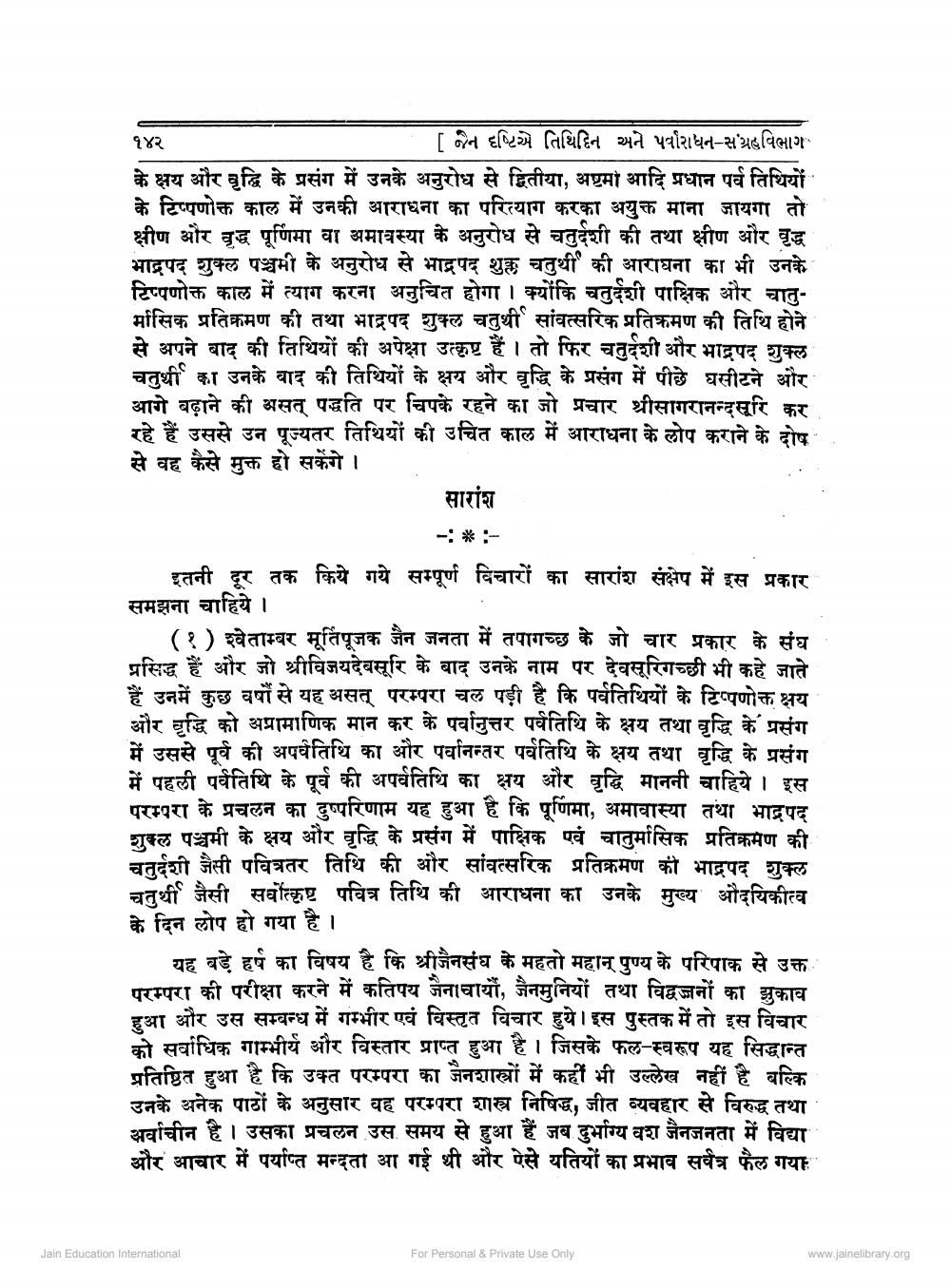________________
१४२
[ જૈન દૃષ્ટિએ તિથિરિન અને પરાધન-સંગ્રહવિભાગ के क्षय और वृद्धि के प्रसंग में उनके अनुरोध से द्वितीया, अष्टमा आदि प्रधान पर्व तिथियों के टिप्पणोक्त काल में उनकी आराधना का परित्याग करका अयुक्त माना जायगा तो क्षीण और वृद्ध पूर्णिमा वा अमावस्या के अनुरोध से चतुर्दशी की तथा क्षीण और वृद्ध भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी के अनुरोध से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की आराधना का भी उनके टिप्पणोक्त काल में त्याग करना अनुचित होगा। क्योंकि चतुर्दशी पाक्षिक और चातु
सिक प्रतिक्रमण की तथा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की तिथि होने से अपने बाद की तिथियों की अपेक्षा उत्कृष्ट हैं । तो फिर चतुर्दशी और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का उनके बाद की तिथियों के क्षय और वृद्धि के प्रसंग में पीछे घसीटने और आगे बढ़ाने की असत् पद्धति पर चिपके रहने का जो प्रचार श्रीसागरानन्दसूरि कर रहे हैं उससे उन पूज्यतर तिथियों की उचित काल में आराधना के लोप कराने के दोष से वह कैसे मुक्त हो सकेंगे।
सारांश
-:*:इतनी दूर तक किये गये सम्पूर्ण विचारों का सारांश संक्षेप में इस प्रकार समझना चाहिये।
(१) श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन जनता में तपागच्छ के जो चार प्रकार के संघ प्रसिद्ध हैं और जो श्रीविजयदेवसूरि के बाद उनके नाम पर देवसूरिगच्छी भी कहे जाते हैं उनमें कुछ वर्षों से यह असत् परम्परा चल पड़ी है कि पर्वतिथियों के टिप्पणोक्त क्षय
और वृद्धि को अप्रामाणिक मान कर के पर्वानुत्तर पर्वतिथि के क्षय तथा वृद्धि के प्रसंग में उससे पूर्व की अपर्वतिथि का और पर्वानन्तर पर्वतिथि के क्षय तथा वृद्धि के प्रसंग में पहली पर्वतिथि के पूर्व की अपर्वतिथि का क्षय और वृद्धि माननी चाहिये । इस परम्परा के प्रचलन का दुष्परिणाम यह हुआ है कि पूर्णिमा, अमावास्या तथा भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी के क्षय और वृद्धि के प्रसंग में पाक्षिक एवं चातुर्मासिक प्रतिक्रमण की चतुर्दशी जैसी पवित्रतर तिथि की और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जैसी सर्वोत्कृष्ट पवित्र तिथि की आराधना का उनके मुख्य औदयिकीत्व के दिन लोप हो गया है।
यह बड़े हर्ष का विषय है कि श्रीजैनसंघ के महतो महान् पुण्य के परिपाक से उक्त परम्परा की परीक्षा करने में कतिपय जैनाचार्यों, जैनमुनियों तथा विद्वजनों का झुकाव हुआ और उस सम्बन्ध में गम्भीर एवं विस्तृत विचार हुये। इस पुस्तक में तो इस विचार को सर्वाधिक गाम्भीर्य और विस्तार प्राप्त हुआ है। जिसके फल-स्वरूप यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हुआ है कि उक्त परम्परा का जैनशास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है बल्कि उनके अनेक पाठों के अनुसार वह परम्परा शास्त्र निषिद्ध, जीत व्यवहार से विरुद्ध तथा अर्वाचीन है। उसका प्रचलन उस समय से हुआ हैं जब दुर्भाग्य वश जैनजनता में विद्या और आचार में पर्याप्त मन्दता आ गई थी और ऐसे यतियों का प्रभाव सर्वत्र फैल गया
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org