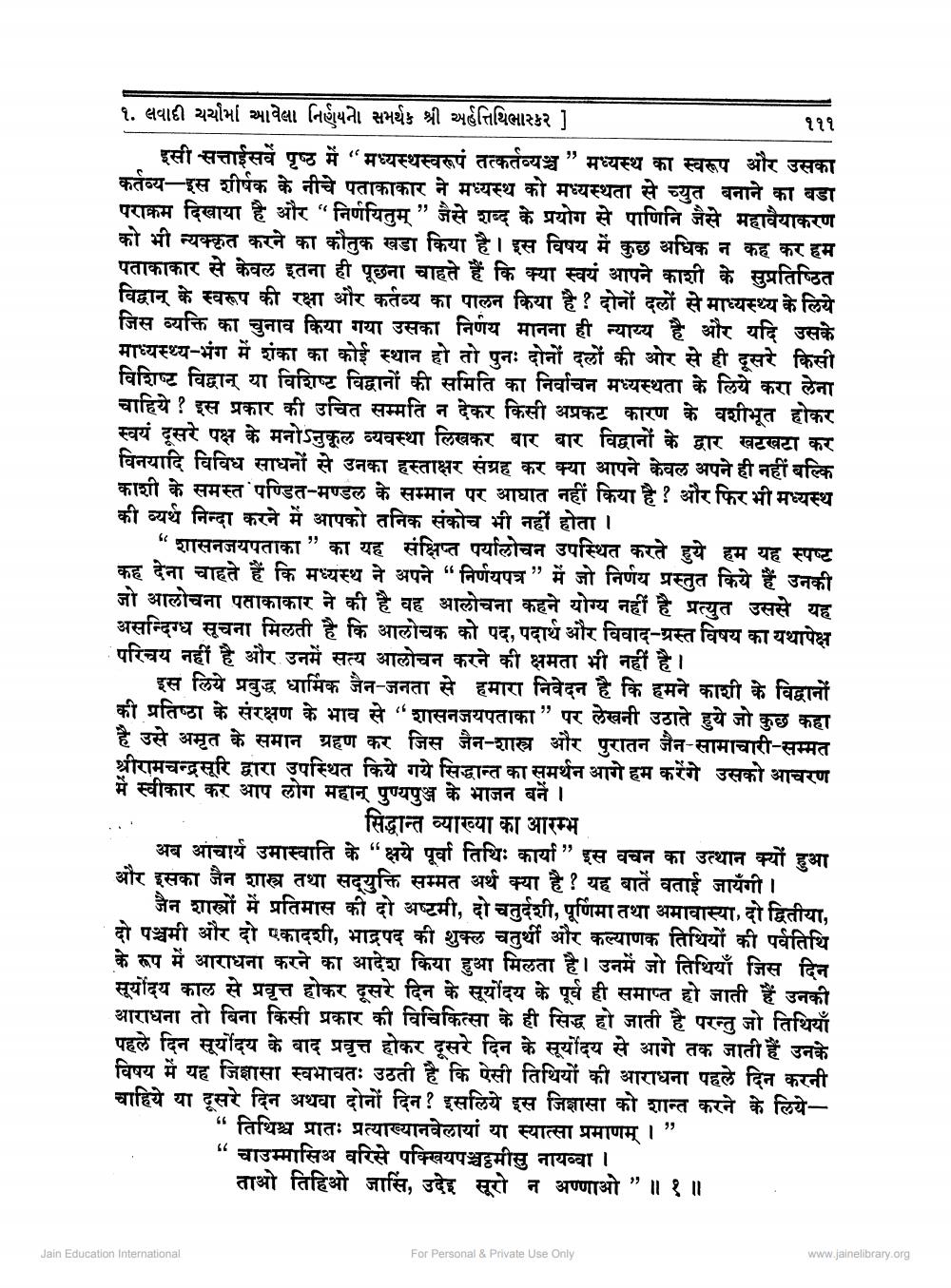________________
૧. લવાદી ચર્ચામાં આવેલા નિર્ણયનો સમર્થક શ્રી અહતિથિભાસકર ]
૧૧૧ ____ इसी सत्ताईसवें पृष्ठ में “मध्यस्थस्वरूपं तत्कर्तव्यञ्च" मध्यस्थ का स्वरूप और उसका कर्तव्य-इस शीर्षक के नीचे पताकाकार ने मध्यस्थ को मध्यस्थता से च्युत बनाने का बडा पराक्रम दिखाया है और “निर्णयितुम्" जैसे शब्द के प्रयोग से पाणिनि जैसे महावैयाकरण को भी न्यक्कृत करने का कौतुक खडा किया है। इस विषय में कुछ अधिक न कह कर हम पताकाकार से केवल इतना ही पूछना चाहते हैं कि क्या स्वयं आपने काशी के सुप्रतिष्ठित विद्वान् के स्वरूप की रक्षा और कर्तव्य का पालन किया है ? दोनों दलों से माध्यस्थ्य के लिये जिस व्यक्ति का चुनाव किया गया उसका निर्णय मानना ही न्याय्य है और यदि उसके माध्यस्थ्य-भंग में शंका का कोई स्थान हो तो पुनः दोनों दलों की ओर से ही दूसरे किसी विशिष्ट विद्वान् या विशिष्ट विद्वानों की समिति का निर्वाचन मध्यस्थता के लिये करा लेना चाहिये ? इस प्रकार की उचित सम्मति न देकर किसी अप्रकट कारण के वशीभूत होकर स्वयं दूसरे पक्ष के मनोऽनुकूल व्यवस्था लिखकर बार बार विद्वानों के द्वार खटखटा कर विनयादि विविध साधनों से उनका हस्ताक्षर संग्रह कर क्या आपने केवल अपने ही नहीं बल्कि काशी के समस्त पण्डित-मण्डल के सम्मान पर आघात नहीं किया है ? और फिर भी मध्यस्थ की व्यर्थ निन्दा करने में आपको तनिक संकोच भी नहीं होता।
“शासनजयपताका" का यह संक्षिप्त पर्यालोचन उपस्थित करते हुये हम यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि मध्यस्थ ने अपने " निर्णयपत्र" में जो निर्णय प्रस्तुत किये हैं उनकी जो आलोचना पताकाकार ने की है वह आलोचना कहने योग्य नहीं है प्रत्युत उससे यह असन्दिग्ध सूचना मिलती है कि आलोचक को पद, पदार्थ और विवाद-ग्रस्त विषय का यथापेक्ष परिचय नहीं है और उनमें सत्य आलोचन करने की क्षमता भी नहीं है। ___ इस लिये प्रबुद्ध धार्मिक जैन-जनता से हमारा निवेदन है कि हमने काशी के विद्वानों की प्रतिष्ठा के संरक्षण के भाव से “शासनजयपताका" पर लेखनी उठाते हुये जो कुछ कहा है उसे अमृत के समान ग्रहण कर जिस जैन-शास्त्र और पुरातन जैन-सामाचारी-सम्मत श्रीरामचन्द्रसूरि द्वारा उपस्थित किये गये सिद्धान्त का समर्थन आगे हम करेंगे उसको आचरण में स्वीकार कर आप लोग महान् पुण्यपुञ्ज के भाजन बने ।
सिद्धान्त व्याख्या का आरम्भ ___ अब आचार्य उमास्वाति के "क्षये पूर्वा तिथिः कार्या" इस वचन का उत्थान क्यों हुआ और इसका जैन शास्त्र तथा सयुक्ति सम्मत अर्थ क्या है ? यह बातें बताई जायँगी।
जैन शास्त्रों में प्रतिमास की दो अष्टमी, दो चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अमावास्या, दो द्वितीया, दो पञ्चमी और दो एकादशी, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी और कल्याणक तिथियों की पर्वतिथि के रूप में आराधना करने का आदेश किया हुआ मिलता है। उनमें जो तिथियाँ जिस दिन सूर्योदय काल से प्रवृत्त होकर दूसरे दिन के सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाती हैं उनकी आराधना तो बिना किसी प्रकार की विचिकित्सा के ही सिद्ध हो जाती है परन्तु जो तिथियाँ पहले दिन सूर्योदय के बाद प्रवृत्त होकर दूसरे दिन के सूर्योदय से आगे तक जाती हैं उनके विषय में यह जिज्ञासा स्वभावतः उठती है कि ऐसी तिथियों की आराधना पहले दिन करनी चाहिये या दसरे दिन अथवा दोनों दिन? इसलिये इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिये
" तिथिश्च प्रातः प्रत्याख्यानवेलायां या स्यात्सा प्रमाणम् । " " चाउम्मासिअ वरिसे पक्खियपञ्चमीसु नायव्वा ।। ताओ तिहिओ जासिं, उदेइ सूरो न अण्णाओ" ॥१॥
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org